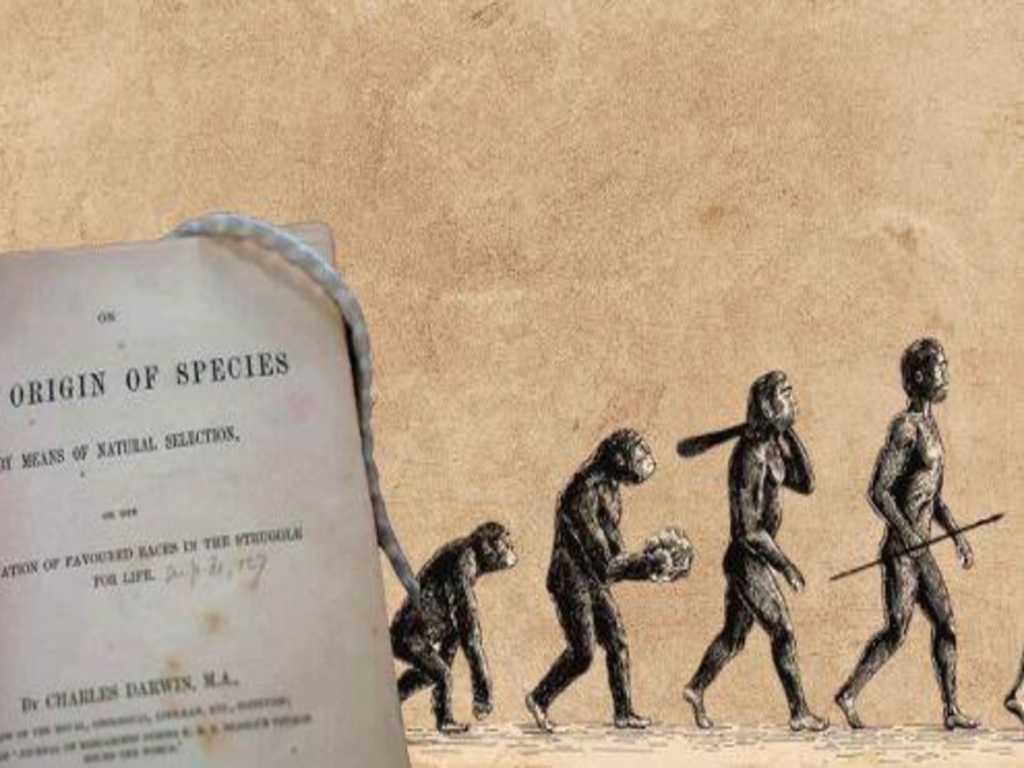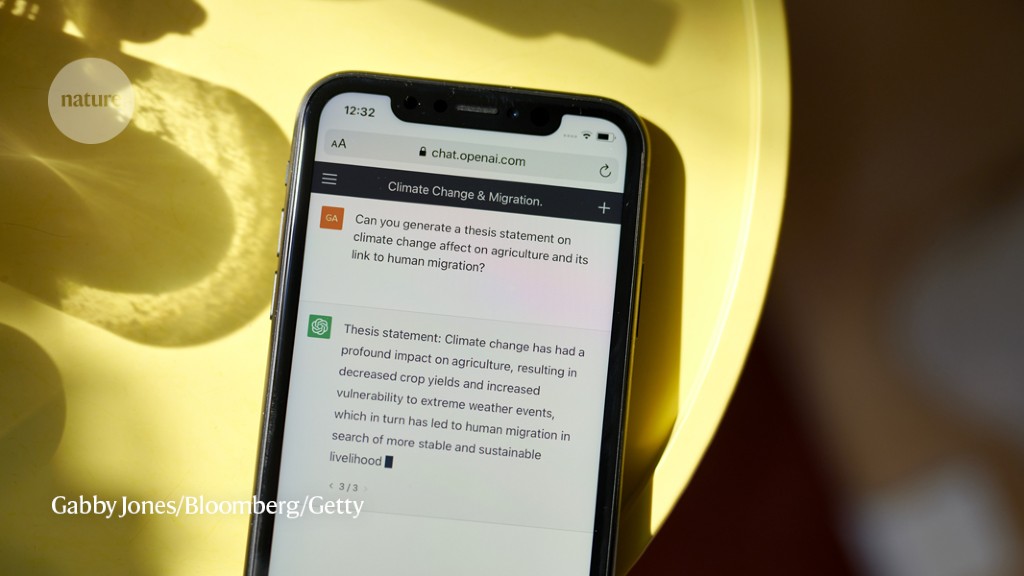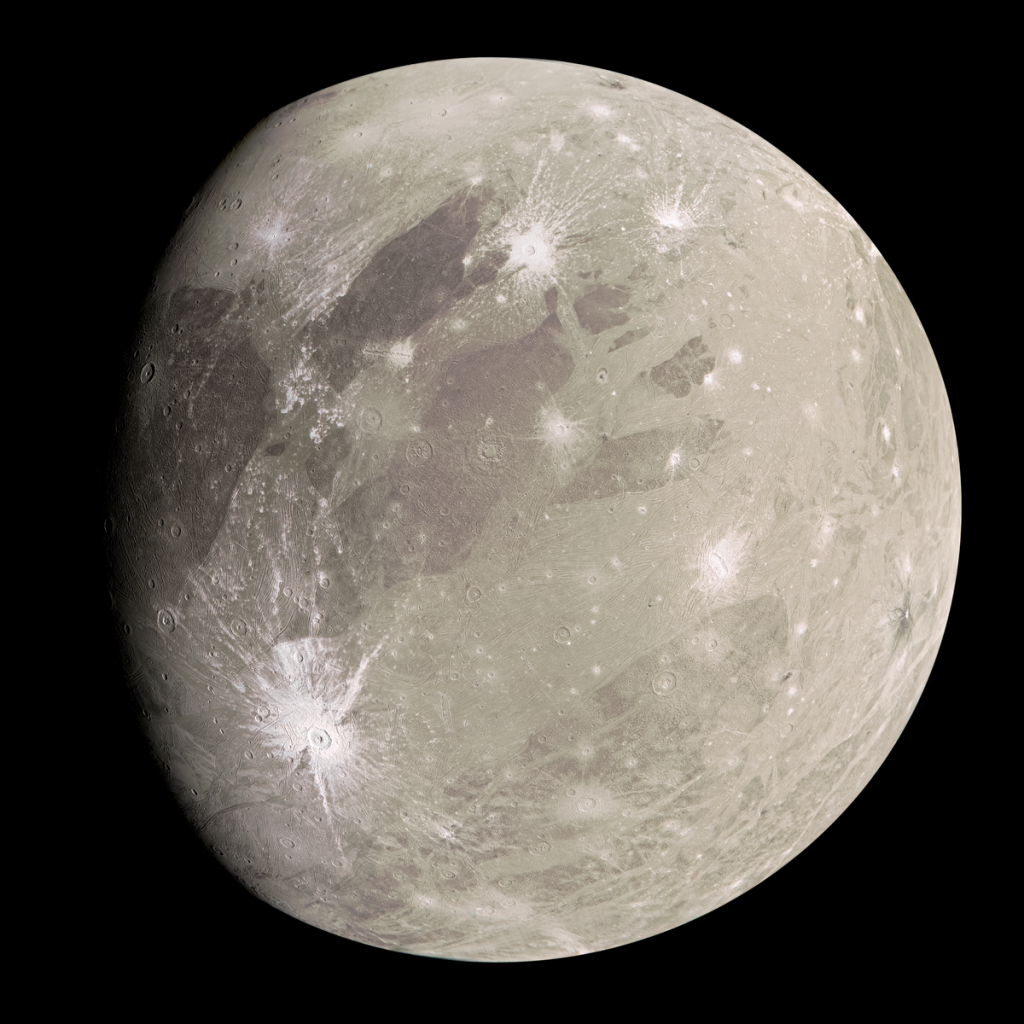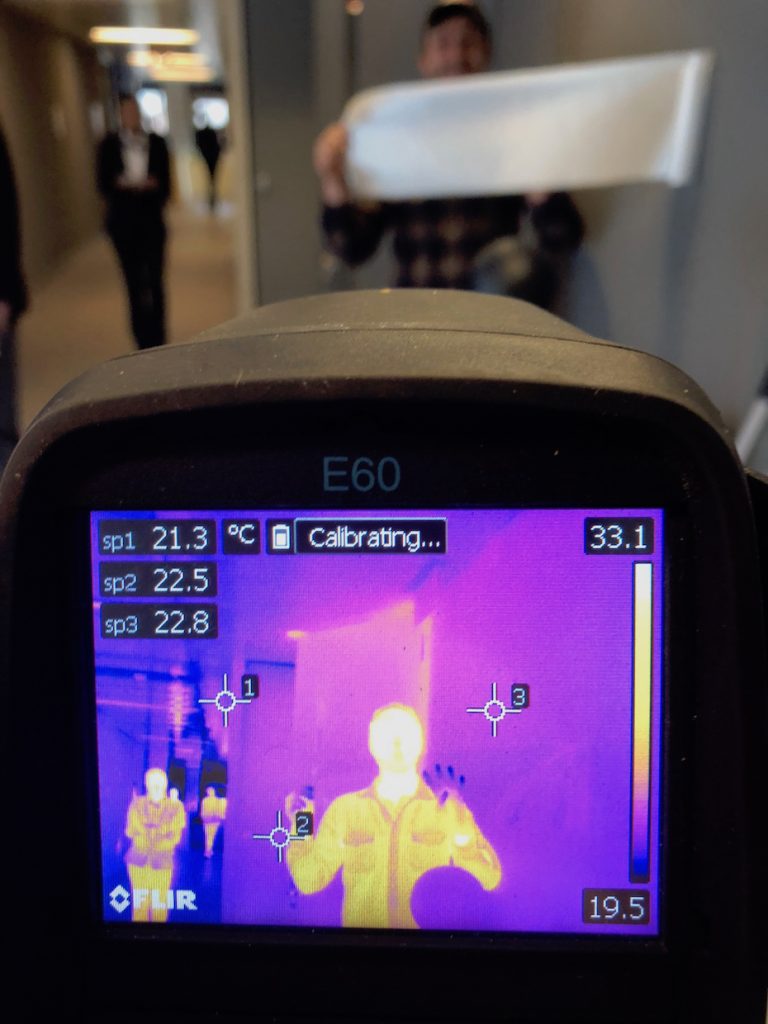आम तौर पर जब किसी बुरी आदत या लत की बात होती है तो हम धूम्रपान या मद्यपान के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक ऐसी भी लत है जिसने वयस्कों और बच्चों की बड़ी संख्या को अपनी चपेट में लिया है। यह लत खानपान की लत है।
खानपान में भी विशेष रूप से वसा और चीनी से भरपूर भोजन हमें अधिक लुभाते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो भोजन की लालसा मात्र एक भावना नहीं है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दशकों में हमारा भोजन अति-प्रोसेस्ड हो गया है। इस प्रकार का भोजन शरीर में चीनी और वसा संवेदी ग्राहियों को सक्रिय कर डोपामाइन मुक्त करने का काम करता है। प्रोसेस्ड खाद्य शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं जिससे मस्तिष्क इनका अधिक सेवन करने को प्रोत्साहित करने लगता है और लंबे समय तक इनका सेवन शरीर के लिए घातक हो सकता है। विशेषज्ञ खानपान की लत को बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके लिए सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि भोजन हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है। एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मस्तिष्क से डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होना है। नशीले पदार्थों के समान खाना खाने से भी डोपामाइन मुक्त होता है। आम समझ है कि डोपामाइन आनंद में वृद्धि करता है लेकिन यह सच नहीं है। यह हमें ऐसे व्यवहारों को दोहराने के लिए उकसाता है जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे भोजन करना और प्रजनन। जितना अधिक डोपामाइन मुक्त होगा, उस व्यवहार को दोहराने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
वसा या चीनी युक्त भोजन का सेवन करने पर हमारे मुंह का सेंसर स्ट्रिएटम को डोपामाइन मुक्त करने का संदेश भेजता है। स्ट्रिएटम मस्तिष्क का एक भाग है जो गतियों और पुरस्कार योग्य व्यवहार से जुड़ा है। लेकिन मुंह के सेंसर द्वारा डोपामाइन मुक्त होना पूरी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है।
विशेषज्ञों के अनुसार आंत में भी वसा और चीनी के लिए एक द्वितीयक सेंसर होता है और वह भी मस्तिष्क के उसी क्षेत्र को डोपामाइन मुक्त करने का संकेत देता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आंत से मस्तिष्क तक चीनी की उपस्थिति का संकेत कैसे पहुंचता है लेकिन वसा के संकेत का पता लगाया जा चुका है। ऊपरी आंत में वसा का पता लगने पर वैगस तंत्रिका के माध्यम से पश्च-मस्तिष्क को संकेत पहुंचता है जो आखिरकार स्ट्रिएटम तक जाता है।
यह देखा गया है कि चीनी व वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ स्ट्रिएटम में डोपामाइन का स्तर सामान्य से 200 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। यह स्तर निकोटीन और शराब द्वारा की जाने वाली वृद्धि के बराबर है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि शकर ने डोपामाइन के स्तर को 135 से 140 प्रतिशत तक बढ़ाया जबकि वसा ने इस स्तर को 160 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। तुलना के लिए कोकेन ने सामान्य डोपामाइन के स्तर को तीन गुना किया जबकि मेथाम्फेटामिन नेे इसे 10 गुना बढ़ाया।
जैसे-जैसे हम भोजन और मस्तिष्क के सम्बंध को समझ रहे हैं, वैसे-वैसे भोजन का उत्पादन इस तरह किया जाने लगा है कि हम खुद को रोक न पाएं। हमारे शरीरों को ऐसे खाद्य पदार्थों से पाट दिया गया है जिनमें कुछ विशिष्ट पोषक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक है – जैसे शकर, वसा और नए-नए पदार्थों के सम्मिश्रण।
औद्योगिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ स्टार्च और हाइड्रोजनीकृत वसा से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा मज़ेदार स्वाद देने वाले कृत्रिम फ्लेवर, पानी और तेल को घुलनशील रखने वाले इमल्सीफायर और खाद्य सामग्री की संरचना को संरक्षित रखने वाले स्टेबिलाइज़र्स ने हमारे भोजन को अधिक आकर्षक तो बना दिया है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया है।
विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और बुनियादी चीज़ों से बनाए खाद्य पदार्थों के बीच अंतर करना ज़रूरी है। यह अंतर आहार सम्बंधी स्वास्थ्य समस्याओं से बचने का पहला कदम हो सकता है। अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ नशे की तरह काम करते हैं। जितनी तेज़ी से कोई चीज़ आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है उतनी ही जल्दी आपको उस चीज़ की लत लगती है। इसके साथ ही डोपामाइन मुक्त होने की गति को बढ़ाने के लिए कई प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को पहले से ही थोड़ा पचाया गया होता है।
आखिर में इस पूरे मुद्दे में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रोसेस्ड खाद्य सामग्री काफी समय से सुलभ और सस्ती है तथा इसका काफी विज्ञापन भी किया जाता रहा है। लिहाज़ा, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि ये खाद्य सामग्री स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं लेकिन फिर भी वे अपने आपको रोक नहीं पाते हैं।
किसी भी पदार्थ या ड्रग की लत के सम्बंध में सहनशीलता और उसे छोड़ने के परिणाम के सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। सहनशीलता यानी किसी ड्रग (या भोजन) का इतना आदी हो जाना कि उतना ही प्रभाव प्राप्त करने के लिए इसका और अधिक सेवन करना पड़े। जबकि छोड़ने के परिणाम का सम्बंध उन शारीरिक और मानसिक लक्षणों से है जो अचानक किसी नशीले पदार्थ का उपयोग बंद या कम करने पर होते हैं।
पूर्व में यह माना जाता था कि भोजन की लत वाले लोग खानपान जारी रखते हैं ताकि खुद को उसे छोड़ने की स्थिति जैसे चिंता, मितली और सिरदर्द से बचा सकें। भोजन के मामले में, डोपामाइन की कमी की परिकल्पना यह बताती है कि अगर हम कुछ खाते हैं और इससे पर्याप्त आनंद नहीं मिलता है, तो हम तब तक खाते रहेंगे जब तक वैसा आनंद महसूस नहीं करते।
लेकिन भोजन के मानसिक असर को लेकर अभी पूरी स्पष्टता नहीं है। वर्तमान में वैज्ञानिकों के पास इस बाबत उत्तर कम, प्रश्न अधिक हैं कि हमारा शरीर भोजन का आदी कैसे हो जाता है। हम जानते हैं कि डोपामाइन ही सब कुछ नहीं है क्योंकि सिर्फ इसी से भोजन आनंददायक नहीं बनता है। हालांकि शोधकर्ताओं ने वर्ष 2012 के एक अध्ययन में पाया है कि खाना खाने से हमारे अफीमी ग्राही उत्तेजित होते हैं, जो आनंद की भावना को बढ़ाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस प्रक्रिया के बारे में कम ही जानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऊपरी आंत में एक संवेदक हमारे भोजन की पसंद-नापसंद में कुछ भूमिका निभाता है। कई अन्य इसके लिए हायपोथैलेमस को महत्वपूर्ण मानते हैं जो शरीर के तापमान से लेकर भूख के एहसास तक सब कुछ नियंत्रित करता है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://static.nationalgeographic.co.uk/files/styles/image_3200/public/gettyimages-541365978.jpg?w=1900&h=1262