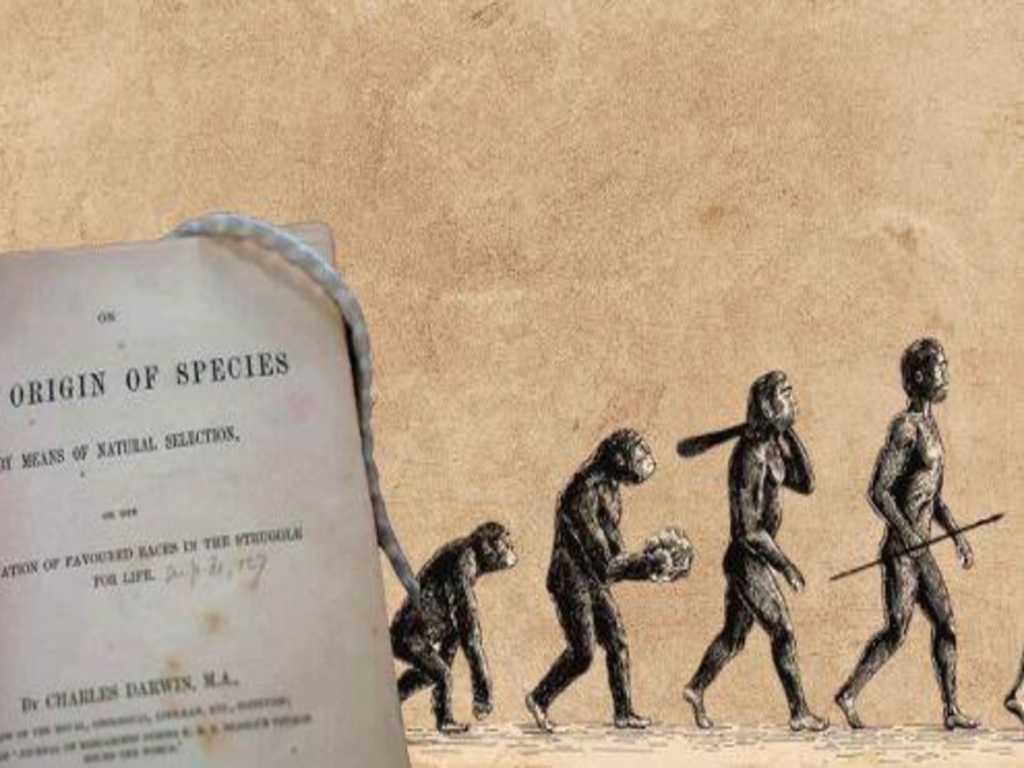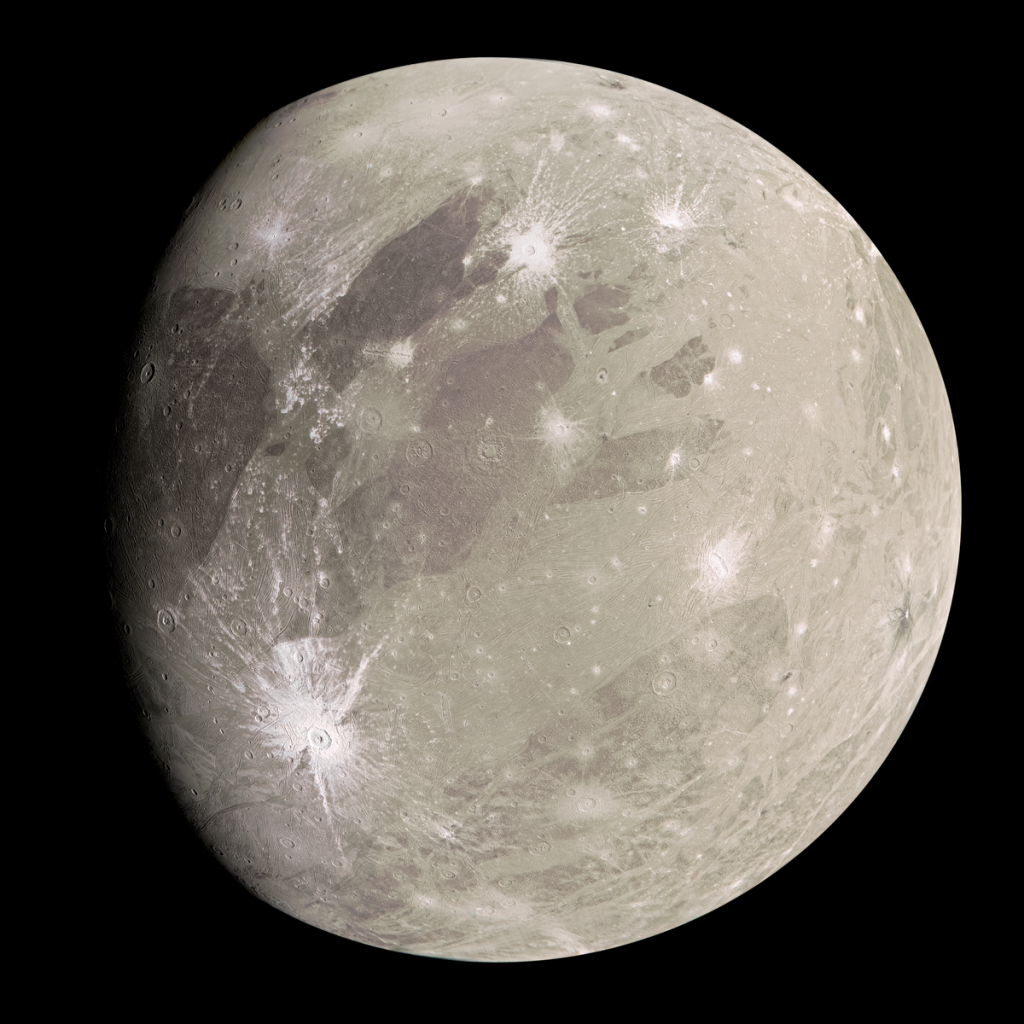सतपुड़ा, विंध्याचल या अरावली पर्वत शृंखलाओं के जंगलों में कभी फरवरी-मार्च के महीनों में पैदल चल कर देखिए; सूखे पत्तों की चरचराहट की आवाज़ साफ सुनाई देगी। मानो पत्ते कह रहे हों कि जनाब आप पतझड़ी जंगल में विचर रहे हैं। इन जंगलों में कहीं-कहीं पर तो सूखे पत्तों की यह चादर एक फीट तक मोटी होती है जो सेमल, पलाश, अमलतास, सागौन वगैरह के पत्तों के गिरने से बनी होती है।
अप्रैल-मई के महीनों में जब तेज़ गर्म हवाएं चल रही होती हैं, हवा भी सूखी होती है, धरती का कंठ भी सूखने लगता है। उस समय देखने में आता है कि इन पतझड़ी पेड़ों के ठूठ हरे होने लगते हैं। पलाश, अमलतास, सुनहरी टेबेबुइया और पांगरा फूलने लगते हैं।
लेकिन बिना पानी के यह कैसे संभव होता है? हमारे बाग-बगीचों की तरह जंगल में तो कोई पानी देने भी नहीं जाता। तब पेड़ों पर फूटने वाली नई कोपलों और फूलों के लिए भोजन-पानी कहां से आता है? जबकि ये पेड़ अपनी पाक शालाएं (पत्तियां) तो दो महीने पहले ही झड़ा चुके थे।
इस सवाल का जवाब एक शब्द ‘सुप्तावस्था’ में छुपा हुआ है। दरअसल ये पेड़-पौधे आने वाले सूखे गर्म दिनों को भांप लेते हैं। अत: आने वाली गर्मियों (या ठंडे देशों में जाड़े) के मुश्किल दिनों को टालने के लिए ये पेड़ दो-तीन महीनों की विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। जब तैयारी पूरी हो जाती है तब सूचना पटल के रूप में पेड़ों की ये लाल-पीली पत्तियां इन पेड़ों की टहनियों पर टंगी नज़र आती है कि अब दुकान बंद हो गई है। फिर कुछ ही दिनों में हवा के झोंकों से ये पत्तियां भी गिर जाती हैं।
इन पतझड़ी पेड़ों की ही तरह ठंडे देशों में ग्रिज़ली बेयर यानी भूरा भालू और डोरमाइस, जो कि एक प्रकार का चूहे जैसा रात्रिचर जीव है, सुप्तावस्था (या शीतनिद्रा) में चले जाते हैं। ग्रिज़ली भालू जाड़ा पड़ने के पहले खा-खाकर अपने शरीर में वसा की इतनी मोटी परत चढ़ा लेता है कि पूरी सर्दियों जीवित रह सके।
पतझड़ी पेड़ भी सुप्तावस्था की तैयारी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। सूर्य की ऊर्जा से वे शर्करा और अन्य पदार्थ बनाते हैं जिन्हें वे अपनी त्वचा के नीचे भंडारित करके रखते हैं। पेड़ों की त्वचा यानी उनकी मोटी छाल ऊपर से तो मरी-मरी लगती है पर अंदर से जीवित होती है। एक निश्चित बिंदु पर आकर पेड़ों का पेट भर जाता है; इस स्थिति में पेड़ थोड़े मोटे भी लगने लगते हैं। ठंडे देशों के चेरी कुल के जंगली पेड़ों की पत्तियां अक्टूबर के पहले ही लाल होने लगती हैं और इसका सीधा अर्थ यह होता है कि उनकी छाल और जड़ों में भोजन संग्रह करने वाले स्थान भर चुके हैं, और यदि वे और शर्करा बनाते हैं तो उसे भंडारित करने के लिए अब उनके पास कोई जगह नहीं बची है।
ठंडे देशों में पहली ज़ोरदार बर्फबारी होने तक उन्हें अपनी सभी गतिविधियां बंद करनी होती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण पानी है; सजीवों के उपयोग हेतु इसे तरल अवस्था में होना ज़रूरी होता है। परंतु लगता है कुछ पेड़ अभी जाड़े के मूड में नहीं हैं।
ऐसा दो कारणों से होता है पहला कि वे अंतिम गर्म दिनों का उपयोग ऊर्जा संग्रह के लिए करते रहते हैं, और दूसरा अधिकांश प्रजातियां पत्तियों से ऊर्जा संग्रह कर अपने तनों और जड़ों में भोजन भेजने में लगी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि उन्हें अपने हरे रंग के क्लोरोफिल को उसके घटकों में तोड़कर उन घटकों को संग्रह करना होता है ताकि आने वाले बसंत में नई पत्तियों में क्लोरोफिल के निर्माण में इनका उपयोग हो सके।।
गर्म देशों के हों या ठंडे देशों के, पतझड़ी पेड़ों के लिए बासी पत्तियों को खिराना एक प्रभावी सुरक्षा योजना होती है। यह पेड़ों के लिए अपने व्यर्थ या अवांछित पदार्थों को त्यागने का एक अवसर भी होता है। व्यर्थ पदार्थ ज़मीन पर इधर-उधर उनकी त्यागी हुई पत्तियों के रूप में उड़ते रहते हैं। जब पत्तियों में भंडारित ऊर्जा वापस शाखाओं और जड़ों में अवशोषित कर ली जाती है, तब पेड़ों की कोशिकाओं में एक विलगन परत बनती है जो पत्तियों और शाखाओं के बीच का संपर्क बंद कर देती है। ऐसे में हल्की हवा का झोंका लगते ही पत्तियां ज़मीन पर आ जाती है।
यह तो हुई ऊर्जा की बात। पानी की व्यवस्था के लिए जब पानी उपलब्ध होता है तब जड़ें उसे तनों की छाल में व स्वयं अपने आप में संग्रह करती रहती हैं। पौधों का एक नाम पादप भी है अर्थात पांव से पानी पीने वाले जीव। पांव (जड़ों) से पीकर पानी को तने और जड़ों में संग्रह कर लिया जाता है।
मई-जून के महीनों में इन मृतप्राय पेड़ों में नई पत्तियां और फूलों के खिलने के लिए जो ऊर्जा और पानी लगते हैं, वे शाखाओं और जड़ों के इसी संग्रह से मिलते हैं। किंतु अब बहाव की दिशा उल्टी है।
पानी का परिवहन
वनस्पति विज्ञान की किताबें कहती हैं कि सौ से डेढ़ सौ फीट ऊंचे पेड़ों में पानी को ज़मीन से खींचकर शीर्ष तक पहुंचाने में पत्तियों में होने वाली वाष्प उत्सर्जन क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सिद्धांत को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल नाम दिया गया है। पर यह सवाल गर्मियों के दिन में बड़ा रोचक हो जाता है – जब पेड़ों पर पानी खींचने वाले छोटे-छोटे पंप अर्थात पत्तियां नहीं हैं, तो फिर पत्ती विहीन पेड़ों के शीर्ष पर फूटने वाली नई कोपल और कलियों को पानी कौन और कैसे पहुंचाता है। अत: लगता है मामला कुछ और भी है जो हम अभी तक नहीं जानते। सचमुच प्रकृति के क्रियाकलाप अद्भुत हैं और जानने को आज भी बहुत कुछ है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://forsythlodge.com/wp-content/uploads/2022/03/Trees-in-Satpura.jpg