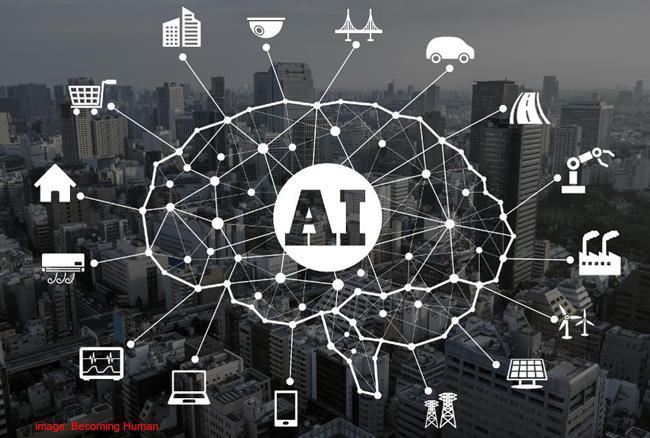देश में लगातार फैल रहे बोतलबंद पानी के कारोबार पर संसद की स्थाई समिति ने कई सवाल खड़े किए हैं। समिति की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पेयजल के कारोबार से अरबों रुपए कमाने वाली कंपनियों से सरकार भूजल के दोहन के बदले में न तो कोई शुल्क ले रही है और न ही कोई टैक्स वसूलने का प्रावधान है। समिति ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूजल का दोहन करने वाली इन कंपनियों से भारी-भरकम जल-कर वसूलने की सिफारिश की है। समिति का विचार है कि इससे जल की बरबादी पर भी अंकुश लगेगा। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में जल संसाधन सम्बंधी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की है।
रिपोर्ट का शीर्षक है ‘उद्योगों द्वारा जल के व्यावसायिक दोहन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव’। इसमें केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय की खूब खिंचाई की गई है। समिति ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना सरकार का नैतिक और प्राथमिक कर्तव्य है। किंतु सरकार इस दायित्व के पालन में कोताही बरत रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने भूजल के दोहन के लिए 375 बोतलबंद पेयजल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए हैं। इसके इतर 5,873 पेयजल इकाइयों को बीआईएस से बोतलबंद पानी उत्पादन के लायसेंस मिले हैं। ये कंपनियां हर साल 1.33 करोड़ घनमीटर भूजल जमीन से निकाल रही हैं। चिंताजनक पहलू यह है कि ये कंपनियां कई ऐसे क्षेत्रों में भी जल के दोहन में लगी हैं जहां पहले से ही जल का अधिकतम दोहन हो चुका है।
समिति ने सवाल उठाया है कि न तो सरकार के पास ऐसा कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड है कि वाकई ये इकाइयां कुल कितना पानी निकाल रही हैं और न ही इनसे किसी भी प्रकार के टैक्स की वसूली की जा रही है जबकि ये देशी-विदेशी कंपनियां करोड़ों-अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं और इनसे राजस्व प्राप्त करके जन-कल्याण में लगाने की ज़रूरत है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जनता को शुद्ध और स्वच्छ जल की आपूर्ति को केवल निजी उद्योगों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार देता है। लेकिन जीने की मूलभूत सुविधाओं को बिंदुवार परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए आज़ादी के 70 साल बाद भी पानी की तरह भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जीने के बुनियादी मुद्दे पूरी तरह संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं आए हैं। यही वजह रही कि 2002 में केंद्र सरकार ने औद्योगिक हितों को लाभ पहुंचाने वाली ‘जल-नीति’ पारित की और निजी कंपनियों को पेयजल का व्यापार करने की छूट दे दी गई। भारतीय रेल भी ‘रेलनीर’ नामक उत्पाद लेकर बाज़ार में उतर आई।
पेयजल के इस कारोबार की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। यहां शिवनाथ नदी पर देश का पहला बोतलबंद पानी संयंत्र स्थापित किया गया। इस तरह एकतरफा कानून बनाकर समुदायों को जल के सामुदायिक अधिकार से अलग करने का सिलसिला चल निकला। यह सुविधा युरोपीय संघ के दबाव में दी गई थी। पानी को वि·ा व्यापार के दायरे में लाकर पिछले एक-डेढ़ दशक के भीतर एक-एक कर विकासशील देशों के जल रुाोत अंधाधुंध दोहन के लिए इन कंपनियों के हवाले कर दिए गए। इसी युरोपीय संघ ने दोहरा मानदंड अपनाकर ऐसे नियम-कानून बनाए हुए हैं कि वि·ा के अन्य देश पश्चिमी देशों में आकर पानी का कारोबार नहीं कर सकते हैं।
युरोपीय संघ विकासशील देशों के जल का अधिकतम दोहन करना चाहता है, ताकि इन देशों की प्राकृतिक संपदा का जल्द से जल्द नकदीकरण कर लिया जाए। पानी अब केवल पीने और सिंचाई का पानी नहीं रह गया है, बल्कि विश्व बाज़ार में ‘नीला सोना’ के रूप में तब्दील हो चुका है। पानी को लाभ का बाज़ार बनाकर एक बड़ी आबादी को जीवनदायी जल से वंचित करके आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को जल उपभोक्ता बनाने के प्रयास हो रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया में देखते-देखते पानी का कारोबार 40 हज़ार 500 अरब डॉलर का हो गया है।
प्रमुख राज्यों में बोतलों में भरने के लिए भूजल निकासी
| प्रांत | कंपनियों की संख्या | प्रतिदिन निकासी (घन मीटर) |
| आंध्र प्रदेश | 41 | 55 |
| उत्तर-प्रदेश | 111 | 941 |
| गुजरात | 24 | —- |
| कर्नाटक | 63 | —- |
| तमिलनाड़ु | 374 | 1000 |
भारत में पानी और पानी को शुद्ध करने के उपकरणों का बाज़ार लगातार फैल रहा है। देश में करीब 85 लाख परिवार जल शोधन उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं। भारत में बोतल और पाउच में बंद पानी का 11 हज़ार करोड़ का बाजार तैयार हो चुका है। इसमें हर साल 40 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस पानी के करीब एक सौ ब्रांड प्रचलन में हैं और 1200 से भी ज्यादा संयंत्र लगे हुए हैं। देश का हर बड़ा कारोबारी समूह इस व्यापार में उतरने की तैयारी में है। कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भारत में ओम्नी प्रोसेसर संयंत्र लगाना चाहते हैं। इस संयंत्र से दूषित मलमूत्र से पेयजल बनाया जाएगा।
भारतीय रेल भी बोतलबंद पानी के कारोबार में शामिल है। इसकी सहायक संस्था इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ‘रेल नीर’ नाम से पानी पैकिंग करती है। इसके लिए दिल्ली, पटना, चैन्नई और अमेठी सहित कई जगह संयंत्र लगे हैं। उत्तम गुणवत्ता और कीमत में कमी के कारण रेल यात्रियों के बीच यह पानी लोकप्रिय है। अलबत्ता, निजी कंपनियों की कुटिल मंशा है कि रेल नीर को घाटे के सौदे में तब्दील कराकर सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम को बाज़ार से बेदखल कर दिया जाए। तब कंपनियों को रेल यात्रियों के रूप में नए उपभोक्ता मिल जाएंगे।
वर्तमान में भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यहां हर साल 250 घन किमी पानी धरती के गर्भ से खींचा जाता है, जो विश्व की कुल खपत के एक चौथाई से भी ज़्यादा है। इस पानी की खपत 60 फीसदी खेतों की सिंचाई और 40 प्रतिशत पेयजल के रूप में होती है। इस कारण 29 फीसदी भूजल के रुाोत अधिकतम दोहन की श्रेणी में आकर सूखने की कगार पर हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी का बढ़ता दोहन इन रुाोतों के हालात और नाज़ुक बना रहा है। कई कारणों से पानी की बर्बादी भी खूब होती है। आधुनिक विकास और रहन-सहन की पश्चिमी शैली अपनाना भी पानी की बर्बादी का बड़ा कारण बन रहा है। 25 से 30 लीटर पानी सुबह मंजन करते वक्त नल खुला छोड़ देने से व्यर्थ चला जाता है। 300 से 500 लीटर पानी टब में नहाने से खर्च होता है। जबकि परंपरागत तरीके से स्नान करने में महज 25-30 लीटर पानी खर्चता है। एक शौचालय में एक बार फ्लश करने पर कम से कम दस लीटर पानी खर्च होता है। 50 से 60 लाख लीटर पानी मुंबई जैसे महानगरों में रोज़ाना वाहन धोने में खर्च हो जाता है जबकि मुंबई भी पेयजल का संकट झेल रहा है। 17 से 44 प्रतिशत पानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में वॉल्वों की खराबी से बर्बाद हो जाता है।
पेयजल की ऐसी बर्बादी और पानी के निजीकरण पर अंकुश लगाने की बजाय सरकारें पानी को बेचने की फिराक में ऐसे कानूनी उपाय लागू करने को तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र भी कमोबेश इसी विचार को समर्थन देता दिख रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने पानी और स्वच्छता को बुनियादी मानवाधिकार घोषित किया हुआ है लेकिन इस बाबत उसके अजेंडे में पानी एवं स्वच्छता के अधिकार का वास्ता मुफ्त में मिलने से कतई नहीं है। बल्कि इसका मतलब यह है कि ये सेवाएं सबको सस्ती दर पर हासिल हों। साफ है, पानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाज़ार के हवाले करने की साजि़श रची जा रही है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://guardian.ng/wp-content/uploads/2016/12/stored-bottled-water.jpg