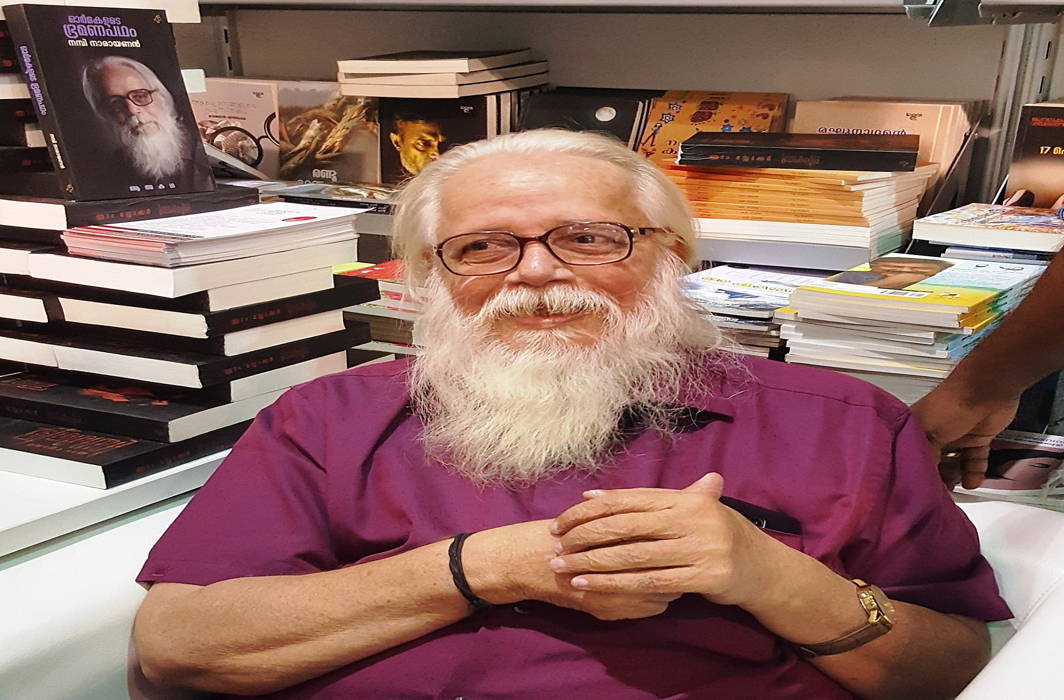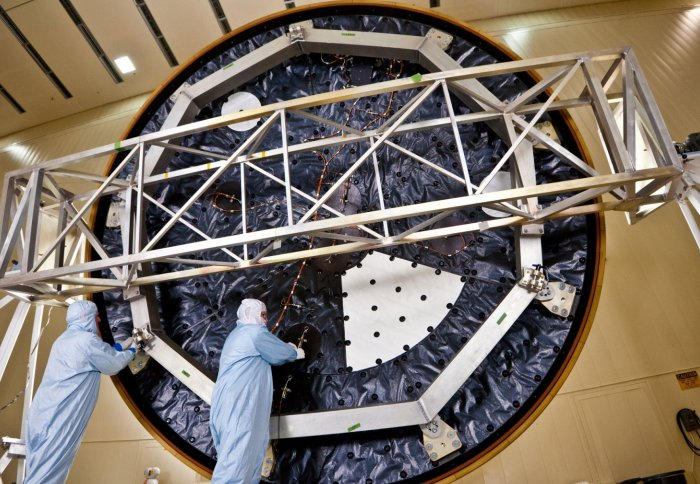कुछ ततैया पौधों पर परजीवी होती हैं। उनमें से एक है बेलोनानीमा ट्रीटी जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा में पाई जाती है। यह एक ओक वृक्ष पर अंडे देती है जिनसे इल्लियां निकलती हैं। ये इल्लियां कुछ वृद्धि हारमोन छोड़ती हैं जिनकी वजह से पौधों पर गठानें बन जाती हैं। ये गठानें युवा ततैया को रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं। इन छोटी-छोटी गठानों को वैज्ञानिक ‘गाल’ कहते हैं। ये गठानें ततैया की इल्लियों को लगातार पोषक पदार्थ भी उपलब्ध कराती हैं। इन ततैया के लिए तो ये गठानें वरदान हैं पर पौधे के लिए अभिशाप क्योंकि उनका पोषण ततैया के बच्चे चुरा लेते हैं।
पोषक पदार्थों से लबरेज़ ये लड्डू जैसे गाल अन्य परजीवियों की निगाहों से ओझल रह जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि पोषक पदार्थों से भरे ये गाल लव वाइन नामक एक परजीवी लता के निशाने पर हैं। एक सर्वे से पता चला कि यह लव वाइन (प्रेमलता) ऐसे गाल के आसपास लिपटी रहती है। ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इस प्रेमलता ने वास्तव में गाल की दीवार को भेद रखा है जिसमें परजीवी ततैया वृद्धि कर रही थी। यह लता वहां से पोषक पदार्थ भी चूसती है। मज़ेदार बात है कि यह पोषक पदार्थ वह सीधे वृक्ष से नहीं बल्कि ततैया के शरीर से प्राप्त करती है। अंतत: वहां ततैया की लाश ही शेष बचती है। बेल के तो मज़े हैं पर ततैया की शामत। इसी को कहते हैं चोर के घर चोरी।
इस खोज के बाद वैज्ञानिकों ने ‘परजीवी पर परजीवी’ सम्बंध की और जांच-पड़ताल की। उन्होंने पाया कि 51 मामलों में प्रेमलता ततैया के बनाए गाल पर चिपकी थी, और उनमें से आधे से ज़्यादा में ततैया मृत मिली। करंट बायोलॉजी के एक ताज़ा अंक में यह रपट प्रकाशित हुई है। 101 गाल पर प्रेमलता नहीं लिपटी थी और उनमें से केवल 2 में ही ततैया मृत मिली। पेड़ के लिए इसका क्या अर्थ है इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट पता नहीं है।
क्या है प्रेमलता
प्रेमलता यानी लव वाइन एक पूर्ण परजीवी बेल है। यह अमेरिका, इन्डोमलाया, ऑस्ट्रेलेशिया, पोलीनेशिया और कटिबंधीय अफ्रीका की मूल निवासी है। इसका वानस्पतिक नाम कैसिथा फिलीफॉर्मिस है। वैसे कैरेबियन क्षेत्र में कई बेलों को लव वाइन कहा जाता है। यह उनमें से एक है। लव वाइन अर्थात प्रेमलता नामकरण के पीछे यह मान्यता है कि इसमें कामोत्तेजक गुण होते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया में इसे डोडर-लॉरेल भी कहते हैं और डेविल्स गट्स भी। दक्षिण भारत में छांछ को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका औषधीय महत्व भी है।
भारत में ऐसी ही एक परजीवी बेल बहुतायत से मिलती है जिसका नाम है अमरबेल (कस्कुटा)। इसकी करीब 100-170 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इनका तना नारंगी, लाल या हल्का पीला होता है। इस पूर्ण परजीवी बेल का बीज अंकुरित होकर पौधों के आसपास सर्पिल क्रम में वृद्धि करता है जब तक कि यह किसी सही पोषक पौधे के सम्पर्क में न आ जाए। इसकी पत्तियां शल्क पत्र के रूप में होती हैं, वे भी मात्र 1 मि.मी. लंबी। पत्तियां सूक्ष्म हैं और तना भी हरा नहीं होता। यानी पूरी बेल क्लोरोफिल विहीन होती है। ऐसे में इस बेल के पास दूसरों से भोजन चुराने के अलावा कोई और चारा नहीं है।
गंगा सहाय पांडेय तथा कृष्ण चंद्र चुनेकर द्वारा सम्पादित भाव प्रकाश निघण्टु में अमरबेल नाम कस्कुटा रिफ्लेक्सा के लिए और आकाशबेल कैसिथा फिलीफॉर्मिस के लिए प्रयुक्त किया गया है। दोनों ही भारत में मिलती है। अमरबेल लगभग सभी जगह और आकाश बेल समुद्र तट के पेड़ों और झाड़ियों पर। वासुदेवन नायर अपनी किताब कॉन्ट्रोवर्सियल ड्रग प्लांट्स में कहते हैं कि इसके बारे में भ्रम है कि आकाश वल्ली आखिर कौन है – कस्कुटा रिफ्लेक्सा या कैसिथा फिलीफार्मिस।
क्यों बनते हैं पौधों पर गाल
पौधो पर विभिन्न कीटों द्वारा बनाए जाने वाले ये गाल्स इन जीवों के लिए सुरक्षित वास स्थान और भोजन का स्रोत दोनों का कार्य करते हैं। इन गठानों के अंदर ये कीट परजीवियों और शिकारियों से आंशिक रूप से सुरक्षित रहते हैं।
गाल की आंतरिक भित्ती नम होती है जिसका द्रव सामान्यत: प्रोटीन और शर्करा से भरा होता है। जबकि पौधों के सामान्य ऊतकों में इन पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। पोषक पदार्थों की सहज उपलब्धता के कारण कई कीट इन गठानों में सहयोगी के रूप में रहते हैं। इन्हें जीव वैज्ञानिक पर-निलय वासी (इनक्विलाइन) कहते हैं। यानी दूसरे के घर में रहने वाले। उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक ने एक गाल में ऐसे 31 रहवासियों की सूची बनाई है। जिनमें 10 पर-निलय वासी, 16 परजीवी और 5 यदा-कदा आने वाली प्रजातियां शामिल थीं।
ये गाल्स बैक्टीरिया, कवक, कृमि, माहू, मिजेस, ततैया और घुन बनाते हैं। यदि प्रभावित भागों पर अंडे या कीट दिखाई दें तो यह पता लगाया जा सकता है कि ये गाल कीट ने बनाए हैं या नहीं। ओक के पौधों पर गाल्स बहुतायत से देखे जाते हैं। ओक 500 से ज़्यादा ततैया, 3 एफिड (माहू), घुन और मिजेस का पोषक पौधा है जो इसकी पत्तियों और टहनियों पर गाल्स बनाते हैं।
सामान्यत: कीट और पिस्सू गाल बनाने वाले सबसे आम जीव हैं। कुछ लोग इन्हें बागवान भी कहते हैं क्योंकि ये पौधों पर नई रचनाएं बनाते हैं। पौधों मे दो तरह के गाल्स देखे जाते हैं – खुले और बंद। खुले गाल एफिड, काकसिड और माइट्स जैसे जीव बनाते हैं। जबकि बंद प्रकार के गाल कीटों की इल्लियों द्वारा बनाए जाते हैं।
पत्तियों और तनों पर बने ये गाल ज़्यादा जाने-पहचाने हैं बजाय उन कीटों के जो इन्हें बनाते हैं। ये कीट बहुत छोटे होते हैं और इन्हें पहचानना भी मुश्किल होता हैं। गाल बनाने वाले कीट अपने अंडे पोषक पौधे के ऊपर या अंदर देते हैं। अंडों से निकली इल्ली जहां पौधे के संपर्क में आती है, वहीं से गठान बनने की शुरुआत होती है।
ये गठानें असामान्य वृद्धि का नतीजा होती हैं और पत्तियों, शाखाओं, जड़ों और फूलों पर भी बनती हैं। ये गठानें इल्लियों द्वारा इन भागों को कुतरने के फलस्वरूप उत्पन्न उद्दीपन के कारण बनना शुरू होती हैं। ये गेंद, घुंडी, मस्सों आदि के रूप में होती है। इस तरह की गठानें आप करंज, सप्तपर्णी और गूलर, पाकड़ की पत्तियों पर देख सकते हैं। एक समय में ऐसा माना जाता था कि इनमें औषधीय गुण होते हैं। वर्तमान में इनका इस हेतु उपयोग नहीं किया जाता।
जहां तक इनके आर्थिक महत्व का सवाल है, इनमें टैनिक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में होता है। युरोपियन सिनिपिड द्वारा बनाए गए गाल से लगभग 65 प्रतिशत टैनिक अम्ल जबकि अमेरिकन सुमेक गाल से 50 प्रतिशत टैनिक अम्ल प्राप्त होता है। इन गाल से रंग भी मिलते हैं। टर्की रेड रंग मैड एप्पल गाल से निकाला जाता है। पूर्वी अफ्रीका में इन गठानों का उपयोग टेटू बनाने में रंग के लिए किया जाता था। सिनिप्स गैली टिंक्टोरी नामक कीट से उत्पन्न गाल से स्याही बनायी जाती है। एक समय कुछ देशों में कानूनी दस्तावेज़ इसी स्याही से लिखे जाते थे। यहां तक कि यूएस टे्रज़री, बैंक आफ इंग्लैंड, जर्मन चांसलरी और डेनमार्क सरकार के पास एलेप्पो गाल से स्याही बनाने के विशेष फार्मूले हैं। अधिकांश गाल्स का स्वाद उनके पोषक पौधे जैसा होता है।
तो इस गाल में हैं शामिल हैं, एक स्वपोषी पौधा (ओक), एक शाकाहारी परपोषी जन्तु (बेलोनानीमा ट्रीटी) और साथ में एक परजीवी प्रेमलता (कैसिथा फिलीफॉर्मिस)। ऐसा तिहरा सम्बंध जीवजगत में काफी पाया जाता है और जीवन की रणनीति का एक हिस्सा है।(स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://static1.squarespace.com/static/544591e6e4b0135285aeb5b6/t/5b7b7e7d758d462bead7ec09/1534819977361/?format=750w