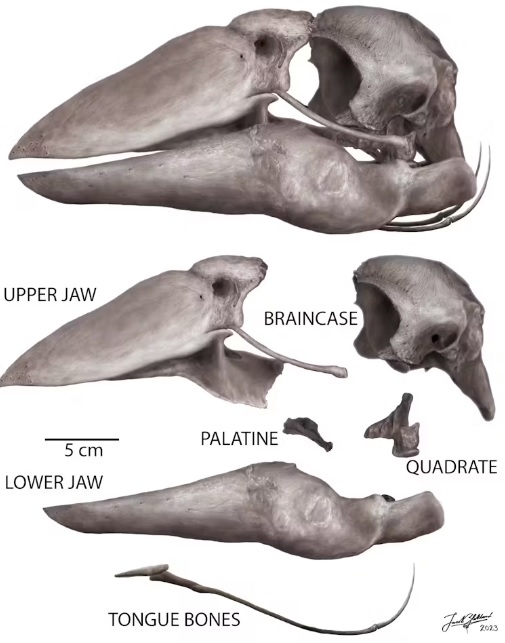वैसे तो पहले भी कुछ अध्ययनों में देखा जा चुका है कि कौवों में संख्या ताड़ने की क्षमता होती है। जैसे यदि उनके सामने कई डिब्बे रखकर मात्र 6 डिब्बों में खाने की चीज़ें रखी जाएं तो वे मात्र 6 डिब्बों को पलटाने के बाद रुक जाते हैं। या यदि कौवे किसी बगीचे में हैं और कुछ मनुष्य वहां घुसें तो वे छिप जाते हैं। और तब तक छिपे रहते हैं जब तक कि सारे मनुष्य निकल न जाएं। ऐसा देखा गया था कि वे यह ‘गिनती’ 16 तक कर पाते हैं। इसी प्रकार से एक प्रयोग में यह भी देखा गया था कि यदि किसी स्क्रीन पर कुछ बिंदु अंकित हों तो वे ताड़ सकते हैं कि दो समूहों में बिंदुओं की संख्या बराबर है या नहीं।
और अब जर्मनी के टुबिंजेन विश्वविद्यालय के जंतु वैज्ञानिक एंड्रियास नीडर और उनके साथियों ने इसमें एक नया आयाम जोड़ा है। साइन्स पत्रिका में प्रकाशित अपने शोधपत्र में इस टीम ने बताया है कि कौवों की यह क्षमता मनुष्यों में संख्या कौशल के विकास को समझने में सहायक हो सकती है।
जर्मनी के शोधकर्ताओं ने तीन कैरियन कौवों (Corvus corone) के साथ काम किया। इन कौवों को आदेशानुसार कांव करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका था। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक इन्हें यह सिखाया गया कि स्क्रीन पर 1, 2, 3 या 4 के दृश्य संकेत दिखने पर उन्हें उतनी ही संख्या में कांव करना है। उन्हें ऐसे श्रव्य संकेतों से भी परिचित कराया गया जो एक-एक अंक से जुड़े थे।
प्रयोग के दौरान ये कौवे स्क्रीन के सामने खड़े होते थे और उन्हें दृश्य या श्रव्य संकेत दिया जाता था। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे उस संकेत से मेल खाती संख्या में कांव करेंगे और यह काम पूरा करने के बाद वे ‘एंटर कुंजी’ पर चोंच मारेंगे। यदि वे सही करते तो उन्हें पुरस्कार स्वरूप लजीज़ व्यंजन दिया जाता।
कौवे अधिकांश बारी सही रहे। कम से कम उनके प्रदर्शन को मात्र संयोग का परिणाम तो नहीं कहा जा सकता।
प्रयोग करते-करते शोधकर्ताओं को यह भी समझ आया कि वे कौवे की पहली कांव को सुनकर यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि वह कुल कितनी बार कांव करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कौवा पहले से ही कांव की संख्या की योजना बना लेता है अर्थात यह प्रक्रिया सचमुच संज्ञानात्मक नियंत्रण में है। अलबत्ता, ऐसा नहीं था कि कौवे हर बार सटीक होते थे। कभी-कभार वे कम या ज़्यादा बार कांव भी कर देते थे। लेकिन यह भी पूर्वानुमान किया जा सकता था।
लिहाज़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये तीन कौवे वास्तव में गिन रहे थे जिसके लिए संख्याओं की सांकेतिक समझ ज़रूरी है लेकिन हो सकता है कि उनका प्रदर्शन इस समझ के विकास का अग्रदूत हो। आगे और शोध ही इस सवाल पर रोशनी डाल सकेगा। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://th-thumbnailer.cdn-si-edu.com/egyg-6AOBCx5QHygyWnN7Eoaq4s=/1000×750/filters:no_upscale():focal(1685×1171:1686×1172)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/11/22/11228101-b1b2-4366-b675-f7f8d566f262/51984109685_632ca93abb_o.jpg