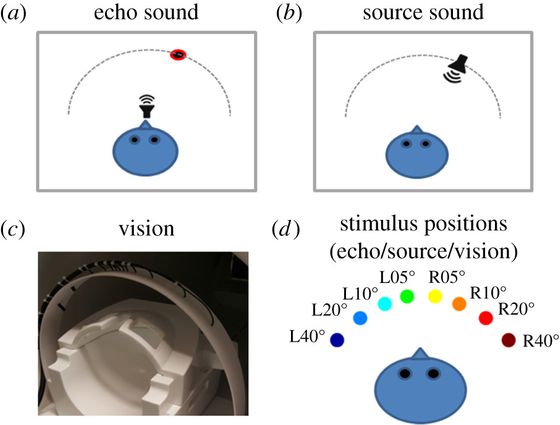भारत सितंबर
महीना खत्म होने को है और भारत में सेमीनार और सम्मेलनों के आयोजन का मौसम शुरू हो
गया है। आम तौर पर कॉन्फ्रेंस में एक व्यापक विषयवस्तु पर विविध विषयों के
विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। दूसरी ओर, सेमीनार
में किसी एक खास विषय या उपविषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है जो मिलकर
उस विषय पर विचारों का आदान-प्रदान और समीक्षा करते हैं। सम्मेलनों में श्रोता या
प्रतिभागी किसी ऐसे विषय पर तकरीरें सुनते हैं जिससे वे परिचित नहीं हैं। इस तरह
से यह उनके लिए सीखने का एक अवसर होता है। विशेष-थीम पर केंद्रित सेमीनार में प्रतिभागी
सेमीनार में मात्र श्रोता नहीं होते, वे
उस विषय से परिचित होते हैं और विषय की बारीकियां सुनते हैं,
जिसमें से वे कुछ नया सीखते हैं,
सराहते हैं और उससे कुछ ग्रहण करते हैं। इस तरह सम्मेलन और
सेमीनार दोनों उपयोगी होते हैं।
लेकिन
इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। प्रस्तुतीकरण या तकरीर के दौरान कुछ या कई श्रोता
सिर हिलाते-हिलाते
ऊंघने लगते हैं और झपकी ले लेते हैं। इसे नॉड ऑफ कहते हैं। इस संदर्भ में 15 साल पहले (दिसंबर 2004 में) केनेडियन मेडिकल
एसोसिएशन जर्नल में के. रॉकवुड और साथियों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में बताया गया
था कि व्याख्यानों के दौरान श्रोता ऐसा क्यों करते हैं,
कितनी दफा करते हैं और झपकी आने के क्या कारक हैं। इस
हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक शोधपत्र में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने चुपके
से एक ही समूह का लगातार (कोहॉर्ट) अध्ययन किया जिसमें
उन्होंने पता लगाया कि वैज्ञानिक मीटिंग के दौरान श्रोता-चिकित्सक कितनी बार झपकी लेते हैं,
और झपकी आने के पीछे क्या कारक हो सकते हैं।
एक
दो-दिवसीय
व्याख्यान, जिसमें तकरीबन 120 लोग शामिल हुए थे,
के अध्ययन में उन्होंने पाया कि प्रत्येक 100 प्रतिभागी पर प्रति
व्याख्यान झपकी की संख्या (नॉडिंग ऑफ इवेंट पर लेक्चर, एनओईएल) 15-20 मिनट के व्याख्यान
के दौरान 10 रही,
लेकिन व्याख्यान 30-40 मिनट का होने पर बढ़कर तकरीबन 22 हो गई थी। अर्थात
जितना लंबा व्याख्यान उतनी अधिक झपकी संख्या (एनओईएल)।
अध्ययन
में यह भी पता चला कि झपकी-प्रेरित सिर हिलाना और वक्ता की बात से सहमति पर सिर हिलाना
एकदम अलग-अलग
हैं। इनमें सिर हिलाने का तरीका, समय और आवृत्ति अलग-अलग होती है।
ऐसा
क्यों होता है? और किन कारणों से
होता है? इसके कई कारक सामने
आए और ये कारक हैं माहौल (जैसे
मद्धिम रोशनी, कमरे का तापमान,
आरामदायक बैठक व्यवस्था), दृश्य-श्रव्य गड़बड़ी (जैसे खराब स्लाइड,
माइक्रोफोन पर ना बोलना), शरीर की दैनिक लय (सुबह-सुबह के समय,
भोजन के बाद या भारी नाश्ता या लंच के बाद नींद आना) और वक्ता सम्बंधी
कारण (जैसे
नीरस तरीके से बोलना या उबाऊ भाषण)।
आजकल
तो सेमीनार या सम्मेलनों में कई श्रोता मोबाइल, लैपटॉप
वगैरह साथ लेकर जाते हैं। हालांकि आयोजकों की ओर से निर्देश दिए जाते हैं कि
व्याख्यान के दौरान मोबाइल फोन या तो बंद कर दिए जाएं या साइलेंट मोड पर रखे जाएं
लेकिन व्याख्यान उबाऊ लगने पर श्रोता अपने मोबाइल या लैपटॉप में मशगूल हो जाते हैं,
जिससे व्याख्यान के दौरान झपकी की संख्या (एनओईएल) में कमी दिखती है।
जब आयोजकों ने व्याख्यान के दौरान मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल ना करने पर सख्ती
दिखाई तो व्याख्यान के दौरान झपकी की संख्या में वृद्धि भी देखी गई।
अध्ययन
में आगे अध्ययनकर्ताओं ने झपकी लेने वालों को टोका और अदब के साथ उनसे पूछा कि
उन्हें झपकी क्यों आई। पहले तो जब उन्हें यह बताया गया कि इस व्याख्यान के दौरान
सिर्फ उन्हें ही नहीं अन्य लोगों को भी झपकी आई तो उनमें से कई लोगों को इस बात की
तसल्ली हुई कि यह उनका दोष नहीं था। जब उनसे यह पूछा गया कि इस तरह के व्याख्यान
में क्या वे आगे भी शामिल होंगे तो कुछ ने लोगों ने हां में जवाब दिया और कहा कि
उन्हें हमेशा एक झपकी की ज़रूरत रहती है, कुछ
ने कहा कि यदि इसके लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा तो वे शामिल होंगे और कुछ ने जवाब
में दांत दिखा दिए। जब उनसे यह पूछा गया कि झपकी आने के पीछे गलती किसकी थी तो
अधिकतर लोगों ने कहा कि पूरी गलती वक्ता की थी जबकि सिर्फ कुछ ही लोगों ने कहा कि
गलती उनकी थी।
वक्ताओं
को इस अध्ययन से क्या सीखना चाहिए? कैसे वे व्याख्यान
में श्रोताओं की रुचि बनाए रखें? स्लाइड,
पीपीटी या वीडियो दिखाते समय हॉल की मद्धिम रोशनी जैसे
कारकों को तो हटाया नहीं जा सकता। लेकिन हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट इस सम्बंध
में काफी उपयोगी सलाह देती है। इसके अनुसार एक आदर्श वक्तव्य में 37 प्रतिशत टेक्स्ट,
29 प्रतिशत
चित्र और 33
प्रतिशत वीडियो होना चाहिए। व्याख्यान के इस तरह के बंटवारे को अमल में लाना
फायदेमंद हो सकता है और देखा जा सकता है कि यह कैसे काम करता है। व्याख्यान में
पीपीटी के चित्र या टेक्स्ट की ऊंचाई-चौड़ाई का अनुपात सही हो (5 × 3), बड़े अक्षर उपयोग किए
जाएं ताकि आसानी से पढ़े जा सकें, टेक्स्ट और
पृष्ठभूमि के रंग में साफ अंतर हो (काला या नीला पटल होने पर उस पर स्पष्ट दिखते किसी अन्य रंग
से लिखा टेक्स्ट)।
इसके अलावा वक्ता आहिस्ता, स्पष्ट और माइक पर
बोलें। आप कुछ उपयोगी सुझाव इस लिंक पर पढ़ सकते हैं: http://www.med-ed-online.org)
और
अब इन झपकियों के पीछे के मस्तिष्क-विज्ञान को बेहतर समझ लिया गया है। चीनी और जापानी
वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार मस्तिष्क में
न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस नामक हिस्से में यह क्षमता होती है कि वह अणुओं के एक समूह
(A2A रिसेप्टर) को सक्रिय कर झपकी प्रेरित कर सकता है। नेचर
कम्युनिकेशन में प्रकाशित इस शोध पत्र के मुताबिक मुख्य अणु एडिनोसीन है जो A2A रिसेप्टर को सक्रिय कर देता है और नींद आने लगती है।
एडिनोसीन के अलावा अन्य नींद-प्रेरक अणु भी A2A
रिसेप्टर पर कार्य करते हैं। नींद की प्रचलित दवाइयां भी A2A रिसेप्टर को सक्रिय करती हैं और नींद लाती हैं। इसके
विपरीत कॉफी और चाय में मौजूद कैफीन इस रिसेप्टर को अवरुद्ध करते हैं और आपको जगाए
रखते हैं।
तो अगली बार व्याख्यान सुनने जाएं तो एक प्याला कॉफी पीकर जाएं और जागे रहें। और यदि आप व्याख्याता हैं तो उपरोक्त लिंक पर दिए गए सुझावों का लाभ लें। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://th.thgim.com/sci-tech/science/k06dhy/article29542979.ece/alternates/FREE_660/29TH-SCILECTURE