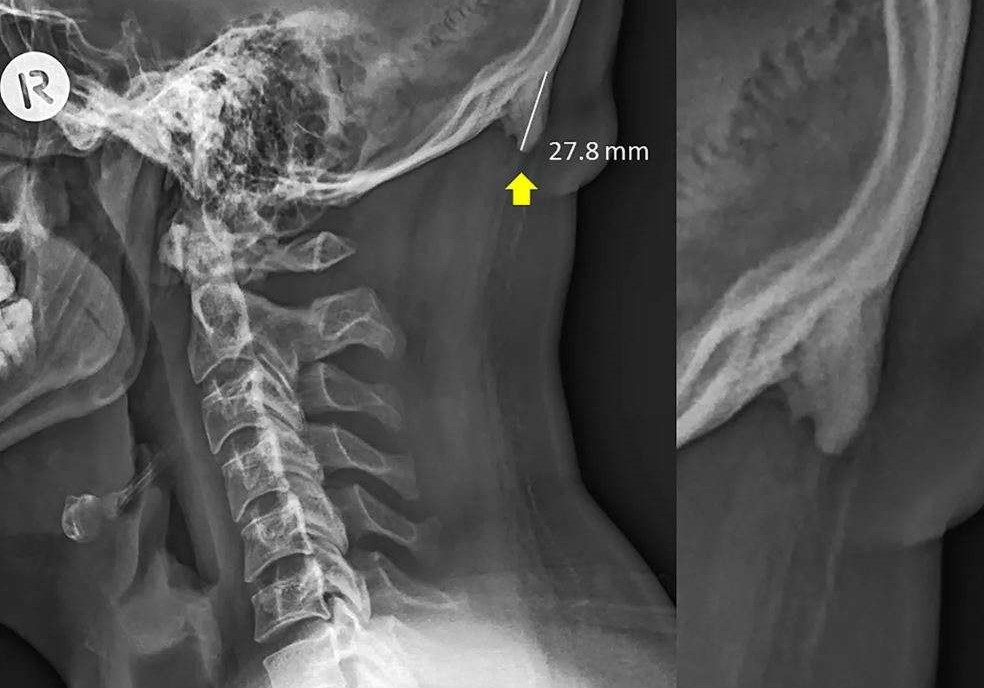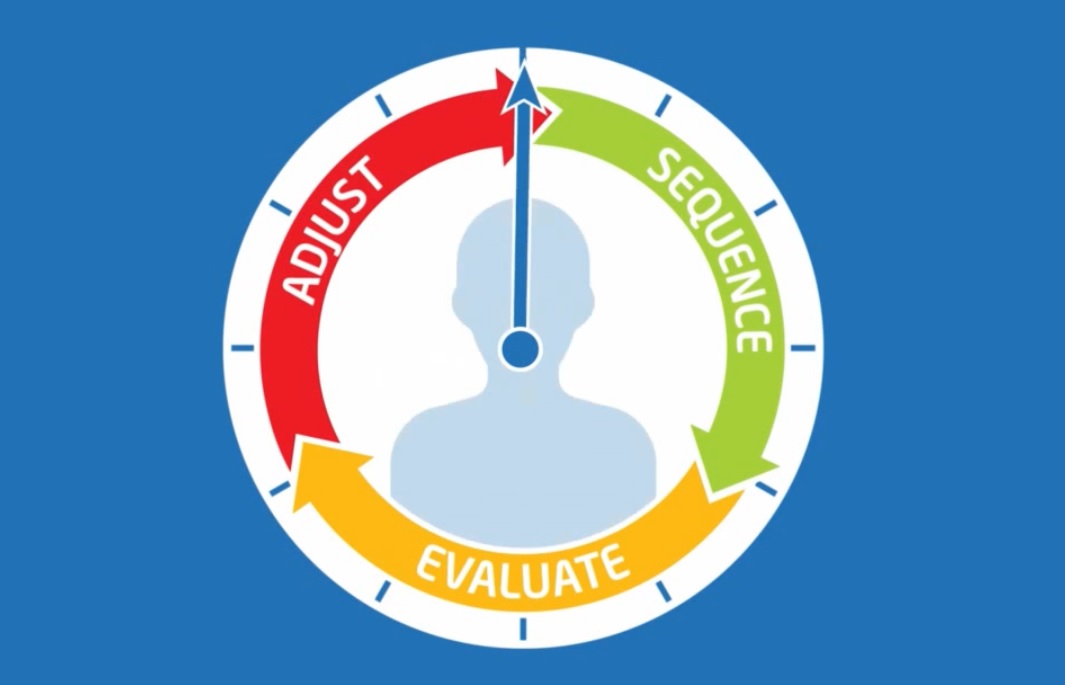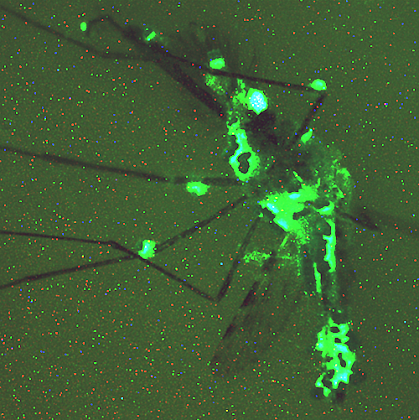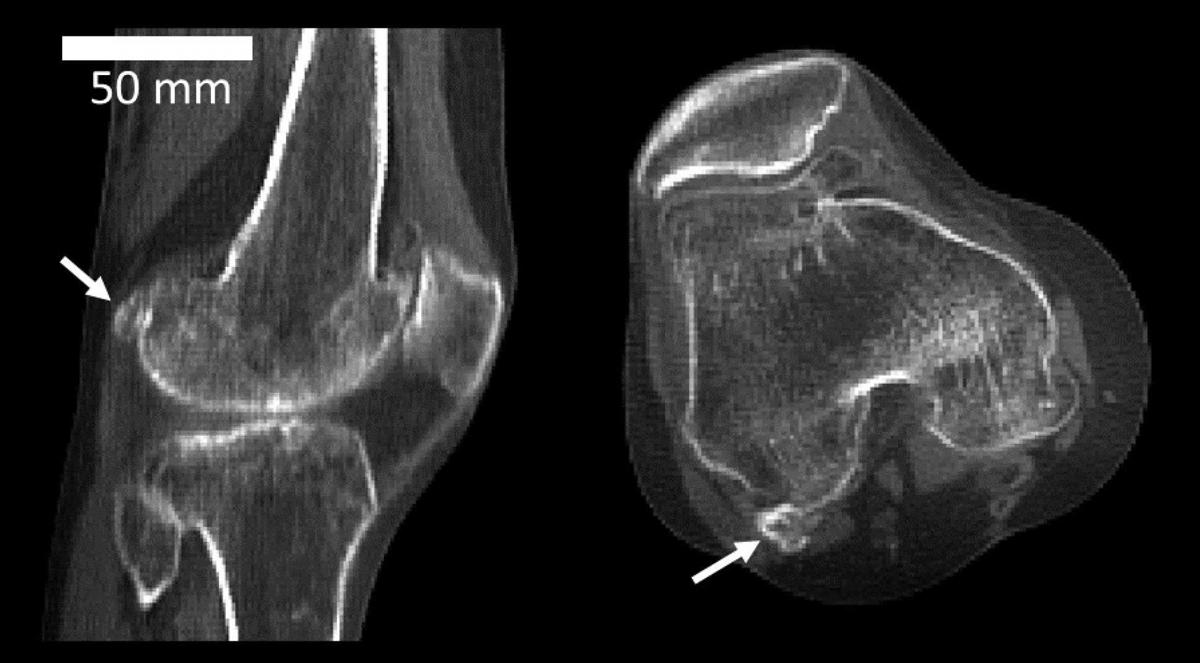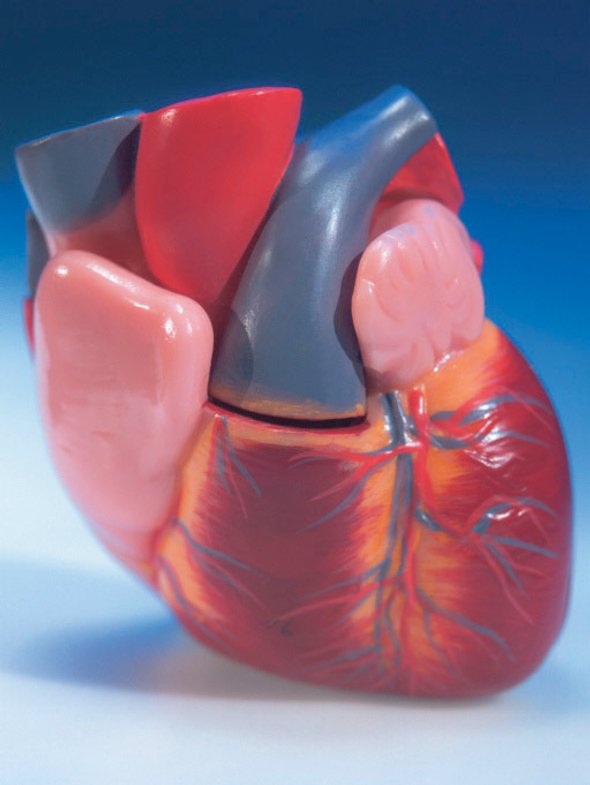आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक परामर्श पत्र की पड़ताल जिसमें आयुर्वेद पर किसी भी अध्ययन में आयुष विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2019 को जारी एक परामर्श पत्र (एडवायज़री) में “गैर-आयुष वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं द्वारा आयुष औषधियों और उपचारों को लेकर बेबुनियाद वक्तव्यों तथा निष्कर्षों वाले शोध पत्रों के प्रकाशन तथा वैज्ञानिक अध्ययनों, जो पूरी प्रणाली की वि·ासनीयता और शुचिता को नुकसान पहुंचाते हैं,” पर चिंता व्यक्त की गई है क्योंकि “इन शोध पत्रों व अध्ययनों में योग्यता प्राप्त आयुष विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया या उनसे परामर्श नहीं किया गया।”
परामर्श पत्र में आगे कहा गया है कि “सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में आयुष की संभावना और विस्तार को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। साथ ही आयुष से सम्बंधित वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान में मनमाने बयानों तथा बेबुनियाद निष्कर्षों से जनता को आयुष का उपयोग करने से विमुख नहीं किया जा सकता है।” इसलिए परामर्श पत्र में कहा गया है कि “सभी गैर-आयुष शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, संस्थानों और चिकित्सा/वैज्ञानिक पत्रिकाओं के संपादकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आयुष औषधि या उपचार का आकलन करने हेतु किए गए वैज्ञानिक अध्ययन/नैदानिक परीक्षण/अनुसंधान हस्तक्षेप के संचालन के लिए या ऐसे परीक्षणों के परिणामों के पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त आयुष विशेषज्ञ/संस्थान/अनुसंधान परिषद को शामिल करें ताकि आयुष के बारे में गलत, मनमाने और अस्पष्ट बयानों एवं निष्कर्षों से बचा जा सके।”
हालांकि हम आयुष मंत्रालय की इस चिंता से पूरी तरह सहमत हैं कि कुछ शोध प्रकाशनों में प्रस्तुत निराधार, एकतरफा और दोटूक निष्कर्षों के कारण पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की छवि को क्षति पहुंचना संभव है, लेकिन हमारा मानना है कि इन्हें रोकने के लिए इस परामर्श पत्र में अनुशंसित व्यवस्था उपयुक्त नहीं है।
परामर्श पत्र में आग्रह किया गया है कि इसकी अनुशंसाओं पर “सम्बंधित शोधकर्ता/वैज्ञानिक/जांचकर्ता” ध्यान दें और इनका पालन करें, लेकिन देखा जाए, तो इनका अनुपालन और क्रियांवयन लगभग असंभव है। अलबत्ता, इस परामर्श अधिक गंभीर और चिंताजनक अर्थ यह है कि इस तरह के कदमों से न केवल इन पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में आवश्यक निष्पक्ष शोध पर अंकुश लगेगा, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता पर भी काफी असर पड़ेगा। निष्पक्ष शोध और सोचने की स्वतंत्रता, ये दोनों ही किसी भी क्षेत्र में हमारी समझ में सुधार के लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं।
हमारा मानना है कि आयुर्वेद सहित विभिन्न पारंपरिक भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिष्ठा में कमी का वास्तविक कारण निम्न-गुणवत्ता वाली शोध पत्रिकाओं का तेज़ी से उभरना है। ये पत्रिकाएं खुद आयुष ‘विशेषज्ञों’ द्वारा किए गए घटिया गुणवत्ता के शोध को प्रकाशित करती रहती हैं। यह निम्न गुणवत्ता का शोध कुकुरमुत्तों की तरह तेज़ी से पनपते कॉलेजों और वि·ाविद्यालयों में किए जा रहे स्नातकोत्तर/पीएचडी शोध ग्रंथों में अप्रामाणिक डेटा को शामिल करने का परिणाम है। यह बात भी किसी छुपी नहीं है कि इनमें से कई आयुष कॉलेज ‘छद्म’ रोगियों, शिक्षकों और यहां तक कि फजऱ्ी छात्रों के माध्यम से अपनी मान्यता बनाए रखे हैं। ज़ाहिर है, ऐसे संस्थानों में किया गया छद्म शोध न केवल आयुष को बदनाम करता है, बल्कि एक ऐसा कार्य-बल तैयार करता है जो इन प्रणालियों को नुकसान पहुंचा सकता है।
अप्रामाणिक व संदिग्ध फार्मेसियों द्वारा खराब गुणवत्ता वाली औषधियों का विपणन भी आयुष को बदनाम कर रहा है। पारंपरिक विचारों से पूरी तरह सहमत न होने वाले अध्ययनों पर प्रतिबंध और ऐसे शोध और आवाज़ों को दबाने की बजाय मंत्रालय की वास्तविक चिंता इन मुद्दों पर होनी चाहिए।
यह भी संभव है कि ऐसे गैर-आयुष शोधकर्ता मौजूद हैं जो घटिया अनुसंधान करके प्रकाशित करते हैं। हालांकि, जैसे अच्छे और गुणवत्ता के प्रति सजग आयुष शोधकर्ता होते हैं, वैसे ही गैर-आयुष शोधकर्ता भी हैं जिन्होंने इन उपचारों की क्रियाविधियों और सिद्धांतों को समझने में सकारात्मक और महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, कार्बनिक रसायन विज्ञानी आसीमा चटर्जी, टी. टी. गोविंदाचारी और अन्य द्वारा आयुर्वेद में प्रयुक्त हर्बल उत्पादों के रसायन शास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी और व्यापक योगदान जाना-माना है। इसी तरह, कई प्रकार के हर्बल और आयुर्वेदिक औषधि मिश्रणों की क्रियाविधियों पर किए गए बुनियादी वैज्ञानिक अध्ययनों ने उनकी जैविक क्रियाविधियों को उजागर करके नए एवं प्रभावी चिकित्सीय अनुप्रयोग के रास्ते खोले हैं। ऐसे कई अध्ययनों ने हर्बल और आधुनिक दवाइयों के बीच सकारात्मक और नकारात्मक अंतर्क्रियाओं को समझने में मदद दी है। कुछ जीनोमिक और आणविक जीव विज्ञानियों ने आयुर्वेद की त्रिदोष/प्रकृति जैसी अवधारणाओं को वर्तमान जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये गैर-आयुष शोधकर्ताओं के योगदान के कुछ चंद उदाहरण भर हैं, जो वास्तव में आयुष को समृद्ध बना रहे हैं।
यह कहना ठीक नहीं होगा कि समकालीन संदर्भों में बगैर प्रमाणित किए, प्राचीन ज्ञान और तौर-तरीकों को सिर्फ इसलिए बगैर सोचे-समझे स्वीकार कर लिया जाए कि वे पारंपरिक हैं। आयुष प्रथाओं और नुस्खों को प्रमाणों की बुनियाद मिलना आवश्यक है। शोध चाहे आयुष शोधकर्ताओं द्वारा किया जाए या गैर-आयुष शोधकर्ताओं द्वारा, यदि वह परंपरागत रूप से मान्य वि·ाासों पर सवाल उठाता है और ऐसे व्यवस्थित प्रमाण उपलब्ध कराता है जो उनकी तार्किकता को चुनौती दें, तो इसे प्राचीन ज्ञान का ‘अपमान’ न समझकर गंभीरता से लेना चाहिए। बुद्धि और सामाजिक व्यवस्था केवल उस ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ती है जो हमारे पूर्वजों के ज्ञान और समझ से भी आगे ले जाए।
यदि इस परामर्श पत्र को गंभीरता से लिया गया, तो यह केवल एक ही विचार को पनपने देगा और उन सभी लोगों को अपने विचार रखने से रोकेगा जो इससे असहमत हैं। एक अच्छा विज्ञान बाहरी सत्यापन के लिए सदैव खुला रहना चाहिए। वास्तव में, सारे दरवाज़े बंद करने की व्यवस्था, जिसमें सिर्फ सहमत लोग हों, अपनाने की बजाय, निष्पक्ष बहु-विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बंद दरवाज़ा व्यवस्था आयुष के लिए खतरनाक साबित होगी। कल्पना कीजिए, अगर जीव विज्ञान के शोधकर्ताओं ने बीसवीं सदी में श्रोडिंजर, डेलब्राुक, पौलिंग, क्रिक, रोसलिंड फ्रेंंकलिन, बेन्ज़र जैसे गैर-जीव वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान में कार्य न करने देने का फैसला किया होता, तो आज जीव विज्ञान या आधुनिक विज्ञान कहां होता?
आयुष को अन्य शोधकर्ताओं से केवल समर्थक साक्ष्य की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि हम अलग-अलग राय रखते हैं, तो बहस को आगे बढ़ाने और तर्क-वितर्क के लिए अकादमिक मंच और पत्रिकाएं मौजूद हैं। यह समझना चाहिए कि आयुष और गैर-आयुष शोधकर्ताओं के जो शोध-परिणाम आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को समर्पित अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, वे अच्छी सहकर्मी-समीक्षा प्रणाली से गुज़रे होंगे और इस प्रकार वे वास्तव में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली के विकास में योगदान दे रहे हैं। संपादकों से यह कहना कि शोध पत्र में एक लेखक के रूप में आयुष विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से शामिल करें, न केवल शोधकर्ताओं की स्वायत्तता के खिलाफ है, बल्कि ऐसे ‘विज्ञान प्रकाशन’ की प्रतिष्ठा के लिए काफी अपमानजनक भी है जहां प्रकाशन से पूर्व लेखक की औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की बजाय सिर्फ यह देखा जाता है कि शोध पत्र में व्यक्त विज्ञान अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं। उक्त परामर्श पत्र संभावित रूप से आयुष और गैर-आयुष विशेषज्ञों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकता है। क्लीनिकल ट्रायल सम्बंधी अनुसंधान में आयुष विशेषज्ञों को शामिल करना वांछनीय होगा, लेकिन प्रयोगशाला में और/या जंतु अध्ययनों में आयुष प्रभाविता की जांच करने वाले सभी अध्ययनों में यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता। जैसे भी हो, आयुष विशेषज्ञ मॉनिटर या वॉचडॉग नहीं बल्कि सहयोगी होंगे।
आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद चिकित्सकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दशक से थोड़ा अधिक समय पहले शुरू किए गए ‘आयुर्वेदिक जीव विज्ञान’ मिशन के अंतर्गत विभिन्न शोधकर्ताओं ने आयुर्वेद में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आयुर्वेदिक जीव विज्ञान के उत्प्रेरक, मूलत: एक ह्मदय शल्य चिकित्सक और नवाचारकर्ता एम.एस. वालियाथन की टिप्पणी है, “इस समय कोई ऐसा सामान्य धरातल नहीं है जहां भौतिक विज्ञानी, रसायनज्ञ, प्रतिरक्षा विज्ञानी और आणविक जीव विज्ञानी आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ बातचीत कर सकें। भारत में आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान की ही नहीं, सारे जीव विज्ञानों की जननी है। इसके बावजूद, विज्ञान आयुर्वेद से पूरी तरह अलग हो चुका है।” ज़ाहिर है, पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों का एकीकरण हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष भागीदारी तथा सचमुच के अंतर-विषयी अध्ययनों की आवश्यकता है। ऐसा एकीकरण ही मानव समाज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकेगा।
हमारा मानना है कि आयुष मंत्रालय के लिए सही दृष्टिकोण यह होगा कि वह पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में खराब गुणवत्ता वाली शोध पत्रिकाओं पर रोक लगाए बनिस्बत इसके कि विभिन्न विषयों के उन शोधकर्ताओं पर रोक लगाए जो वास्तव में आयुर्वेदिक सिद्धांतों और कामकाज का सत्यापन आधुनिक वैज्ञानिक गहनता के तहत कर सकते हैं जो आय़ुर्वेद के लिए ज़रूरी है। आयुष की प्रामाणिकता को बढ़ावा देने के लिए, एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी जो मज़बूत वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हो। आयुष मंत्रालय विभिन्न आयुष महाविद्यालयों और उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों में शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानक स्थापित करके इसको बढ़ावा दे सकता है। आगे की सोच और आगे बढ़ना आयुष के लिए लाभदायक होगा। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://mk0similima57rg8gkp8.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2015/12/ayush.jpg