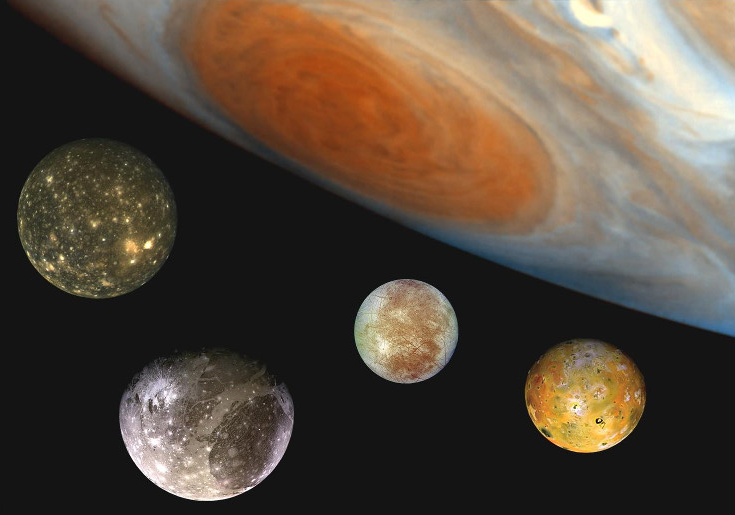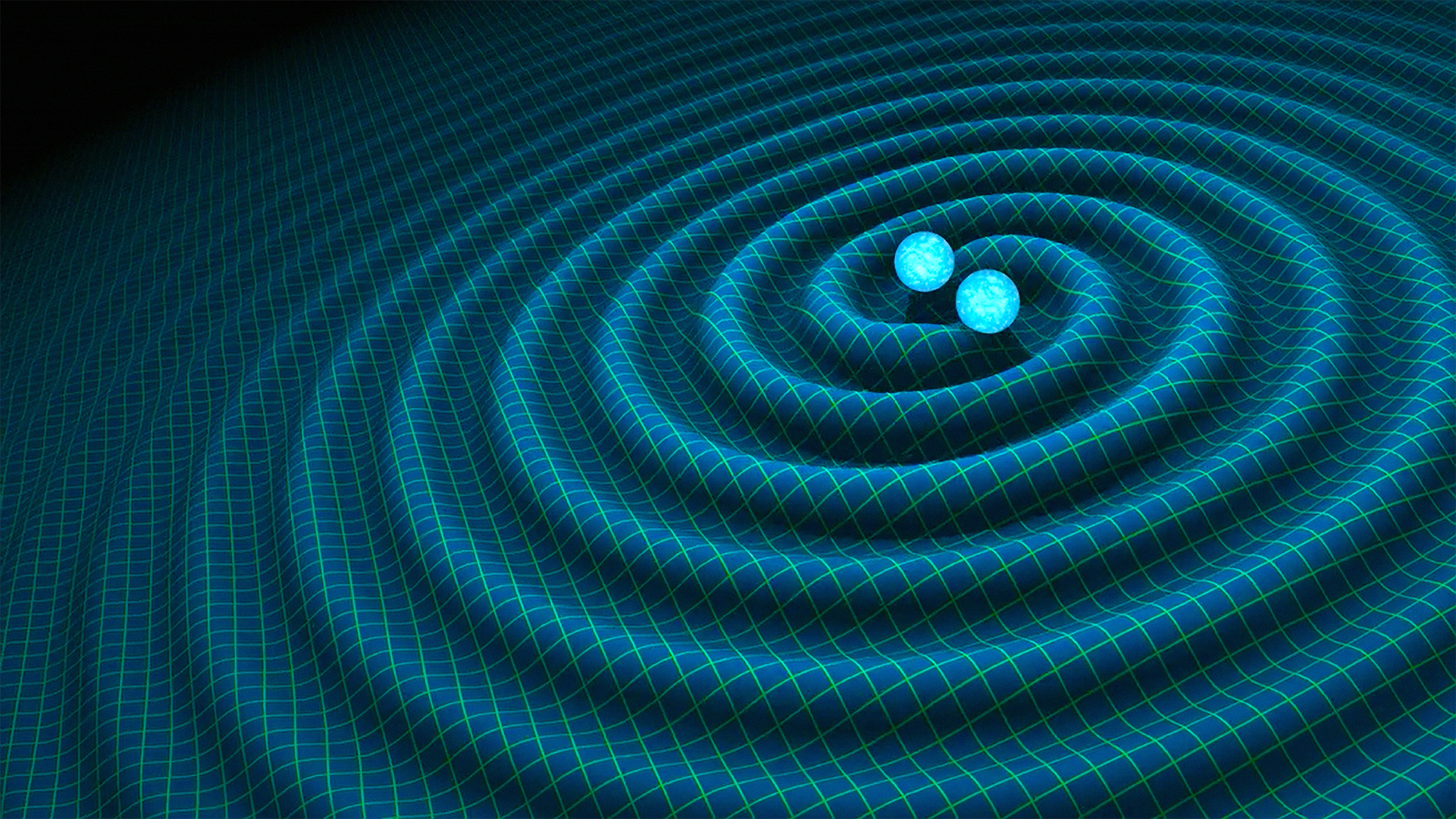अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान संघ ने हाल ही में घोषणा की है कि पृथ्वी के वर्तमान दौर को एक विशिष्ट काल के रूप में जाना जाएगा। यह होलोसीन युग का एक हिस्सा है जिसे नाम दिया गया है मेघालयन। भूगर्भ संघ के मुताबिक हम पिछले 4200 वर्षों से जिस काल में जी रहे हैं वही मेघायलन है।
भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के लगभग 4.6 अरब वर्ष के अस्तित्व को कई कल्पों, युगों, कालों, अवधियों वगैरह में बांटा है। इनमें होलोसीन एक युग है जो लगभग 11,700 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब भूगर्भ वैज्ञानिक मान रहे हैं कि पिछले 4,200 वर्षों को एक विशिष्ट नाम से पुकारा जाना चाहिए – भारत के मेघालय प्रांत से बना नाम मेघालयन।
दरअसल, भूगर्भीय समय विभाजन भूगर्भ में तलछटों की परतों, तलछट के प्रकार, उनमें पाए गए जीवाश्म तथा तत्वों के समस्थानिकों की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। समस्थानिकों की विशेषता है कि वे समय का अच्छा रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। इनके अलावा उस अवधि में घटित भौतिक व रासायनिक घटनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान संघ ने बताया है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में आखरी हिम युग के बाद कृषि आधारित समाजों का विकास हुआ था। इसके बाद लगभग 200 वर्षों की एक जलवायु–सम्बंधी घटना ने इन खेतिहर समाजों को तहस–नहस कर दिया था। इन 200 वर्षों के दौरान मिस्र, यूनान, सीरिया, फिलीस्तीन, मेसोपोटेमिया, सिंधु घाटी और यांगत्से नदी घाटी में लोगों का आव्रजन हुआ और फिर से सभ्यताएं विकसित हुर्इं। यह घटना एक विनाशकारी सूखा था और संभवत: समुद्रों तथा वायुमंडलीय धाराओं में बदलाव की वजह से हुई थी।
इस अवधि के भौतिक, भूगर्भीय प्रमाण सातों महाद्वीपों पर पाए गए हैं। इनमें मेघायल में स्थित मॉमलुह गुफा (चेरापूंजी) भी शामिल है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के कई स्थानों से तलछट एकत्रित करके विश्लेषण किया। मॉमलुह गुफा 1290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत की 10 सबसे लंबी व गहरी गुफाओं में से है (गुफा की लंबाई करीब 4500 मीटर है)। इस गुफा से प्राप्त तलछटों में स्टेलेग्माइट चट्टानें मिली हैं। स्टेलेग्माइट किसी गुफा के फर्श पर बनी एक शंक्वाकार चट्टान होती है जो टपकते पानी में उपस्थित कैल्शियम लवणों के अवक्षेपण के कारण बनती है। संघ के वैज्ञानिकों का मत है कि इस गुफा में जो परिस्थितियां हैं, वे दो युगों के बीच संक्रमण के रासायनिक चिंहों को संरक्षित रखने के हिसाब से अनुकूल हैं।
गहन अध्ययन के बाद विशेषज्ञों के एक आयोग ने यह प्रस्ताव दिया कि होलोसीन युग को तीन अवधियों में बांटा जाना चाहिए। पहली, ग्रीलैण्डियन अवधि जो 11,700 वर्ष पहले आरंभ हुई थी। दूसरी, नॉर्थग्रिपियन अवधि जो 8,300 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और अंतिम मेघालयन अवधि जो पिछले 4,200 वर्षों से जारी है। अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान संघ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
मेघालयन अवधि इस मायने में अनोखी है कि यहां भूगर्भीय काल और एक सांस्कृतिक संक्रमण के बीच सीधा सम्बंध नज़र आता है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : BBC