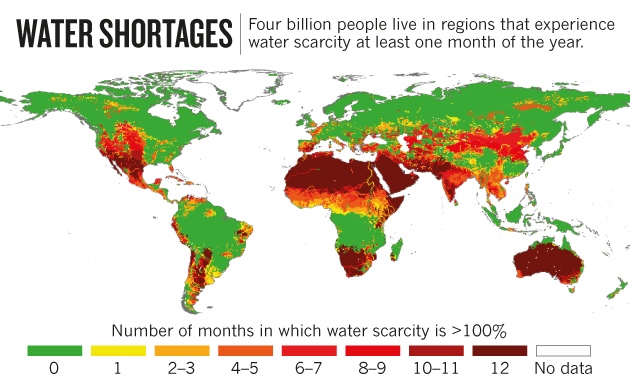अतीत में हुर्इं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं ने बड़ी संख्या में प्रजातियों को खत्म कर दिया था, लेकिन उस वक्त कई प्रजातियों को इतना वक्त मिला था कि वे इस परिवर्तन के साथ तालमेल बना सकीं और बेहतर समय आने तक अपने वंश को जीवित रख सकीं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की हालिया रफ्तार को देखते हुए एक सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान जलवायु परिवर्तन प्रकृति को इतनी गुंजाइश देगा।
इस संदर्भ में विक्टोरिया रैडचक और जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड, यू.के., चेक गणतंत्र, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा, स्पेन, यू.एस., जापान, फिनलैंड, नॉर्वे, स्विटज़रलैंड और पोलैंड के 60 अन्य वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित पेपर में इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है। यह पेपर 58 पत्रिकाओं में प्रकाशित 10,090 अध्ययनों के सार और 71 अध्ययनों के डैटा पर आधारित है। इसमें उन्होंने इस बात का आकलन किया है कि जीवों में हो रहे शारीरिक बदलाव क्या जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन बनाने की दृष्टि से हो रहे हैं। अध्ययन के अनुसार कई प्रजातियों में तो अनुकूलन हो रहा है लेकिन अधिकांश प्रजातियां इस दौड़ में हारती नज़र आ रही हैं।
अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और प्रजातियों की विलुप्ति के चलते पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के परस्पर समर्थक संतुलन में कमी आती है। जीव अपनी आबादी को तब ही बनाए रख सकते हैं जब उनमें जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह के शारीरिक या व्यावहारिक बदलाव हों, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करते हों या उसके अनुकूल हों। ऐसा या तो शारीरिक अनुकूलन के द्वारा हो सकता है (जैसे आहार में परिवर्तन के साथ-साथ पाचक रसों में परिवर्तन) या विकास के छोटे-छोटे कदमों से हो सकता है, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में प्रवास करने से संभव हो सकता है। लेकिन शारीरिक अनुकूलन में भी वक्त लगता है। जैसे पर्वतारोही अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ने के पहले बीच में रुककर खुद को पर्यावरण के अनुरूप ढालते हैं, तब आगे चढ़ाई करते हैं। किसी प्रजाति में वैकासिक परिवर्तन पर्यावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलित किस्मों के चयन द्वारा होता है, और ऐसा होने में तो कई पीढ़ियां लग जाती हैं। पेपर के अनुसार, प्रजातियों की संख्या का पूर्वानुमान लगाने और योजनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए यह पता करना महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दशकों में प्रजातियों में आए बदलावों में से कितने ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के जवाब में हुए हैं।
अनुकूलन का एक उदहारण है – प्रजनन करने या अंडे देने का समय इस तरह बदलना कि उस समय संतान को खिलाने के लिए भोजन के स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। लेखकों ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया है कि यूके में पिछले 47 वर्षों में पक्षियों की एक प्रजाति के अंडे देने का समय औसतन 14 दिन पहले खिसक गया है। अध्ययन के अनुसार यह एक ऐसा मामला है जहां “पर्यावरण के हिसाब से एक-एक जीव के व्यवहार में बदलाव ने पूरी प्रजाति को तेज़ी से बदलते परिवेश के साथ बारीकी से समायोजन करने में सक्षम बनाया है।”
एक अन्य अध्ययन में, प्रतिकूल-अनुकूलन का एक मामला सामने आया है। एक पक्षी प्रजाति है जो आर्कटिक ग्रीष्मकाल के दौरान प्रजनन करती है। जब ये पक्षी जाड़ों में उष्णकटिबंधीय इलाके की ओर पलायन करते हैं तब वे काफी अनफिट साबित होते हैं। गर्मियों में जन्मे चूज़ों में अनुकूलन यह होता है कि वे छोटे आकार के होते हैं ताकि शरीर से अधिक ऊष्मा बिखेरकर गर्मियों का सामना अधिक कुशलता से कर सकें। लेकिन छोटे पक्षियों की चोंच भी छोटी होती है जिससे उनको सर्दियों में प्रवास के दौरान काफी नुकसान होता है क्योंकि इन इलाकों में भोजन थोड़ा गहराई में दबा होता है और छोटी चोंच के कारण वे पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते।
रेनडियर जैसे शाकाहारी ऐसे मौसम में संतान पैदा करने के लिए विकसित हुए थे जब पौधे उगने का सबसे अच्छा मौसम होता है। प्रजनन काल तो दिन की लंबाई से जुड़ा होने के कारण यथावत रहा जबकि पौधों की वृद्धि का मौसम स्थानीय तापमान से जुड़ा था। जलवायु परिवर्तन के साथ यह समय बदल गया (जबकि दिन-रात की अवधि नहीं बदली)। एक अध्ययन के अनुसार इन प्राणियों में मृत्यु दर तो बढ़ी ही है, साथ-साथ जन्म दर में चार गुना कमी आई है।
वैसे तो समय के साथ सभी प्रजातियों के रूप और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, लेकिन इस अध्ययन का उद्देश्य उन परिवर्तनों की पहचान करना था जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के उदाहरण हों। इस पेपर के अनुसार ऐसा तभी माना जा सकता है जब तीन चीज़ें हुई हों। पहली यह कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो। दूसरी यह कि जीवों की शारीरिक विशेषताओं में बदलाव सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ हो, किसी अन्य कारण से नहीं। और तीसरी यह कि परिवर्तन उन लक्षणों के चयन के कारण हुआ हो जो जीवों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं।
लेखकों के अनुसार तीसरी स्थिति के परीक्षण के लिए ऐसे डैटा की आवश्यकता होगी जो किसी एक प्रजाति की निश्चित आबादी की कई पीढ़ियों के लिए एकत्रित किए गए हों। शोधकर्ताओं की इस विशाल टीम ने उन अध्ययनों को खोजा है जो इस बात की पड़ताल करते हैं कि तापमान और वर्षा या दोनों विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट या जीवन की घटनाओं को किस तरह प्रभावित करते हैं। विशाल उपलब्ध डैटा में से उन्हें पक्षियों के सम्बंध में उपयोगी जानकारी मिली। और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पक्षियों के बारे में लंबी अवधियों की जानकारी प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है – घोंसला बनाने का समय, अंडे देने और उनके फूटने का समय, और गतिशीलता।
पेपर के अनुसार, जलवायु परिवर्तन पर जीवों की प्रतिक्रिया सम्बंधी कई पूर्व में किए गए अध्ययन प्रजातियों के फैलाव और उनकी संख्या में आए बदलाव पर केंद्रित थे। जलवायु परिवर्तन के चलते जीवों के व्यवहार, आकार या शरीर विज्ञान में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन बहुत कम किया गया है। और प्रजातियों के फैलाव तथा आबादी की गणना करने वाले मॉडल्स में इस संभावना को ध्यान में नहीं रखा गया था कि प्रजाति में अनुकूलन भी हो सकता है। लिहाज़ा, लेखकों के अनुसार उनके वर्तमान “अध्ययन ने बदलते पर्यावरण में प्रजातियों की प्रतिक्रियाओं के समयगत पहलू पर ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है।” उनके अनुसार “हमने दर्शाया है कि कुछ पक्षियों ने गर्म जलवायु के मुताबिक अपने जीवनचक्र की घटनाओं के समय को बदल लिया है। अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि प्रजातियां अपनी ऊष्मा सम्बंधी ज़रूरतों का समाधान उसी स्थान पर खोज सकती हैं और इसके लिए भौगोलिक सीमाओं में बदलाव ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता, हमें सभी प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के प्रमाण नहीं मिले हैं, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अनुकूल परिवर्तन करने वाले जीव भविष्य में बने ही रहेंगे।”
लेखक आगे बताते हैं कि जिन प्रजातियों का अध्ययन किया गया है वे सुलभ और काफी संख्या में उपलब्ध हैं और इनके बारे में डैटा आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि “हमें डर है कि दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादियों की निरंतरता का पूर्वानुमान अधिक निराशाजनक होगा।”
निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस सदी के अंत तक बहुत-सी प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना है जो काफी चिंताजनक है। ऐसे कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि जैव तकनीक ही वह नैया है जो हमें 21 सदी पार करा देगी।
सच है, उपरोक्त अध्ययन वनस्पति प्रजातियों पर नहीं हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से पेड़-पौधे भी प्रभावित होते हैं। और जंतु वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। इस अध्ययन के परिणाम शायद बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों के मामले में भी सच्चाई से बहुत दूर न हों। इसलिए जैव विविधता में भारी गिरावट वनस्पति जगत में भी दिखाई देगी और आने वाले दशकों में यह पौधों की भूमिका के लिए ठीक नहीं होगा जिसको लेकर हम इतने आश्वस्त हैं। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://cosmos-magazine.imgix.net/file/spina/photo/19794/190723-parus_full.jpg?fit=clip&w=835