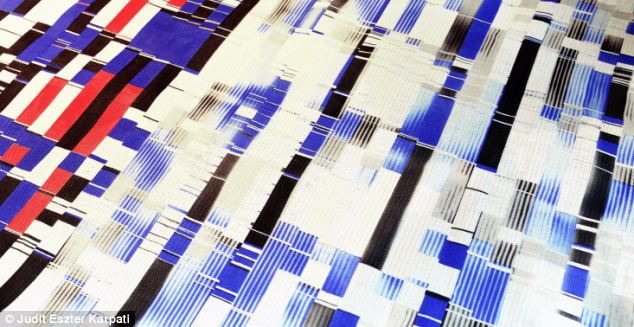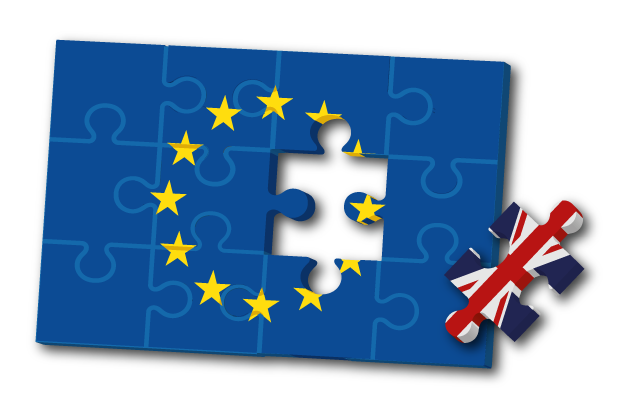वैसे तो अभी जाड़े का मौसम आने वाला है लेकिन गर्मियां भी दूर नहीं हैं। और भारत की चिलचिलाती गर्मी नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। बढ़ती गर्मी न सिर्फ असुविधा पैदा कर रही है बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। निरंतर बढ़ते तापमान और अत्यधिक आर्द्रता के परिणामस्वरूप हीट स्ट्रोक (लू लगने) से मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
पिछले वर्ष दी लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2000-04 और 2017-21 के बीच गर्मी से मरने वाले लोगों की संख्या में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका सबसे अधिक प्रभाव शहरी क्षेत्रों पर हो रहा है जहां टार और कांक्रीट जैसी गर्मी सोखने वाली निर्माण सामग्री का भरपूर उपयोग हो रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों के चलते यह जोखिम बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि 2025 तक भारत की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास करेगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव शहरी गरीबों पर होगा जो न एयर कंडीशनिंग का खर्च उठा सकते हैं और बाहर खुले में काम करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए शोधकर्ता और नीति निर्माता अब इस बढ़ते संकट को समझने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियां विकसित कर रहे हैं।
ऐतिहासिक रूप से भारत में आपदा नियोजन प्रयास चक्रवातों और बाढ़ से निपटने पर केंद्रित रहे हैं। लेकिन वर्ष 2015 से राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीष्म लहरों को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। कुछ शहरों में शोधकर्ता आपातकालीन योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ ग्रीष्म-लहर की चेतावनी जारी करने और शीतलता केंद्र खोलने पर विचार कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ता तो घरों को ठंडा बनाने के लिए सस्ते तरीके भी आज़मा रहे हैं। कुछ अन्य शोधकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के तापमान पर भूमि उपयोग और वास्तुकला का प्रभाव समझकर शहरों के विस्तार के लिए समुचित डैटा जुटा सकें।
इसी तरह का एक प्रयास नागपुर में अर्बन हीट रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत शोधकर्ताओं द्वारा किया गया; 30 लाख की आबादी वाला यह शहर भारत के सबसे गर्म शहरों में से एक है।
तापमान के दैनिक पैटर्न से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कई अध्ययन दर्शाते हैं कि गर्म दिनों के साथ रातें भी गर्म रहें तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं क्योंकि ऐसा होने पर शरीर को गर्मी से कभी राहत नहीं मिलती है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि भारत में लगातार गर्म दिन और गर्म रातें आम बात होती जा रही हैं।
इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक कारकों और गर्मी के प्रति संवेदनशीलता के सम्बंध को भी समझने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए गरीब लोग घर को ठंडा रखने के उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते। यह भी संभव है कि बुज़ुर्गों को ऐसी बीमारियां होती हों जो उन्हें गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति या स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है जो गर्मी से सम्बंधित बीमारी से निपटने में मदद कर सकते हैं। जैसे नागपुर के बाहरी इलाकों में लोगों के पास स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम है।
टीम ने गर्मी के बारे में लोगों की समझ को भी महत्वपूर्ण माना है। पिछले साल ग्रीष्म लहर के दौरान शोधकर्ताओं ने पैदल लोगों से बातचीत की। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी अधिकांश लोगों ने कम ही चिंता व्यक्त की क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ नया नहीं है, मौसम तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। यह काफी चिंताजनक है क्योंकि आम जनता को गर्मी से होने वाले जोखिमों के बारे में पर्याप्त समझ नहीं है। संभव है कि वे ग्रीष्म लहर से सम्बंधित चेतावनियों पर भी ध्यान नहीं देंगे। इस स्थिति में हीट एक्शन प्लान (एचएपी) तैयार करना और भी ज़रूरी हो जाता है।
मुख्य तौर पर एचएपी का उद्देश्य अधिकारियों को ग्रीष्म-लहर की चेतावनी जारी करने के लिए तैयार करने और अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों को सचेत करना है। इसके तहत अस्पतालों को गर्मी के मौसम में लू के रोगियों के इलाज के लिए कोल्ड वार्ड बनाने और बिल्डरों को अत्यधिक गर्म दिनों में मज़दूरों को छुट्टी देने का सुझाव दिया गया है।
एचएपी सबसे पहले 2013 में अहमदाबाद में स्थानीय वैज्ञानिक संस्थानों और गैर-मुनाफा संस्था नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल (एनआरडीसी) द्वारा शुरू किया गया था। 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत कम से कम 1190 लोगों की जान बचाई गई। आपदा प्रबंधन एजेंसी अब देश के 28 में से 23 राज्यों में एचएपी विकसित करने के लिए काम कर रही है।
अलबत्ता, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा एचएपी का कार्यान्वयन असमान रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना में पर्याप्त धन की कमी है। इसके अलावा योजना के तहत निर्धारित सीमाएं स्थानीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में तो केवल दिन का उच्चतम तापमान ही अलर्ट के लिए पर्याप्त माना गया है। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में प्रारंभिक अलर्ट के लिए सीमा 41 डिग्री सेल्सियस निर्धारित की गई है। लेकिन कई अन्य स्थानों पर, रात का तापमान या आर्द्रता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि दिन का तापमान लेकिन इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।
जैसे, मुंबई में अप्रैल माह में देर सुबह और बिना किसी छाया के आयोजित एक समारोह में 11 लोगों की लू से हुई मौतों ने अधिक सूक्ष्म और स्थान-आधारित चेतावनियों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उस दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था, जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तटीय शहरों के लिए निर्धारित अलर्ट सीमा से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। लेकिन गर्मी का प्रभाव आर्द्रता के कारण अधिक बढ़ गया था जिसे गर्मी चेतावनी प्रणालियों में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। विडंबना यह है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में इस त्रासदी से सिर्फ 2 महीने पहले एचएपी अपनाया गया था। इसमें गर्म दिनों में बाहरी कार्यक्रमों को अलसुबह करने की सलाह दी गई थी।
एचएपी को बेहतर बनाने में मदद के लिए शोधकर्ता एक मॉडल योजना पर काम कर रहे है जिसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके। साथ ही सभी शहरों की अधिक जोखिम वाली आबादी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जोखिम मानचित्र का भी सुझाव दिया गया है।
ऐसा मानचित्र बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें अधिक बुजुर्ग आबादी वाले या अनौपचारिक आवासों वाले इलाकों को चिंहित किया जा सकता है ताकि उन्हें विशेष चेतावनी मिल सके या पर्याप्त शीतलन केंद्रों की व्यवस्था की जा सके। नागपुर परियोजना के तहत एक जोखिम मानचित्र तैयार किया गया है जो यह बता सकता है कि ग्रीष्म लहर की स्थिति में किन इलाकों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
शोधकर्ताओं का मानना है कि एचएपी में केवल अल्पकालिक आपातकालीन सेवाओं के अलावा मध्यम से दीर्घकालिक उपायों पर भी काम किया जाना चाहिए। जैसे छाया प्रदान करने के लिए पेड़ लगाने के स्थान तय करना। एचएपी के तहत घरों के पुनर्निर्माण या भवन निर्माण नियमों में बदलाव के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। शहरों को ठंडा रखने के लिए उनके निर्माण के तरीके बदलना होंगे। नागपुर की टीम ने शहर की ऐसी इमारतों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। लेकिन ऐसे घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं है और इनके रख-रखाव का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है।
हाल के वर्षों में, आवास मंत्रालय ने जलवायु अनुकूल इमारतों के निर्माण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसमें पारंपरिक वास्तुकला के कुछ सिद्धांत शामिल किए गए हैं। लेकिन ये दिशानिर्देश ज़्यादातर कागज़ों पर ही हैं। बिल्डर और स्थानीय सरकारें अपने तौर-तरीकों को बदलने में धीमी या अनिच्छुक लगते हैं।
वैसे, शहरों में रहने वाले कम आय वाले कई परिवारों के लिए नवनिर्मित, जलवायु-अनुकूल निवास में जाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मौजूदा घरों में ही कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे सस्ता और जांचा-परखा तरीका छतों को सफेद परावर्तक पेंट से ढंकना है। एचएपी के तहत इस तकनीक का सबसे पहला उपयोग 2017 में अहमदाबाद में किया गया था। एक अध्ययन के अनुसार पेंट की हुई टीन की छत वाले घर बिना पेंट वाली छतों की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस ठंडे रहते हैं जबकि अधिक महंगी तकनीक का उपयोग करके घरों को 4.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है।
2020 में, 15,000 कम आय वाले घरों तक कूल रूफ कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। इस साल, जोधपुर ने इसी तरह की पहल की है। इसी तरह तेलंगाना ने 2028 तक 300 वर्ग किलोमीटर ठंडी छतें बनाने का संकल्प लिया है। मुंबई और अन्य शहरों में, सीबैलेंस नामक एक निजी फर्म गरीब परिवारों के लिए कम लागत वाली शीतलन तकनीकों का परीक्षण कर रही है।
इस तकनीक में घर को ठंडा रखने के लिए टीन की छत को एल्यूमीनियम पन्नी से ढंककर गर्मी से इन्सुलेशन दिया जाएगा। इन घरों में एक बड़ा परिवर्तन छत के थोड़ा ऊपर पुनर्चक्रित प्लास्टिक कचरे के पैनलों से निर्मित दूसरी छत बनाना है। रसोई की खिड़की के लिए सुबह के समय पैनलों को बंद करने की व्यवस्था होगी जिससे धूप को रोका जा सकेगा और रात में उन्हें फिर से खोलकर गर्मी को बाहर किया जा सकेगा।
फिलहाल तो एक गैर-सरकारी परोपकारी संस्था ने इन परिवर्तनों के लिए धन प्रदान किया है। लेकिन भारत में शीतलन संसाधनों के भुगतान के लिए पैसा एकत्रित करना एक चुनौती है। विशेष पेंट काफी महंगा है। पैसे बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी छतों को साधारण सफेद पेंट से रंगने की कोशिश की है। लेकिन यह तापमान को उतना कम नहीं करता है।
वैसे कई अन्य समस्याएं भी हैं। जैसे मुंबई की बस्तियों में बेतरतीब बिजली के तारों से कुछ छतों पर शेडिंग पैनल स्थापित नहीं किए जा सकते। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छत पर किए जाने वाले परिवर्तनों से वॉटरप्रूफिंग को नुकसान न पहुंचे। इन चुनौतियों के बावजूद, शोधकर्ता और इंजीनियर भारत के शहरों और उसमें भी सबसे कमज़ोर नागरिकों के लिए कूलिंग समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कूलिंग कोई सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मामला बन गया है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.adl0080/abs/_20230929_nf_climate_india_sunset.jpg