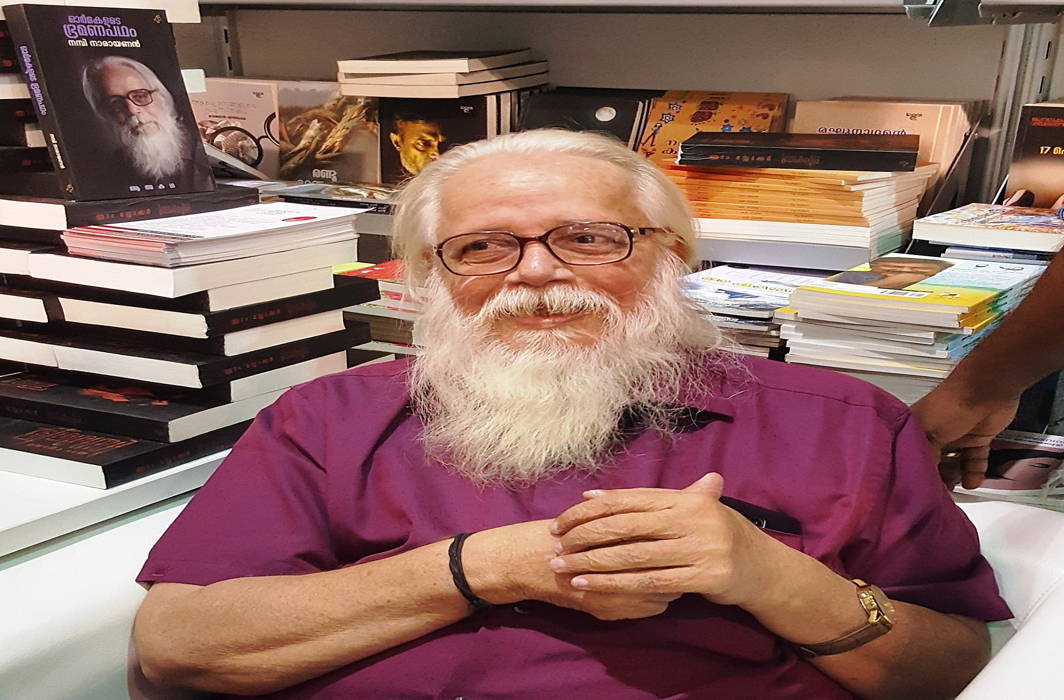बैक्टीरिया की एक नई किस्म किस प्रकार विकसित होती है? मान लीजिए, किसी बैक्टीरिया का सामना किसी खतरे से होता है। यह खतरा एंटीबायोटिक के रूप में हो सकता है। संयोगवश बैक्टीरिया के जीन में एक छोटा–सा परिवर्तन होता है, जो उसे इस खतरे का सामना करने के काबिल बनाता है। दूसरे शब्दों में, उसे प्रतिरोधी बनाता है। चूंकि बैक्टीरिया कुछ मिनटों या घंटों में तेज़ी से बढ़ते हैं इसलिए हम देख सकते हैं कि कुछ ही हफ्तों में बैक्टीरिया की दवा प्रतिरोधी किस्म बढ़ जाएगी और दवा संवेदनशील किस्मों की जगह ले लेगी।
उपरोक्त बात जो बैक्टीरिया के लिए सत्य है वह पौधों और जानवरों पर भी लागू होती है। फर्क केवल इतना है कि पौधों और जंतुओं के मामले में समय मिनटों और घंटों में नहीं बल्कि दशकों, सदियों या सहस्त्राब्दी में देखा जाता है क्योंकि इनमें एक–एक पीढ़ी काफी लंबे समय की होती है। मगर यह सही है कि जब उन पर भी जलवायु या पर्यावरण परिवर्तन, या पालतू बनाए जाने के कारण स्थानीय परिवर्तनों का दबाव पड़ता है तो वे भी उत्परिवर्तन पैदा करते हैं।
क्या ऐसे तनाव एक के बाद एक उत्परिवर्तन क्रमिक रूप से उत्पन्न करते हैं या जीनोम अपेक्षाकृत थोक में (झटके के साथ रुक–रुककर) प्रतिक्रिया देता है? क्रमिकता में विश्वास रखने वाले जीव विज्ञानी इन वैज्ञानिकों को ‘जर्क’ (झटका) कहते हैं। इसके जवाब में झटकेदार उत्परिवर्तन में विश्वास करने वाले वैज्ञानिक क्रमिकता में विश्वास करने वालों को ‘क्रीप’ (सरका) कहते हैं।
मक्का, गेहूं, कपास या चावल जैसे पौधों को देखें। इन्हें जलवायु में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है। इनमें से कई परिवर्तन पुरातन काल में पृथ्वी पर हुए थे। जब मनुष्य ने पालतू बनाने की प्रक्रिया में उन्हें नए वातावरण प्रदान किए तब भी इन्हें परिवर्तनों का सामना करना पड़ा था।
सवाल है कि पौधे इस तरह के तनाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या उनके जीन में क्रमिक परिवर्तनों के ज़रिए सदियों में अनुकूलन होगा, जिसमें एक के बाद एक प्रत्येक उत्परिवर्तन पहले वाले उत्परिवर्तन की मदद करेगा? या एक बड़े पैमाने पर एक झटके में थोक परिवर्तन हो सकते हैं जिनकी वजह से नई किस्में एवं संकर उत्पन्न हो जाएंगे?
जीव विज्ञानी डॉ. बारबरा मैकलिंटॉक मक्का (मकई) में आनुवंशिक परिवर्तन का अध्ययन कर रही थीं। कई वर्षों के की अथक मेहनत के बाद यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि जीनोम के भीतर जीन अनुक्रमों का थोक स्थानांतरण होता रहता है।
उन्होंने पाया कि जीनोम के भीतर डीएनए के टुकड़े कटकर अलग होते हैं, कहीं औेर चिपक जाते हैं, या उनकी प्रतिलिपि बनकर कहीं और जुड़ जाती है। इस प्रकार से जीनोम एक जड़ाऊ काम है, जिसका अनुक्रम बदलता रहता है और अनुक्रम बदलने के साथ संदेश भी बदलता है और नई किस्में पैदा हो सकती हैं।
(उदाहरण के तौर पर, एक वाक्य देखिए: “मारो मत, जाने दो।” अब काट–छांट या शब्दों को कॉपी–पेस्ट करने पर वाक्य का संदेश बदल जाएगा: “मारो, मत जाने दो”)। मैकलिंटॉक ने ऐसे चलते–फिरते डीएनए अनुक्रमों को ट्रांसपोज़ॉन या ट्रांसपोज़ेबल घटक का नाम दिया था। इस खोज के लिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला।
ट्रांसपोज़ॉन्स या फुदकते जीन–अनुक्रम तनाव होने पर या पालतूकरण का दबाव होने पर विकास के लिए एक व्यवस्था प्रदान करते हैं। हाल ही में इस बिंदु को वारविक विश्वविद्यालय, यूके में कपास के पौधे का अध्ययन करने वाले एक समूह द्वारा रेखांकित किया गया है।
उन्होंने कपास के पुरातात्विक नमूने लिए (पेरू से दो, एक–एक ब्राज़ील और मिरुा से)। इनके डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण करने पर देखा कि पालतू बनाई गई किस्मों में काफी जीनोमिक पुनर्गठन हुआ है, जबकि इन्हीं से सम्बंधित जंगली किस्मों में जीनोम अनुक्रम काफी स्थिर बना रहा है।
पालतूकरण और इससे उत्पन्न तनाव पौधों को मजबूर करते हैं कि वे ट्रांसपोज़ॉन्स का उपयोग करके जीन्स का स्थानांतरण करें।
मनुष्यों की सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण इस तरह के एपिसोडिक (घटना–आधारित) परिवर्तनों का अनुभव अकेले कपास ने नहीं किया है। बल्कि साथ–साथ, कपास के कारण मानव व्यवहार और सभ्यता में भी एपिसोडिक परिवर्तन आए हैं।
यह प्राचीन पौधा पहली बार सिंधु घाटी में 6000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया था। वहां से यह अफ्रीका और अरेबिया तक फैल गया, जहां इसे अल कुत्न नाम दिया गया (स्पैनिश में यह अलगोडन हुआ और अंग्रेज़ी में कॉटन)।
स्वतंत्र रूप से, मेक्सिको में 3000 ईसा पूर्व में, इसकी एक और प्रजाति उगाई गई थी। शुरुआती एशियाई और मेक्सिकन लोग इसे कातते और पहनते थे। मसाले, सोना और चांदी के साथ, कपास भी प्राचीन विश्व का खज़ाना था जिसे उपनिवेशवादी लूटा करते थे।
कपास की इस लूटपाट और व्यावसायीकरण ने गुलामी के अपमानजनक और अक्षम्य इतिहास को बढ़ावा दिया। जब युरोपीय लोगों ने अमेरिका की खोज की, और उसके अधिकांश दक्षिणी राज्यों को कपास के खेतों में परिवर्तित कर दिया तो उन्हें मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी।
सिर्फ 1700 से 1900 के बीच, कपास खेतों में काम करने के लिए 40 लाख अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर यू.एस. लाया गया ताकि उन पर जानवरों की तरह अधिकार जताकर खरीदा और बेचा जा सके। (यहां तक कि अमेरिका के संस्थापक भी नीग्रो गुलामों के मालिक थे और उनका इस्तेमाल करते थे)।
फलस्वरूप, कपास फलने–फूलने लगा। 1800 के दशक के मध्य तक अमेरिका प्रतिवर्ष लगभग दो अरब टन कपास निर्यात कर रहा था।
यह सही है कि इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ असंतोष था, लेकिन जब इसने गृहयुद्ध का रूप ले लिया तब राष्ट्रपति लिंकन ने हस्तक्षेप करके युद्ध जीता और देश को एकीकृत किया।
लेकिन काले और गोरे लोगों को समान अधिकार तो तब मिले जब गांधीवादी नेता मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में अश्वेत लोगों ने (अपने गोरे समर्थकों के साथ) इस लड़ाई को बहादुरी से बढ़ाया। उनका नारा था, ‘हम होंगे कामयाब, हम होंगे आज़ाद एक दिन।’
भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रमुख खोज कैलिको था। यह कोज़िकोड (कालीकट, इसलिए कैलिको) में बनाया गया एक कपड़ा था जिसे सूत और बिनौले के छिलके दोनों का उपयोग करके बनाया जाता था।
भारतीय (और मिस्र) सूत की मेहरबानी से कंपनी और साम्राज्य ने सालाना लाखों पाउंड कमाए। जब औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में कपड़ा मिलों की स्थापना हुई, तो सूती कपड़ा और अधिक महीन व बेहतर हो गया और उसकी मांग बढ़ी। भारतीय सूती कपड़े ने यूके (जहां इसे प्रतिबंधित किया गया था) और खुद भारत में भी अपना मूल्य खो दिया।
गांधीजी ने मिल–निर्मित कपड़े के सांस्कृतिक और शोषक मूल्य को समझा। इसी के चलते उन्होंने चरखे और घर की बनी खादी को महत्व दिया। आर्थिक मूल्य के अलावा, यह आज भी राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना जगाता है। अर्थात कपास एक क्रमिक परिवर्तन नहीं लाया, बल्कि राष्ट्रवाद की भारतीय भावना में एक गहरे परिवर्तन को झटके से शुरू किया। यह कितना अन्यायपूर्ण है कि वर्तमान समय के खद्दरधारी नेताओं के युग में, ढाई लाख से अधिक किसान सिर्फ इस कारण आत्महत्या कर चुके हैं कि वे कपास की खेती करने के लिए उठाए गए ऋणों का भुगतान नहीं कर सके। और राहत की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.thehindu.com/migration_catalog/article12928220.ece/alternates/FREE_660/TH12-COTTON-BRSC