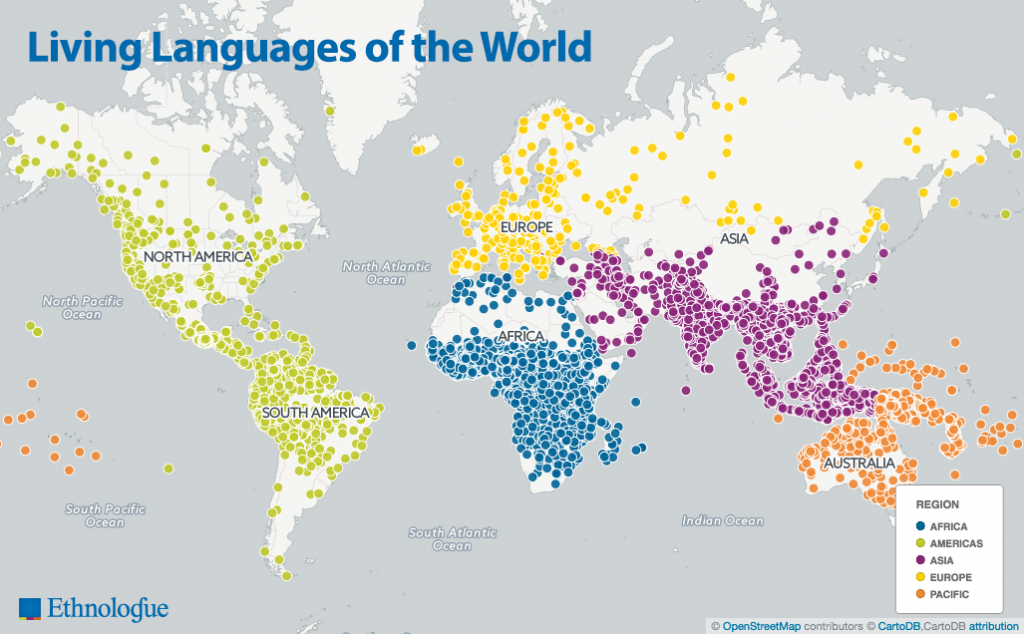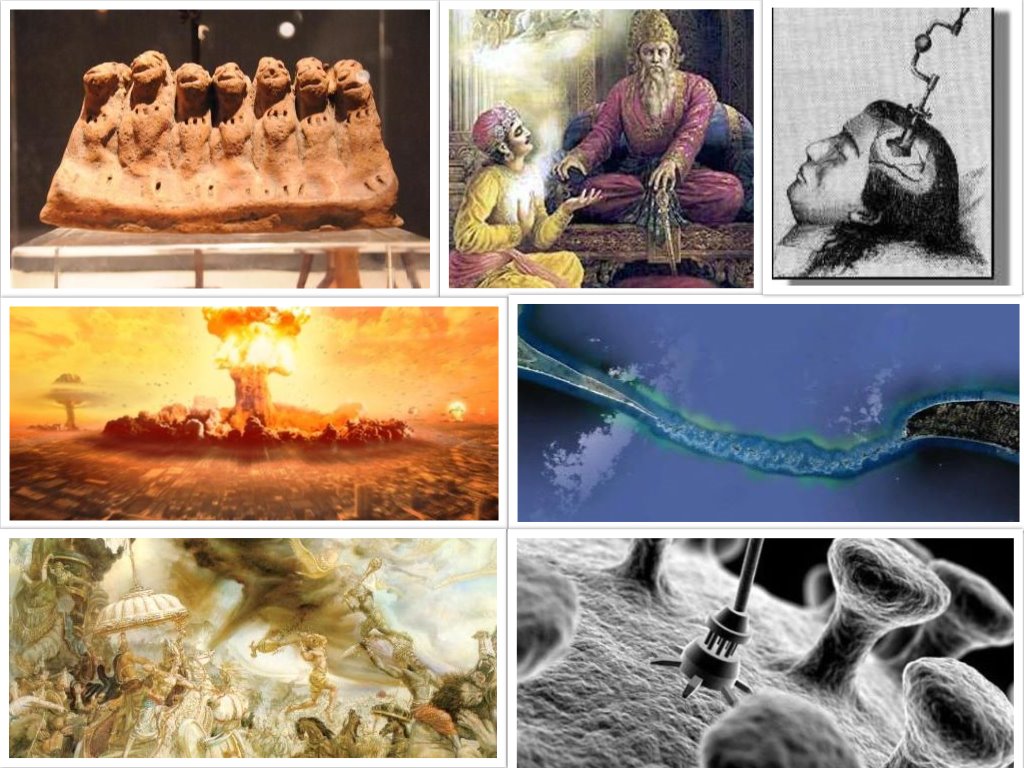लेख की शुरुआत मैं एक गुज़ारिश के साथ करना चाहता हूं। हम अचानक ही मुश्किल और अनिश्चित दौर से घिर गए हैं। अनजाने भविष्य का डर और आशंका बेचैनी पैदा कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस डर को बढ़ाने में हमारा कोई योगदान ना हो, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कैसी जानकारी साझा कर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के ज़रिए। जब भी आप कुछ देखें या पढ़ें तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें: क्या मुझे इस जानकारी पर भरोसा है? अगर यह जानकारी किसी खास विषय से सम्बंधित है तो क्या मैं इसे परखने के लिए पर्याप्त जानकार हूं? क्या दी गई जानकारी के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं? क्या कहीं और भी यह बात कही गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) या स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में क्या कहता है? क्या आपने व्हाट्सएप पर प्राप्त सरकारी आदेश का उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आदेश से मिलान किया है? यदि थोड़ी भी शंका हो तो हमें संदेश साझा करने और आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। वरना हम लोगों को गलत जानकारी देंगे जो उन्हें जोखिम में डाल सकती है।
कोविड-19 महामारी कई लोगों के लिए एक वरदान के रूप में आई है कि वे अपने अज्ञान को समझ व ज्ञान रूपी हथियार का रूप देकर, प्राय: सांस्कृतिक गर्व का मुलम्मा चढ़ाकर दुनिया के समक्ष पेश कर सकें। डिजिटल टेक्नॉलॉजी ने कई लोगों को विशेषज्ञ, विद्वान, डॉक्टर और सर्वज्ञ बना दिया है। मोबाइल फोन और कुछ अन्य माध्यमों के ज़रिए वे इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग बेतुकी और भ्रामक जानकारी फैलाने में कर रहे हैं। इनमें कई बार ऐसी बकवास भी शामिल होती है जो आज़माने वालों के लिए घातक हो सकती है।
कोरोनोवायरस (SARS-CoV-2), कोविड-19 की शारीरिक महामारी के साथ जुड़ी जानकारी की महामारी के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। सबसे अधिक बेतुकी बातें संक्रमण के इलाज और इससे बचाव के उपायों के बारे में कही जा रही हैं। जिससे एक सवाल यह उठता है: गड़बड़ क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? सरल स्तर पर देखें तो, सनसनीखेज़ सामग्रियां डर और उम्मीद के चलते फैल रही हैं, और जीवित रहने के लिए हमारे दिमाग की एक प्रवृत्ति खतरों को बड़े रूप में देखने की है। ऐसा अक्सर महामारी, आपदाओं और युद्ध के समय होता है। पर इस समय हालात को अधिक जटिल और खतरनाक बनाने वाले तीन कारक हैं: पहला, इंटरनेट पर मौजूद असत्यापित अथाह ‘ज्ञान’ के भंडार तक आसान पहुंच; दूसरा, डिजिटल मीडिया की बदौलत प्रसार की तीव्र गति और आसान पहुंच; और तीसरा, सामाजिक और राजनैतिक ध्रुवीकरण जो साज़िश की परिकल्पनाओं को तथा भयंकर पक्षपाती अभिमान से भरे छद्म वैज्ञानिक कथनों को जन्म देता है।
इनमें सबसे प्रचलित हैं खांसी और ज़ुकाम या सामान्य प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए आज़माए जाने वाले घरेलू नुस्खों का विस्तार। इनमें से कुछ उपाय तो गर्म पानी से गरारे करने और गर्मागरम रसम पीने जैसे साधारण सुझाव हैं। इनका एक अन्य स्तर है स्व-परीक्षण; जैसे एक संदेश कहता है कि यदि आप 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक सकते हैं तो आप संक्रमित नहीं हैं। इंटरनेट गलत सूचनाओं से भरा पड़ा है, जिनसे आप चलते-चलते टकरा जाएंगे। गलत सूचनाओं तक संयोगवश पहुंचना कहीं आसान है बनिस्बत प्रामाणिक जानकारी तक पहुंचने के, जिसे खोजना पड़ता है और प्रामाणिकता को परखने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं।
गलत सूचनाएं अक्सर आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज़ों और सील-ठप्पों के साथ पेश की जाती हैं। इनमें से कुछ नामी पेशेवरों के हवाले से आती हैं; जैसे एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट को यह कहते सुना गया था कि जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं उन्हें, परीक्षण किट की कमी के चलते, आठ दिनों के बाद ही परीक्षण के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और सबसे कुख्यात व्हाट्सएप पर कई हास्यास्पद चीज़ें चल रही हैं। जैसे लहसुन कोरोनावायरस को ठीक कर सकता है, या हर 15 मिनट में गर्म पानी पीने से संक्रमण से बचा जा सकता है। सबसे अधिक रोमांचक सलाह शराब और गांजा का सेवन करने की है; दावा है कि दोनों ही वायरस को मार सकते हैं। अमेरिका में काफी प्रचलित सलाह है कि ‘चमत्कारी मिनरल घोल’ यानी ब्लीच वायरस का सफाया कर सकता है। प्रसंगवश बता दें कि यह आपका भी सफाया हमेशा के लिए कर देगा।
मेसेजेस ने इस विचार को भी बढ़ावा दिया है कि मास्क लगाने से वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रहा जा सकता है – यह एक खतरनाक विचार है क्योंकि यह विचार एक मिथ्या आत्मविश्वास पैदा करता है और फिर आपसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार करवाता है। इसके चलते उन लोगों के लिए मास्क की कमी भी हो गई जिन्हें इनकी वाकई ज़रूरत थी। और अंत में, निश्चित ही यह झूठी घोषणा थी कि सरकार ने पूरे इलाके में छिड़काव करके हवा में ही वायरस के खात्मे का इंतजाम किया है।
यह तब और भी चिंताजनक हो जाता है जब ये मूर्खतापूर्ण बातें आधिकारिक नीति बन जाती हैं: स्वास्थ्य मंत्रालय सलाह देता है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक उपचार कोरोनोवायरस के ‘लक्षणों से निपटने’ में मददगार हैं! जबकि इस तरह के दावों का रत्ती भर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी ये सरकार की ओर से ज़ारी किए गए हैं। विशेषज्ञों द्वारा इस पर आपत्ति उठाने पर मंत्रालय ने ‘स्पष्टीकरण’ दिया है कि यह सलाह ‘सामान्य’ वायरस संक्रमण के संदर्भ में जारी की गर्इं है।
यदि कोई इन ‘उपचारों’ को अपना ले तो परिणाम भयावह होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरोनोवायरस के इलाज के लिए क्लोरोक्वीन और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग की वकालत की है। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि “मैं एक ऐसा आदमी हूं जो बहुत सकारात्मक सोच रखता हूं, विशेष रूप से इन दवाओं के मामले में। यह सिर्फ एक एहसास है, सिर्फ एक एहसास है। मैं एक स्मार्ट आदमी हूं।”
इन दवाओं की प्रभाविता के बारे में केवल कहे-सुने प्रमाण उपलब्ध हैं और इन्हें लेकर परीक्षण चल रहे हैं लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पहले ही इस ‘उपचार’ की पैरवी ने मुश्किल खड़ी कर दी है: इन दवाओं की जमाखोरी से इनकी उपलब्धता उन लोगों के लिए कम हो गई है जिन्हें अन्य बीमारियों के इलाज में इनकी ज़रूरत है। लोग कोरोनोवायरस से अपने को बचाने के लिए अब खुद ही इन अत्यधिक ज़हरीली दवाओं का सेवन रहे हैं, जिसके कारण एरिज़ोना और नाइजीरिया में मौतें भी हो चुकी हैं। इसी तरह के हालात भारत में भी बन सकते हैं।
साज़िश परिकल्पनाओं की भी कोई कमी नहीं है। एक प्रचलित बयान यह है कि कोरोनावायरस 5-जी मोबाइल तकनीक के परिणामस्वरूप उपजा है; यह वायरस के माध्यम से लोगों को बीमार करता है। मलेशियाई सरकार को अपने नागरिकों को आश्वस्त करना पड़ा कि यह वायरस लोगों को रक्त-पिपासु दैत्य में नहीं बदलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणपंथी लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट की बाढ़ लगा दी है कि कोरोनावायरस ट्रम्प विरोधी हिस्टीरिया पैदा करने की और ‘देश को अस्थिर करने’ की साज़िश है। इस डर को हवा दी जा रही है कि डब्लूएचओ ‘राष्ट्रों को नियंत्रित कर रहा है और कई लोगों को मारने के लिए जबरन टीके लगाए जाएंगे।’ इसका एक परिणाम इस रूप में सामने आ रहा है कि दक्षिण-पंथी रुझान वाले नागरिक इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और लापरवाही भरा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे बाहर खाना खाना या हाथ मिलाना (यह साबित करने के लिए कि वे सख्त हैं)।
ज़्यादा गहरे स्तर पर दक्षिणपंथी लोग “वायरस के कारण और उसकी उत्पत्ति के बारे में साज़िश-सिद्धांत पेश कर रहे हैं, और इन मनगढ़ंत कहानियों का उपयोग आप्रवासियों, अल्पसंख्यकों या उदारवादी लोगों को बलि का बकरा बनाने हेतु कर रहे हैं।” चीनी मूल के अमेरिकी नागरिकों के साथ दुव्र्यवहार की खबरें तो सामने आ भी चुकी हैं क्योंकि ट्रम्प ने “चीनी वायरस” शब्द प्रचलित कर दिया है। भारत में भी, पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों पर इसी तरह के नस्लवादी हमले किए गए हैं। चीन को एक दैत्य साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि वह अपने ही नागरिकों के प्रति अमानवीय और क्रूर व्यवहार कर रहा है, और ऐसी (झूठी) रिपोर्टें पेश की जा रही हैं कि चीन संक्रमित लोगों को मार रहा है।
लेकिन यह पुराना सवाल बरकरार है: लोग इन बकवास बातों में क्यों आ जाते हैं? एक अन्य लेख में इस बात की चर्चा की गई है कि कैसे क्राउडसोर्सिंग द्वारा बकवास भी ‘ज्ञान’ बन जाता है। मोटे तौर पर कहा जाए तो विभिन्न कारणों से आबादी के एक बड़े हिस्से के लोगों में समीक्षात्मक कौशल की कमी के चलते कितनी भी हास्यास्पद या बकवास बात ‘विश्वसनीय’ बन जाती है। सही शिक्षा तक लोगों की पहुंच के अभाव और आधारभूत वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी की कमी के कारण उनके पास लगातार मिल रही इन सूचनाओं की वैधता जांचने का कोई तरीका नहीं होता। इसके अलावा सवाल करने की मानसिकता की अनुपस्थिति, जो वैज्ञानिक स्वभाव का अंतर्निहित हिस्सा है, के कारण वे जो भी देखते, पढ़ते और सुनते हैं उसकी गहन पड़ताल नहीं कर पाते।
यहां स्पष्ट रूप से दो तरह के परिदृश्य हैं
पहली श्रेणी उन लोगों की है जो तार्किकता से शुरुआत तो करते हैं लेकिन एक समय बाद प्रामाणिक से दिखने वाले नकली दस्तावेज़ों या वैज्ञानिक लगने वाले तर्कों में फंस जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण यह बयान है कि होम्योपैथी कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए सभी अद्भुत दवाएं उपलब्ध करा रही है। इस तरह के दावे वैसी ही भाषा शैली का उपयोग करते हैं जैसी कि आधुनिक चिकित्सा में उपयोग की जाती है, जिससे होम्योपैथी चिकित्सा बिल्कुल इसके समान और इसका विकल्प लगने लगती है। यह उस छद्म विज्ञान को ढंक देती है जिस पर होम्योपैथी आधारित है। कोरोनोवायरस महामारी के इलाज और उसके टीके सम्बंधी ये दावे इस संक्रमण के खिलाफ अजेयता का भ्रम पैदा कर सकते हैं।
‘जनता कर्फ्यू’ के मामले में सोशल मीडिया पर एक छद्म वैज्ञानिक व्याख्या काफी प्रचलित है: किसी एक स्थान पर कोरोनोवायरस 12 घंटे जीवित रहता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। इसलिए सार्वजनिक स्थलों या बिंदुओं को, जहां कोरोनावायरस पड़ा रह गया होगा, यदि 14 घंटे तक छुआ नहीं जाएगा तो इससे कोरोनावायरस की शृंखला टूट जाएगी। यह ना केवल अजीबो-गरीब तर्क है बल्कि यह वायरस के जीवन काल के तथ्य के आधार पर भी गलत है। इस प्रकार के कर्फ्यू वायरस के संपर्क में आने में कमी ला सकते हैं, और आपातकालीन उपायों के हिसाब से यह एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा कि ‘कोरोनावायरस की शृंखला टूट जाएगी’।
व्हाट्सएप पर एक और बेतुका तर्क दिया जा रहा है कि भारत के 130 करोड़ लोग यदि एक समय, एक साथ ताली और शंख बजाएंगे तो इतना कंपन पैदा होगा कि वायरस अपनी सारी शक्ति खो देगा। यदि कुछ ट्वीट्स की मानें तो ऐसा करके हमें पहले ही बड़ी सफलता मिल चुकी है क्योंकि “नासा SD13 तरंग डिटेक्टर ने ब्राहृाण्ड स्तरीय ध्वनि तरंग डिटेक्ट की हैं और हाल ही में बनाए गए बायो-सैटेलाइट ने दिखाया है कि कोविड-19 स्ट्रेन घट रहा है और कमज़ोर हो रहा है” और वह भी सामूहिक शंखनाद के कुछ मिनटों बाद।
इससे ज़्यादा ऊटपटांग बात कोई हो नहीं सकती। दूसरी ओर, सामाजिक दूरी का विचार, जिसे सरकारें जी-जान से बढ़ावा देने में जुटी हैं, तब हवा में उड़ गया जब कई लोग राजनेताओं के आव्हान से उत्साहित होकर संक्रमण से लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के सम्मान में लोग ताली-थाली बजाने के लिए अपने-अपने घरों से बाहर निकल कर एक साथ जमा हो गए। लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, हम वास्तव में अपने आसपास इन कार्यकर्ताओं को नहीं चाहते क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना है। मकान मालिकों ने एयरलाइन कर्मचारियों और यहां तक कि चिकित्सा पेशेवरों को घर खाली करने को कहा है – यह काफी निराशाजनक स्थिति दिखती है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को महत्व नहीं देते हैं, उनकी भी जो संकट के समय हमारी सेवा करते हैं। जिन लोगों को क्वारेंटाइन किया गया है उनके प्रति सहानुभूति में कमी और उनकी निजता पर आक्रमण और भी शर्मनाक है।
हम वास्तव में सबसे भौंडा इतिहास बनते देख रहे हैं
दूसरा, हमारे यहां कई ऐसे लोग हैं जो निहित रूप से अंधविश्वासों और अतार्किक विश्वासों के प्रति संवेदी हैं। इसके लिए विचित्र धार्मिकता से लेकर इन विश्वासों को मानने वाली संस्कृति में परवरिश जैसे कई कारण ज़िम्मेदार हैं। इन मामलों में ज्ञान और जानकारी बुज़ुर्गों, समुदाय प्रमुखों और धार्मिक गुरुओं से आंख मूंदकर प्राप्त की जाती है, उस पर सवाल नहीं उठाए जाते; दिमागों को सवाल उठाने या प्रमाण खोजने के लिए तैयार नहीं किया जाता। इसलिए इन लोगों को जो कुछ भी सूचनाएं मिलती हैं, उसे मान लेते हैं, और इससे भी अधिक तत्परता से उन सूचनाओं को मान लेते हैं जो किसी भी किस्म के अधिकारियों – राजनीतिक नेताओं, धार्मिक हस्तियों – से प्राप्त हुई हैं। ‘गो कोरोना गो’ का एक वीडियो बीमारी से लड़ने में एक आशावादी मनोस्थिति बनाने का अच्छा साधन हो सकता है लेकिन यह वीडियो एक मुगालता भी पैदा करता है कि कोरोनोवायरस को जाप से, खासकर सामूहिक जाप से भगाया जा सकता है।
कोरोनावायरस सम्बंधी इस तरह की बेतुकी बयानबाज़ी करने वाले अधिकतर वे लोग हैं जो धार्मिक और राष्ट्रवादी गौरव से भरे होते हैं। यह वक्त, जो महान राजनीतिक ध्रुवीकरण और तीव्र सामाजिक आक्रोश का गवाह है, ने सांस्कृतिक श्रेष्ठता के आख्यानों से पूर्ण दंभ के उग्रवादी रूप को जन्म दिया है।
इसी के चलते, गोमूत्र का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जा रहा है और बिना सोचे-समझे लोगों पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। दक्षिणपंथी राजनेताओं का दावा है कि गोमूत्र और गोबर कोरोनोवायरस का इलाज कर सकते हैं, और हवन वायरस को मार सकता है। इनमें से कुछ ने विशेष सभाओं का आयोजन किया जहां आमंत्रित लोगों को गोमूत्र पीने के लिए दिया गया। कई ज्योतिष हमें बताते हैं कि हम अस्तित्व के संकट का सामना क्यों कर रहे हैं, और यह कब दूर होगा। एक अन्य दावा कहता है कि प्राचीन भारतीय योग के श्वसन का तरीका कोरोनावायरस के संक्रमण से बचा सकता है, और यह भी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयुक्त अश्वगंधा ‘मानव प्रोटीन से कोरोना प्रोटीन को जुड़ने नहीं देगी।’ इंडोनेशिया में मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि वजू करना वायरस को मार सकता है।
जो लोग इनमें से किसी भी कथन को गंभीरता से लेते हैं और मानते हैं कि उनके पास कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए उपाय है तो हो सकता है कि वे खुद को और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं।
हमें घेरती जा रही इस अज्ञानता के और भी अधिक भयावह और दीर्घकालिक प्रभाव हैं। आक्रामक शाकाहार-श्रेष्ठता के उन्माद में स्वनामधन्य ज्ञान उड़ेला जा रहा है: कोरोनावायरस की उत्पत्ति चीन के ‘मांस बाज़ार’ से हुई, जहां मारे गए जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियां एक साथ होती हैं, जिससे वायरस एक प्रजाति से होते हुए दूसरी प्रजाति और अंतत: मनुष्य में आ गया। यह बात मांसाहार की कटु आलोचना के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। मांस खाने वालों को दोष देते हुए कतिपय सभ्यता की श्रेष्ठता के दावे किए जा रहे हैं और सभ्यता के घोर अनुयायी मांग कर रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति कोरोनावायरस की प्रतिमा से क्षमा याचना करें कि उन्होंने मांस खाया। संक्रमित मटन बाज़ार दिखाने वाले वीडियो भावनाओं को और भड़का रहे हैं। इस प्रकार कोरोनावायरस मांस खाने वालों के खिलाफ प्रकृति का प्रतिशोध बन गया है। इससे भारत में मुर्गियों की कीमत बहुत कम हो गई है, और यह उद्योग आर्थिक संकट झेल रहा है।
सिर्फ अनुशंसित वेबसाइटों (जैसे डब्ल्यूएचओ) से जानकारी प्राप्त करने की सलाह और गुज़ारिश किसी भी तरह से लोगों को गलत सूचना मानने और आगे बढ़ाने से रोक नहीं रही है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत सी गलत सूचनाएं जानबूझकर बरगलाने के लिए प्रचारित की जाती हैं, अक्सर दक्षिणपंथी सांस्कृतिक लोगों द्वारा। जब तक हम इस सूचना की महामारी के “प्रसार की शृंखला” को नहीं तोड़ेंगे तब तक यह जारी रहेगी।
लिहाज़ा, डिजिटल मीडिया कई मायनों में उन मासूम लोगों के लिए एक उपहार है जो उनको बताई गई किसी भी बकवास पर, और उसे रचने वालों पर यकीन कर लेते हैं। फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक के तमाम प्लोटफार्म, जिन पर कोई भी कुछ भी कह या लिख सकता है, वास्तव में इन्हें उपयोग करने वाले सर्वज्ञाताओें (चाहें नादान हों या किसी मत के) के लिए मुफ्त में उपलब्ध हथियार की तरह है जिसे किसी पर भी चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में दुनिया में किसी तरह की मूर्खता नहीं थी लेकिन मूर्खता को सर्वव्यापी बनाने के साधन अनुपस्थित थे, जिससे किसी बेतुकेपन के निर्माण और प्रसार की गति सीमित थी।
बड़ी टेक कंपनियां गलत सूचना के प्रसार को रोकने की कोशिश कर रही हैं लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे खुद के बनाए गए विशालकाय जाल को नियंत्रित कर पाएंगी। आधुनिक तकनीक और दुनिया के असमीक्षात्मक, रूढ़िवादी सोच की जुगलबंदी हमें यह याद दिलाती है कि जो समाज अंधविश्वास को बढ़ावा देता है वह छद्म विज्ञान में लौट जाता है और तार्किकता को कम करता है। इस परिस्थिति का उपयोग सांस्कृतिक और राजनीतिक लड़ाई में हथियार के रूप में किया जाता है।(स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/5ea89d09b67f3800075cd1ab/960×0.jpg?fit=scale