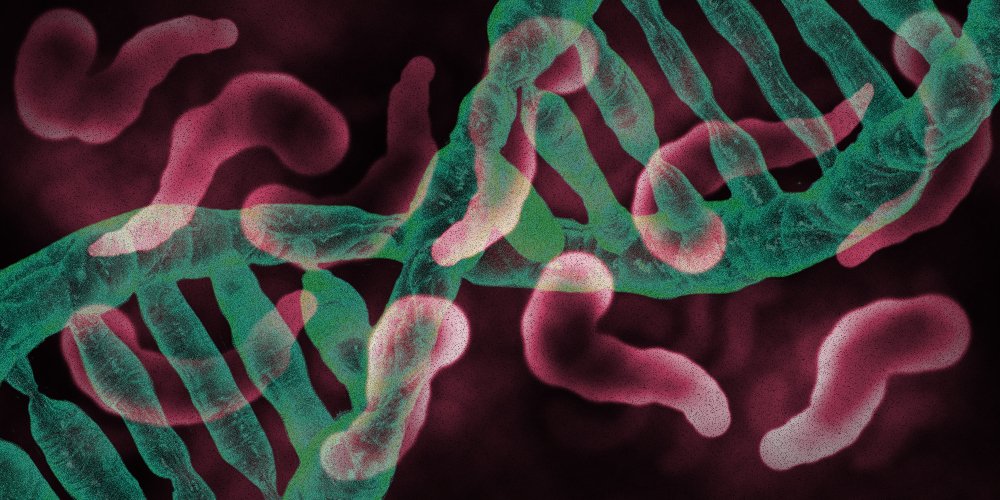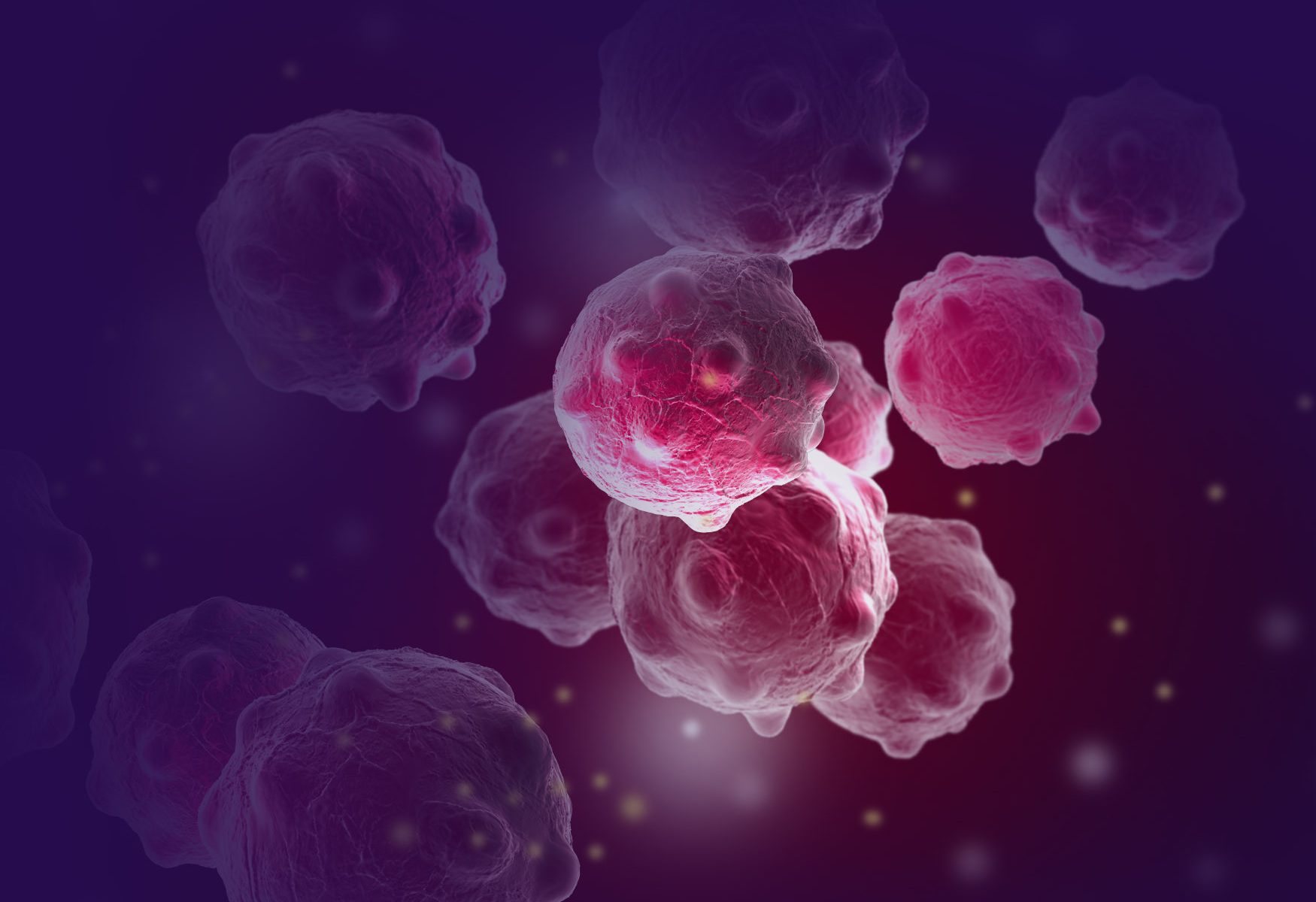छिपकली को जब भी किसी खतरे का अंदेशा होता है तो वह अपने बचाव में अपने शरीर से पूंछ अलग कर गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। अगले 60 दिनों के भीतर छिपकली के शरीर पर नई पूंछ आ जाती है। लेकिन नई पूंछ कैसे और क्यों आती है? एरिज़ोना स्टेट युनिवर्सिटी के डॉ. केनरो कुसुमी और उनके साथियों ने अपने शोध में इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि दोबारा पूंछ विकसित करने के लिए छिपकली अपने शरीर के किसी खास हिस्से के जीनोम में लगभग 326 जीन्स को सक्रिय कर देती है। इसके अलावा वे ‘सैटेलाइट कोशिकाओं’ को भी सक्रिय कर देती हैं, जो विकसित होकर कंकाल की पेशियों और अन्य ऊतकों में तबदील हो सकती हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि चूंकि मनुष्यों में भी सैटेलाइट कोशिकाएं होती हैं इसलिए संभावना है कि इन्हें सक्रिय करके मनुष्यों में भी पेशियों और उपास्थियों को पुन: विकसित किया जा सके।
छिपकली जैव विकास के क्रम में काफी देर से अस्तित्व में आई थीं। छिपकली लगभग 31-32 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई जबकि उनसे पहले केंचुए लगभग 51 करोड़ वर्ष पूर्व और चपटे कृमि लगभग 84 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तिस्व में आ चुके थे। अरस्तू ने इन्हें ‘पृथ्वी की आंत’ और डार्विन ने ‘प्रारंभिक जुताई करने वाले’ की उपमा दी थी। प्रोसिडिंग्स ऑफ रॉयल सोसायटी में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह पता किया है कि कृमियों की 35 विभिन्न प्रजातियां शरीर का कोई हिस्सा कटकर अलग हो जाने पर उसे पुन: विकसित (या अंग पुनर्जनन) कैसे करती हैं। जैसे कम-से-कम चार तरह के कृमि अपने सिर को दोबारा विकसित कर लेते हैं। तो छिपकली की तरह इन जीवों की जीव वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का अध्ययन अंग पुनर्जनन की बेहतर समझ बनाने में मददगार होगा।
सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि विकास क्रम में पहले अस्तित्व में आए कृमि, अपना सिर तक पुन: विकसित कर पाते हैं जबकि उनके बाद अस्तित्व में आर्इं छिपकलियां सिर्फ पूंछ दोबारा बना पाती हैं। और उनके भी बाद आए ‘ऊंचे दर्जे के जानवर’ तो कोई भी अंग फिर से नहीं बना पाते। इस मामले में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। युनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड की प्रोफेसर एलेक्सेन्ड्रा बेली ने अपनी समीक्षा इवॉल्यूशनरी लॉस ऑफ एनिमल रीजनरेशन: पैटर्न एंड प्रोसेस (विकास के दौरान जीवों में अंग-पुनर्जनन क्षमता की हानि: पैटर्न और प्रकिया) में बताया है कि पुनर्जनन में नई कोशिकाएं, ऊतक और आंतरिक अंग तो बन सकते हैं लेकिन भुजाओं जैसी रचनाओं के पुनर्जनन पर उम्र, लिंग, पोषण और अन्य कारकों का नियंत्रण होता है। या क्या यह भी हो सकता है कि पुनर्जनन इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि जीवों ने मरम्मत में ऊर्जा खर्च करने की बजाय उसे वृद्धि में लगाया। अंग-पुनर्जनन में लगने वाली ऊर्जा और उससे मिलने वाले लाभ के आधार पर इस प्रक्रिया को फिर से समझने की ज़रूरत है।
युनिवर्सिटी ऑफ बाथ के डॉ. जोनाथन स्लैक द्वारा इएमबीओ रिपोर्ट में एक अध्ययन एनिमल रीजनरेशन: एंसेस्ट्रल केरेक्टर ऑर इवॉल्यूशनरी नॉवेल्टी? (जंतु पुनर्जनन: पूर्वजों की विरासत या वैकासिक नवीनता?) प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन में उन्होंने जेनेटिक विश्लेषण के आधार पर बताया था कि सभी जीवों (छिपकली से लेकर मानवों तक) में आनुवंशिक गुण दो मुख्य जीन, Wnt और BMP, के व्यवहार के कारण दिखते हैं। Wnt जीन कोशिकाओं की तेज़ी से वृद्धि और स्व-नवीनीकरण संकेत देने में मददगार होता है। BMP जीन सभी जीवों में शरीर और अंगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जीन सभी जीवों की सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से ऐसा लगता है कि अंग-पुनर्जनन सभी जीवों में संभव है।
इसके बावजूद, कुत्ते या बिल्ली की पूंछ कटने के बाद दोबारा नहीं आती। वे अपनी कटी पूंछ के साथ ही रहना सीख जाते हैं। डॉ. बेली के अनुसार इन जीवों में, पूंछ को दोबारा विकसित में लगने वाली ऊर्जा के बदले पूंछ के बिना जीना ज़्यादा फायदेमंद या सार्थक लगता है। (जबकि छिपकली के मामले में उसकी पूंछ जीवित बचने और विकास में अहम अंग है।)
छिपकली पर लौटते हैं। छिपकली में दोबारा जो पूंछ विकसित होती है वह दरअसल मूल पूंछ जैसी नहीं होती बल्कि उसकी अधूरी नकल होती है। इस नकली पूंछ में कोई हड्डी नहीं होती बल्कि इसमें उपास्थि होती है और यह मूल पूंछ की तुलना में अधिक नरम और लचीली होती है। कलकत्ता के डॉ. शुक्ल घोष के शब्दों में यह वास्तविक अंग-पुनर्जनन नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति वृद्धि है।
स्टेम सेल तकनीक
हालांकि एरिज़ोना के कुसुमी और उनके साथियों को छिपकली की पुन: विकसित पूंछ के ऊतकों में कोई प्रोजीनेटर कोशिका या स्टेम कोशिका नहीं मिली, लेकिन उभरती हुई स्टेम कोशिका तकनीक से इस क्षेत्र में काफी उत्साह बढ़ा है। इस तकनीक में स्टेम कोशिका की मदद से किसी अन्य अंग की कोशिका या ऊतक प्रयोगशाला में विकसित किए जा सकते हैं। इस तकनीक की मदद से मूत्राशय विकसित किया गया है और एक युवा को लगाया गया, जिसका मूत्राशय क्षतिग्रस्त हो गया था। वर्तमान में किसी भी कोशिका को, चार चुने हुए जीन की मदद से, स्टेम कोशिका बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस तरह प्रेरित बहुसक्षम स्टेम कोशिकाएं, प्रयोगशाला में मनचाहे ऊतक और ऑर्गेनाइड (मूल अंग की तुलना में छोटे अंग) बनाने के लिए उपयोग किए जा रही हैं। हालांकि अभी यह इस तकनीक का आगाज़ है लेकिन भविष्य में इसकी मदद से अंग बनाए जा सकेंगे और इनका उपयोग अंग-पुनर्जनन के लिए किया जा सकेगा। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : http://www.californiaherps.com/lizards/images/ecprincnotaildnco.jpg