डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन
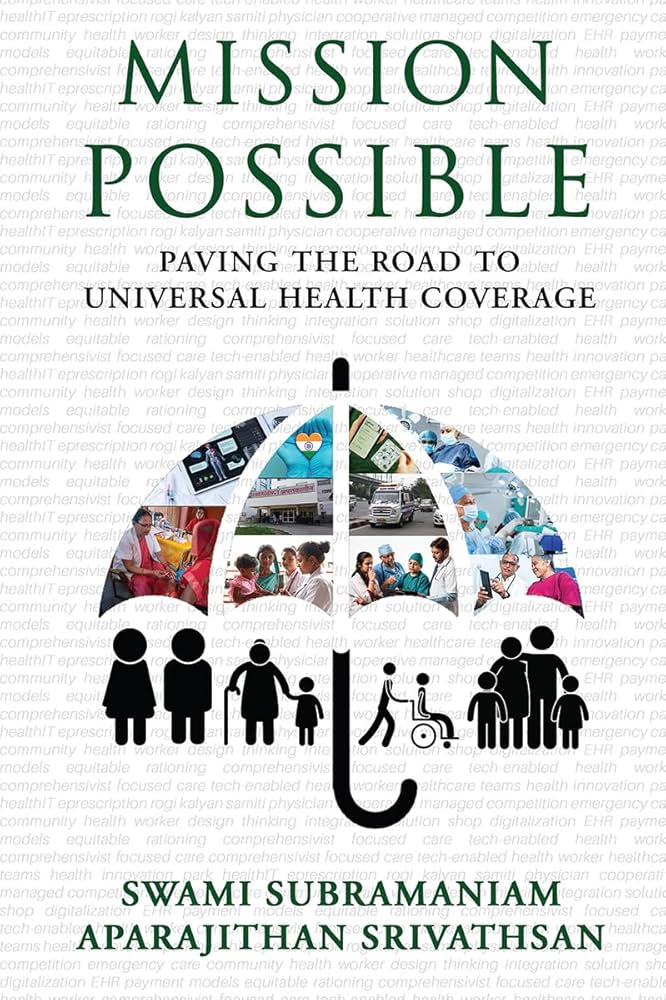
चेन्नई स्थित नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित स्वामी सुब्रमण्यन और अपराजितन श्रीवत्सन अपनी किताब मिशन पॉसिबल में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage – UHC) सुगम करने के लिए राह बनाने के तरीके सुझाते हैं। यह किताब सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। किताब 143 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत (India Population) (जहां 38% बच्चे और 11% वरिष्ठ नागरिक हैं) को ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज करने की बात कहती है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कोई आसान काम नहीं है, और लेखक इसे हासिल करने के तरीके सुझाते हैं।
शुक्र है कि विश्लेषण के आधुनिक तरीकों में हुई प्रगति और सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology – IT) की मदद से यह हासिल करना अब संभव लगता है। यह कहना है दी लैंसेट में प्रकाशित लेख ‘रीइमेजिनिंग इंडिया’स हेल्थ सिस्टम (Reimagining India’s Health System)’ का। इस प्रयास का नेतृत्व अकादमिक लोगों, वैज्ञानिक समुदाय (Scientific Community), सिविल सोसायटी के संगठनों और निजी स्वास्थ्य सेवा (Private Healthcare Sector) के अग्रज़ों द्वारा किया जाना चाहिए। दी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (Public Health Foundation of India – PHFI) ने भारत में एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली (Integrated Healthcare System) के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा (Universal Health Insurance) का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा में जवाबदेह व प्रमाण-आधारित अच्छी गुणवत्ता के तौर-तरीकों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित मानव संसाधन (Skilled Healthcare Workforce) के विकास के लिए स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना, स्वास्थ्य प्रशासन का पुनर्गठन करके उसे अधिक समन्वित तथा विकेंद्रीकृत बनाना और कानून बनाकर समस्त भारतीयों को स्वास्थ्य का हक देना शामिल होगा।
गुणवत्ता में सुधार (Quality Improvement in Healthcare)
इसमें शामिल है भारत में प्रोत्साहक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं (Preventive and Curative Healthcare Services) के प्राथमिक प्रदाता के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (Public Healthcare System) को मज़बूत करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (National Healthcare System) के भीतर निजी क्षेत्र (Private Sector in Healthcare) का एकीकरण करके गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य सम्बंधी खर्च को कम करना। वास्तव में 1946 में, जब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली नहीं थी, तब भोर समिति (Bhore Committee Report 1946) की रिपोर्ट ने भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखी थी। इसने एक त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (Three-Tier Healthcare System) स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसमें सुरक्षात्मक और निवारक सेवाओं को एकीकृत करने और उपचार की फीस भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना चिकित्सा सेवा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया था। समिति ने चिकित्सा शिक्षा प्रणाली (Medical Education System in India) में बड़े बदलाव भी सुझाए थे।
मिशन पॉसिबल बताती है कि जिस तरह आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल व्यक्तिगत पहचान और चुनाव में मतदाता पहचान के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (HealthTech – Healthcare Technology) का उपयोग करने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं (Community Health Workers – CHWs) की टीमों द्वारा सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सकती है। इन टीमों में एक स्थानीय चिकित्सक (Primary Care Doctor) होगा, जिसकी मदद के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (CHWs) का एक समूह होगा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आपात स्थिति को छोड़कर) डॉक्टर के कामों का लगभग 75% काम कर सकते हैं, और मोबाइल फोन (Mobile Health – mHealth) और रोगियों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (Electronic Medical Records – EMR) जैसे साधनों का उपयोग कर सकते हैं। इस टीम में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से लेकर किसी एक अस्पताल में विशेषज्ञ तक शामिल हैं और जैसा कि लेखक कहते हैं, ‘प्रौद्योगिकी एक ऐसी गोंद है जो इस टीम को जोड़े रख सकती है’। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगभग 40,000 की आबादी की सेवा करेगा, और तृतीयक देखभाल देने वाले 75 बिस्तरों वाले ज़िला अस्पताल (District Hospital) के साथ काम करेगा। प्रत्येक राज्य में एक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा (Top Medical Institute in India) होनी चाहिए (जैसे, दिल्ली का AIIMS (All India Institute of Medical Sciences – AIIMS), हैदराबाद का NIMS (Nizam’s Institute of Medical Sciences – NIMS))। सभी एमबीबीएस (MBBS) (और एमएससी बायोटेक (MSc Biotechnology)) के विद्यार्थियों को सामुदायिक चिकित्सा में तीन महीने का प्रशिक्षण लेना चाहिए।
आगे लेखक का सुझाव है कि जिस तरह ज़िला प्रशासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service – IAS) की भूमिका होती है, उसी तरह एक भारतीय चिकित्सा सेवा (Indian Medical Service – IMS) का गठन किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist Doctors) राज्य स्तर पर मदद करें। इसके अलावा, सरकारी चिकित्सा तंत्र के साथ-साथ निजी चिकित्सा केंद्रों एवं संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल, दक्षिण भारत (South India Healthcare Model) में कई नेत्र विज्ञान संस्थान (Ophthalmology Institutes in India) ऐसा कर भी रहे हैं; पिरामिडनुमा चार-स्तरीय मॉडल (Four-Tier Healthcare Model) का उपयोग करते हुए, गांव और शहर के नेत्र देखभाल कर्मचारियों को अस्पतालों के ज़रिए विश्व स्तरीय नेत्र अनुसंधान केंद्रों (Eye Research Centers) से जोड़ा गया है। रोगियों को निदान के लिए नेत्र अस्पताल तक भी नहीं जाना पड़ता है, नेत्र चिकित्सक आधुनिक प्रौद्योगिकियों (Telemedicine in India) की मदद से घर पर ही रोगी की आंखों की जांच करते हैं। इस तरह, सबके लिए स्वास्थ्य (Healthcare for All) की राह बनाई जा सकती है।(स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://m.media-amazon.com/images/I/71EnNJR7GtL.UF1000,1000_QL80.jpg