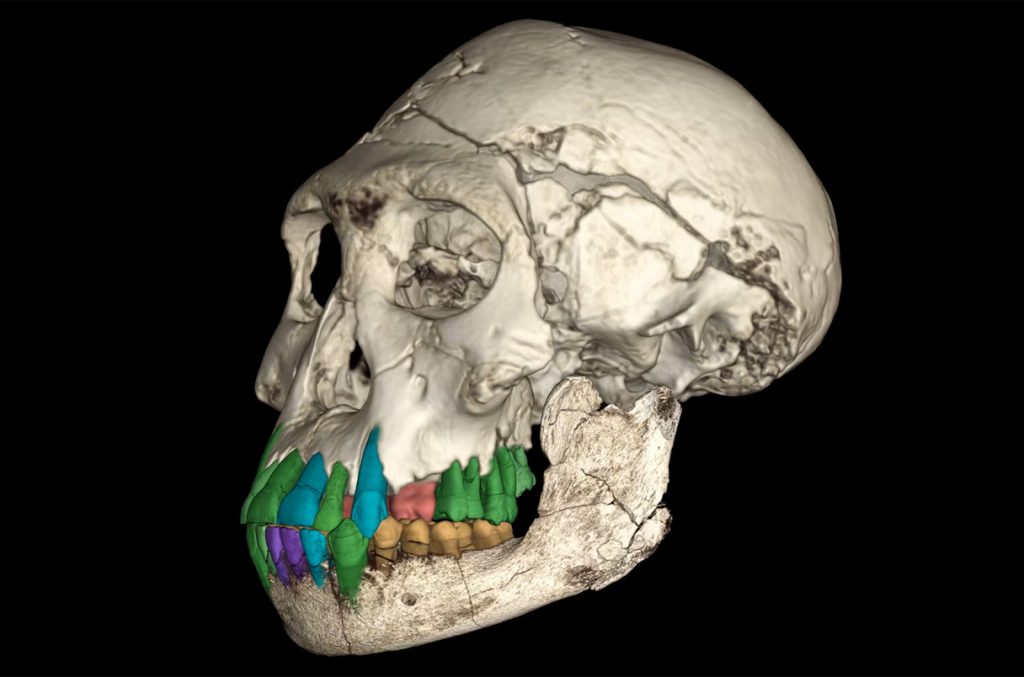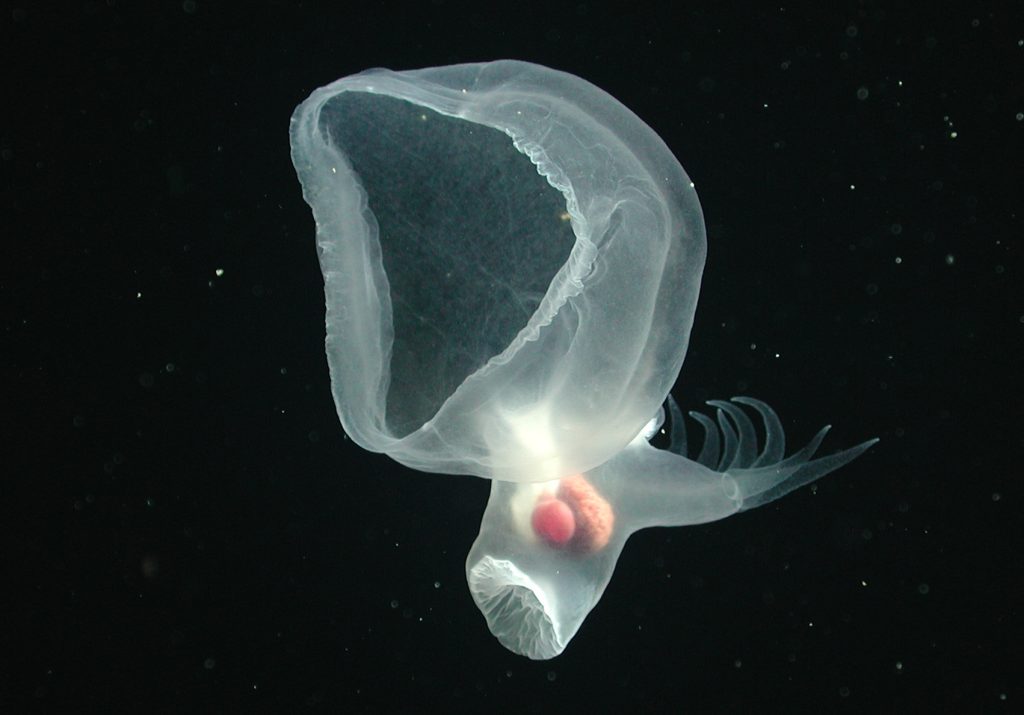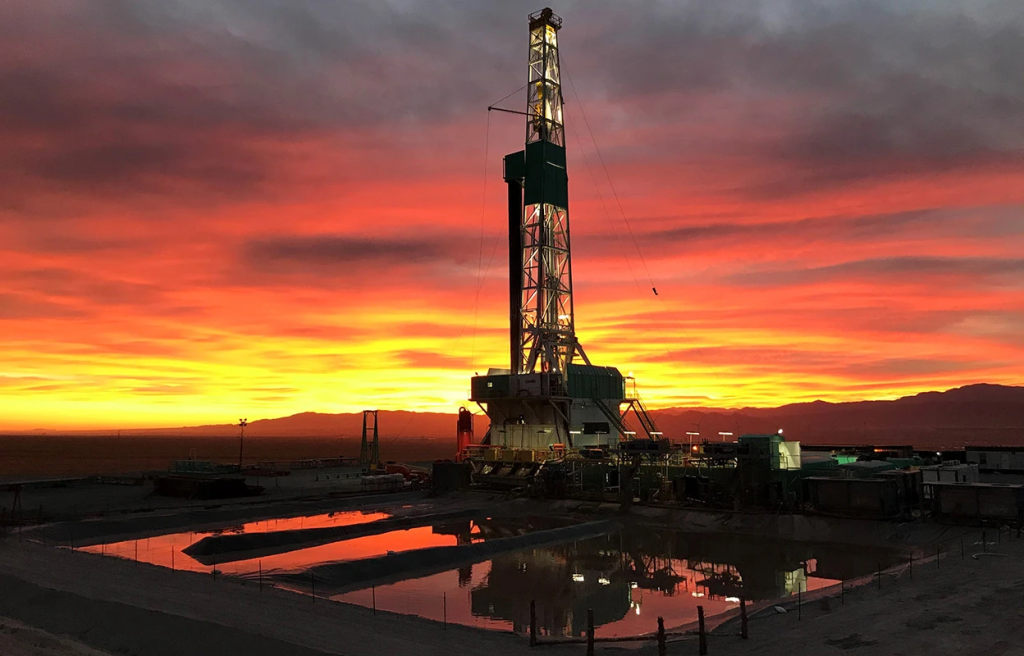डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन, सुशील चंदानी

दीवाली का त्यौहार गुज़रे करीब एक महीना हो गया है। हमारे सभी त्यौहार हमें खुशी-उल्लास देते हैं, लेकिन हमारा दीपों का यह त्यौहार साथ में बहुत ज़्यादा शोर भी देता है। सल्फर डाईऑक्साइड जैसे हानिकारक उत्सर्जन को कम करने और पटाखे फोड़ने पर होने वाले शोर को कम करने के लिए ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की लगातार अपील की जाती है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत निर्देशों, जैसे लड़ियों वाले पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध, के ज़रिए अनिवार्य किया है। लेकिन हर साल इस त्यौहार के मौसम में पटाखों की तेज़ आवाज़ें गूंजती रहती हैं।
लोगों की चिंता पटाखों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण पर केंद्रित रहती है, लेकिन उतनी ही चिंता की बात यह है कि बहुत तेज़ आवाज़ या धमाके हमारी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पटाखों से इतर, साल भर होने वाले शोर या ध्वनि प्रदूषण पर अन्य तरह के प्रदूषण की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा लगता है कि शोर को हमारे आसपास के पर्यावरण के हिस्से के रूप में अधिक आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है, खासकर तब जब यह शोर आप स्वयं पैदा कर रहे हों।
ध्वनि तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ती है। इन तरंगों में ऊर्जा होती है। जितनी अधिक ऊर्जा होगी, उतनी ही ज़्यादा तीव्र तरंग होगी और उतनी ही तेज़ आवाज़ होगी। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल (डीबी) पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसलिए जब ध्वनि स्तर 10 डेसिबल बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि ध्वनि की तीव्रता दस गुना बढ़ गई है। डीबी पैमाने पर, मानव श्रवणशक्ति की शुरुआत 0 डीबी पर सेट की गई है। एक फुसफुसाहट की ध्वनि की माप इस पैमाने पर 30 डेसिबल आती है, और सामान्य बातचीत की ध्वनि की माप 60 डेसिबल।
तेज़ धमाके के साथ फूटने वाले पटाखे की ध्वनि तीव्रता, 10 फीट दूर मापने पर, 140 डेसिबल आती है। यह तीव्रता कान के कॉक्लिया (आंतरिक कान में एक सर्पिलाकार रचना जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है) में मौजूद रोम कोशिकाओं को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। कॉक्लिया कान के परदे के माध्यम से कंपन प्राप्त करता है और फिर रोम कोशिकाएं उन्हें तंत्रिका संकेतों में बदल देती हैं। इन रोम कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने से वे ध्वनि के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। नतीजतन, रोम कोशिका द्वारा प्रतिक्रिया करने और तंत्रिका संकेतों को मस्तिष्क तक भेजने के लिए तेज़ या ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। रोम कोशिकाएं मध्यम आवाज़ के असर के बाद कुछ हद तक ठीक हो सकती हैं। लेकिन हमारी त्वचा कोशिकाओं के विपरीत, ये कोशिकाएं पुनर्जनन में असमर्थ हैं। इसलिए बार-बार होने वाले आघातों से उबरना इन कोशिकाओं के लिए मुश्किल हो सकता है। नतीजतन, लगातार तेज़ शोरगुल के कारण सुनने की क्षमता घट सकती है।
छोटे बच्चों के संवेदनशील कानों के लिए तेज़ आवाज़ें एक गंभीर खतरा हैं, क्योंकि सुनने की क्षमता में मामूली कमी भी उनकी सीखने की क्षमता को कम कर सकती है। शोर के अत्यधिक संपर्क के कारण होने वाला ध्वनि आघात अक्सर कान बजने (टिनिटस) की समस्या पैदा करता है, जिसमें कहीं कुछ आवाज़ न होने पर भी आपको कानों में सीटी बजने सी आवाज़ सुनाई देती रहती है। यह ‘सीटी की आवाज़’ क्षतिग्रस्त रोम कोशिकाओं की असामान्य विद्युत गतिविधि का संकेत है। आम तौर पर, यह आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक लगातार शोर-शराबे के संपर्क में रहने से यह आपके जीवन का स्थायी लक्षण बन सकती है। बेशक, टिनिटस बुज़ुर्गों को भी हो सकता है, जो उम्र से सम्बंधित क्षति के कारण पैदा होता है।
लंबे समय तक मध्यम-तीव्रता वाली आवाज़ों (शोरगुल) के संपर्क में रहने से भी सुनने की क्षमता ठीक वैसे ही कम हो सकती है, जैसे तेज़ आवाज़ें सुनने से होती है। भारतीय शहरों की सड़कों पर यातायात का शोर एक दिन में 60 से 102 डेसिबल तक मापा गया है। साल 2008 में इंडियन जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरनमेंटल मेडिसिन में हैदराबाद शहर के यातायात पुलिसकर्मियों पर किया गया एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। अध्ययन में पांच साल की सेवा के बाद सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों में सुनने की क्षमता में कमी पाई गई थी, ऐसे ही नतीजे सुब्रतो नंदी और सारंग धात्रक को भारत में व्यावसायिक शोर पर किए गए सर्वेक्षण में मिले थे।
इयरप्लग जैसे निवारक उपाय सुनने की क्षमता में कमी के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। निर्माण उद्योग जैसे कुछ पेशों में ज़रूरत के अनुसार इयरप्लग अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसे और अधिक व्यापक बनाने की ज़रूरत है। शायद, ग्रीन पटाखों के चलन में आने के पहले ही, त्यौहार की रातों में इयरप्लग पहनना एक आम दृश्य बन जाएगा। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://th-i.thgim.com/public/incoming/5lhhr0/article68932329.ece/alternates/LANDSCAPE_1200/31102024_Deepavali%20Festival%2006.jpg