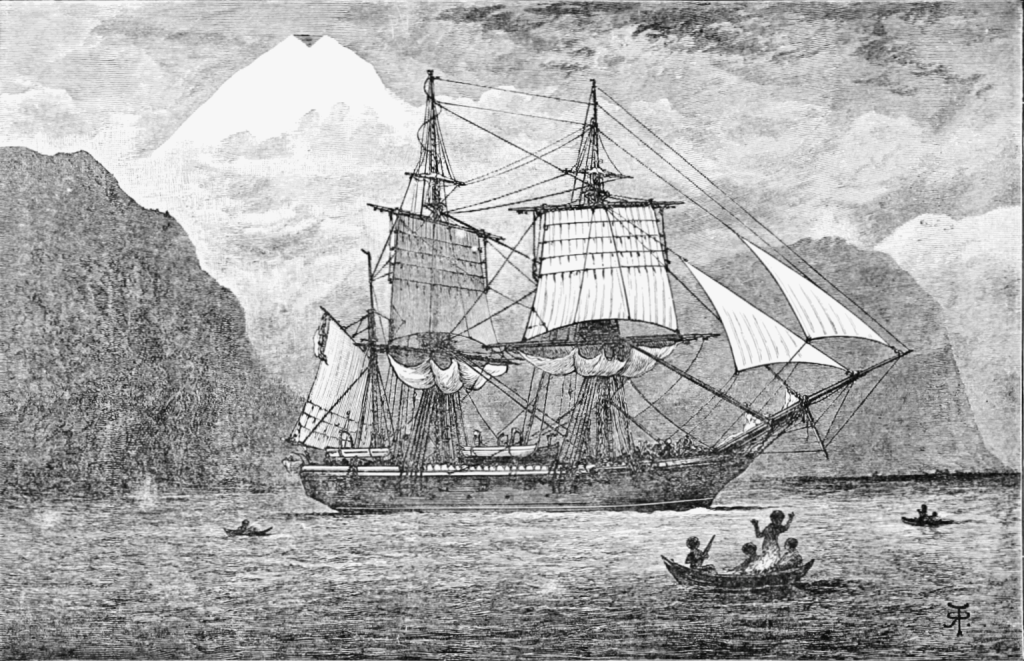
संस्कृति-जैविकी असामंजस्य
प्राकृतिक वरण हमें कम फिट बना सकता है, इसका एक कारण और है – वह है जिस पर्यावरण में हमारा विकास हुआ था और आज जिस पर्यावरण का हम अनुभव करते हैं, उनके बीच असामंजस्य।
यह अक्सर कहा जाता है कि हमारी वर्तमान सभ्यता हमारी पाषाण-युगीन जैविकी से मेल नहीं खाती। बदकिस्मती से, इस तरह मान लिए गए असामंजस्य का वैकासिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है। इसका उपयोग हमारी हर समस्या की ‘व्याख्या’ के लिए किया जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए हमें अपनी आधुनिक जीवन शैली को पूरी तरह त्यागकर उस तरह जीना चाहिए जिस तरह हम कथित तौर पर स्वर्णिम पाषाण युग में जीते थे। वैकासिक जीव विज्ञान का ऐसा लापरवाह और बगैर सोचे-समझे उपयोग उसे बदनाम करता है और काफी हानि पहुंचाता है।
यह समझ लेने के बाद, यह कहा जा सकता है कि असामंजस्य की यह अवधारणा, यदि गहनता और पर्याप्त प्रमाणों के साथ लागू की जाए तो, हमारी चंद वर्तमान तकलीफों को समझने व उनसे निपटने में काफी उपयोगी व सही हो सकती है। पीटर ग्लकनैन और मार्क हैंसन ने अपनी पुस्तक मिसमैच (2008) में इस पर विचार करते हुए दर्शाया है कि हमारी उद्विकसित जैविकी और हमारे वर्तमान पर्यावरण के बीच असामंजस्य कई कारणों से हो सकता है।
उदाहरण के लिए, आधुनिक पाश्चात्य समाजों में, बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के चलते, मनोवैज्ञानिक व यौनिक परिपक्वता का समय बदला है। ये दोनों परिपक्वताएं अतीत में लगभग साथ-साथ आती थीं लेकिन अब इनकी कड़ी टूट गई है। आजकल बच्चे यौन परिपक्वता जल्दी और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता से पहले हासिल कर लेते हैं। यह मनोवैज्ञानिक परिपक्वता यौन परिपक्वता की मांगों से निपटने लिए ज़रूरी होती है। ऐसा न होने पर आजकल के किशोर कई समस्याओं का सामना करते हैं।
हमारी जैविकी और भोजन, ऊर्जा के उपभोग व खर्च की आधुनिक जीवन शैली के बीच असामंजस्य एक और उदाहरण है। कृषि तथा आधुनिक टेक्नॉलॉजी के प्रादुर्भाव के साथ हमारा भोजन नाटकीय रूप से बदल गया है। वसा, नमक और शकर, जो पहले मुश्किल से मिलते थे, आज प्रचुर मात्रा में और नियमित रूप से उपलब्ध हो गए हैं। यह तो कृषि व टेक्नॉलॉजी में तरक्की के फलस्वरूप हुआ है। इसके अलावा, मार्केटिंग की रणनीतियों व व्यापारिक हितों के चलते लोगों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग को प्रेरित किया जाता है और इसने समस्या को और विकट बनाया है। कुल मिलाकर इनका परिणाम तथाकथित जीवन शैली रोगों के रूप में सामने आया है – टाइप-2 मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय-रक्तसंचार सम्बंधी बीमारियां।
लेकिन भोजन और स्वास्थ्य के बीच सम्बंध बहुत स्पष्ट नहीं हैं। लाल मांस, अंडे, वसाएं और शकर के उपभोग को लेकर दी गई सिफारिशों में उलटफेर काफी जानी-पहचाने हैं। ऐसे उलटफेर के चलते अक्सर विज्ञान के प्रति विश्वास कम हो जाता है – आम लोगों में भी और अन्य विषयों के वैज्ञानिकों में भी। तथ्य यह है कि ये कड़ियां निहायत पेचीदा हैं तथा और अनुसंधान की ज़रूरत है, खास तौर से वैकासिक नज़रिए को ध्यान में रखते हुए।
दरअसल, चूंकि विभिन्न खाद्य पदार्थों के उपयोग के पक्ष और विपक्ष में की गई सिफारिशों पर काफी सशक्त व्यावसायिक हित हावी होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति और उसका मूल्यांकन दांव पर लगा है। नेचर पत्रिका में एक हालिया संपादकीय (शीर्षक ‘स्टडीज़ लिंकिंग डाएट विद हेल्थ मस्ट गेट एक होल लॉट बेटर’) में इस बात को रेखांकित किया गया है कि “अधिकांश पोषण सम्बंधी और स्वास्थ्य सम्बंधी सलाहों के पीछे प्रमाणों का आधार…. विवादित है।” संपादकीय में चेतावनी दी गई थी:
“यदि वित्तदाता अपने प्रयासों को अच्छी गुणवत्ता के आंकड़े उत्पन्न करने में नहीं लगाएंगे, तो आम लोग भ्रमित, शंकालु, अनाश्वस्त रहेंगे और उस जानकारी से वंचित रहेंगे जिसकी ज़रूरत स्वास्थ्य व जीवन शैली सम्बंधी निर्णयों के लिए है।”
एक और असामंजस्य होता है क्योंकि लोगों की प्रजनन-काल के बाद की जीवन अवधि लंबी होती जा रही है जिसकी वजह से बढ़ती उम्र की तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं – स्मृतिभ्रंश, पार्किंसन व अल्ज़ाइमर रोग और मेनोपॉज़ से जुड़ी दिक्कतें। हम इनके प्रति अनुकूलित नहीं हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत नई हैं क्योंकि बुढ़ापा स्वयं ही अब पहले की तुलना में ज़्यादा सामान्य बात हो गई है।
और तो और, चूंकि ये बीमारियां बढ़ती उम्र में होती हैं, इसलिए प्राकृतिक वरण की प्रक्रिया इनके विरुद्ध चयन भी नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारी प्रजनन सफलता को प्रभावित नहीं करतीं। इस संदर्भ में एक वैकासिक नज़रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
जैसा कि हमने पहले कहा था, असामंजस्य के कई मामले इसलिए उभरते हैं क्योंकि प्राकृतिक वरण हमारी आधुनिक सभ्यता के साथ कदम नहीं मिला पाया है। विडंबना देखिए कि जिस प्राकृतिक वरण ने हमारे बड़े दिमागों को उत्पन्न किया और हमें भाषा की कुशलता प्रदान की और तदानुसार संस्कृति के विकास को संभव बनाया, उसी ने हमें खुद प्राकृतिक वरण की शक्ति से बच निकलने की गुंजाइश भी दी है। स्वाभाविक सवाल है कि क्या वह कभी कदम मिला पाएगा। सिद्धांतत: तो जवाब ‘हां’ लगता है लेकिन व्यावहारिक तौर पर लगता है कि ‘शायद नहीं’ या ‘कभी-कभार ही’।
दूध की अच्छाई?
हमारी जैविकी और पर्यावरण के बीच सभ्यता-प्रेरित असामंजस्य के जिस उदाहरण का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है, और जहां दोनों के बीच की खाई अंतत: पट जाएगी, वह है लैक्टोस सहनशीलता/असहनशीलता का। चूंकि सारे स्तनधारी जीव अपने शिशुओं को स्तनपान कराते हैं, इसलिए शिशुओं में लैक्टेज़ नामक एक एंज़ाइम पाया जाता है, जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोस शर्करा को पचाता है।
जब शिशुओं को दूध छुड़ाकर अन्य भोजन दिया जाने लगता है, तब वे लैक्टेज़ बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं होती। मनुष्यों में भी ऐसा ही होता है। इसलिए वयस्कों को ‘लैक्टेज़ नॉन-पर्सिस्टेंट’ अर्थात ‘लैक्टोस-असहनशील’ कहा जाता है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में पशुपालन के प्रादुर्भाव के साथ यह काफी फायदेमंद हो गया कि वयस्क आहार में पशुओं के दूध को जगह दी जाए।
इस बात के काफी पुख्ता प्रमाण हैं कि प्राकृतिक वरण ने उन बिरले उत्परिवर्तनों को वरीयता दी जो किसी व्यक्ति को लैक्टेज़ नामक एंज़ाइम वयस्कपन में भी बनाते रहने की क्षमता देते थे। ये लोग ‘लैक्टेज़ पर्सिस्टेंट’ और ‘लैक्टोस सहनशील’ हो गए। इस बात के भी प्रमाण हैं कि दुनिया के अलग-अलग इलाकों उत्परिवर्तन अलग-अलग हैं। आज युरोप के कई हिस्सों तथा अफ्रीका व मध्य-पूर्व के कुछ इलाकों में ‘लैक्टेज़ पर्सिस्टेंट’ और ‘लैक्टोस सहनशीलता’ काफी आम है।
अलबत्ता, इसकी उपस्थिति में काफी विविधता है – स्कैंडिनेविया में 95-97 प्रतिशत, जहां दूध का सेवन सामान्य बात है, से लेकर पूर्वी एशिया में 0-10 प्रतिशत जहां दूध का सेवन काफी कम होता है।
कुल मिलाकर, लैक्टोस असहनशीलता दुनिया में सबसे आम स्थिति है। और वास्तव में यह मनुष्यों की प्राचीन स्थिति है। लेकिन वैकासिक नज़रिए के अभाव में और जाने-पहचाने पाश्चात्य पूर्वाग्रह के चलते, हम अक्सर सोचते हैं कि ‘लैक्टोस असहनशीलता’ एक बीमारी है।
वैकासिक परिप्रेक्ष्य हमें एक सर्वथा अलग तस्वीर प्रदान करता है। लैक्टोस असहनशीलता की प्राचीन स्थिति, जब दूध का सेवन नदारद था, से लेकर वर्तमान तक, जब कम से कम कुछ इलाकों में दूध का सेवन सामान्य बात है, लैक्टोस सहनशीलता का विकास हुआ है और इसने जैविकी और संस्कृति के बीच असामंजस्य को पलट दिया है। यह अपेक्षा उचित ही होगी कि यदि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दूध का सेवन बढ़ता गया तो लैक्टोस सहनशीलता विकसित होती जाएगी। लेकिन प्राकृतिक वरण एक धीमी प्रक्रिया है और ऐसे असामंजस्य सैकड़ों-हज़ारों सालों तक बने रहने की अपेक्षा की जानी चाहिए।
जीन्स का दोष
हमारे शरीर के कई गुणों की तरह हमारी कई बीमारियों का दोष भी जीन्स को दिया जा सकता है। लेकिन यह सहजबोध के थोड़ा उल्टा लगता है क्योंकि ऐसे जीन्स का सफाया करना ही तो प्राकृतिक वरण का काम है। दिक्कत यह है कि प्राकृतिक वरण कई बार ऐसा करने में अशक्त होता है। उदाहरण के लिए, वह कुछ ऐसे खराब जीन्स को नहीं हटा सकता जिनके कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं।
ऐसा सबसे बेहतरीन उदाहरण है वह जीन जो सिकल सेल एनीमिया का कारण है। यह जीन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में काफी आम है। यह एक असामान्य हीमोग्लोबीन का निर्माण करता है जिसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाएं विकृत हो जाती हैं और हंसिए की आकृति ग्रहण कर लेती हैं। ऐसी हंसियाकार कोशिकाएं रक्त के साथ आसानी से प्रवाहित नहीं हो पातीं, जिसकी वजह से रक्तस्राव, एनीमिया और कई अन्य दिक्कतें होती हैं।
जिन व्यक्तियों में दोषपूर्ण जीन की दो प्रतियां (माता और पिता दोनों से प्राप्त) होती हैं, उनमें सारी लाल रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति गंभीर रोगग्रस्त होते हैं (इन्हें उस जीन के लिहाज़ से होमोज़ायगस कहा जाता है)। ऐसे व्यक्ति अक्सर प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व होने से पहले ही मौत के शिकार हो जाते हैं। यदि कहानी सिर्फ इतनी होती तो प्राकृतिक वरण शायद पूरी आबादी से सिकल सेल जीन का सफाया कर चुका होता। लेकिन कहानी में एक पेंच है।
जिन लोगों को किसी एक पालक से दोषपूर्ण जीन विरासत में मिलता है और दूसरे पालक से सामान्य जीन मिलता है वे हेटेरोज़ायगस होते हैं; उनमें एक जीन दोषपूर्ण और एक जीन सामान्य होता है। ऐसे व्यक्तियों में सामान्य जीन सामान्य हीमोग्लोबीन और सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। और उनका काम इन सामान्य कोशिकाओं से चल जाता है। दोषपूर्ण जीन द्वारा बनाई गई असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं को रक्त प्रवाह से हटा दिया जाता है। लिहाज़ा, शरीर में रोग के लक्षण प्रकट होने के लिए दोनों सिकल कोशिका जीन्स दोषपूर्ण होने चाहिए। ऐसे जीन्स को रेसेसिव कहा जाता है।
किसी रेसेसिव घातक जीन का सफाया करना प्राकृतिक वरण के लिए काफी मुश्किल होता है क्योंकि हेटेरोज़ायगस व्यक्तियों में ये जीन प्राकृतिक वरण के लिए ओझल होते हैं और दोषपूर्ण होने के बावजूद ये व्यक्ति जीवित रह पाते हैं और उस जीन को अगली पीढ़ी में प्रेषित कर देते हैं। यदि किसी आबादी में वह जीन काफी कम पाया जाता है, तो संभावना यह होती है कि उस जीन वाले अधिकांश लोग हेटेरोज़ायगस होंगे और प्राकृतिक वरण कम प्रभावी रह जाएगा। इसलिए, रेसेसिव घातक जीन्स किसी आबादी में कम संख्या में लंबे समय तक बने रह सकते हैं।
अब ज़रा कल्पना कीजिए कि हेटेरोज़ायगस लोग वास्तव में सामान्य जीन के होमोज़ायगस लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या यह संभव है? अवश्य संभव है, और कई मामलों में ऐसा होता भी है। उदाहरण के लिए, सिकल कोशिका जीन को ही लीजिए।
यह तो हम देख ही चुके हैं कि हेटेरोज़ायगस व्यक्ति दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाओं को हटाकर काम चला लेते हैं। इसके चलते मलेरिया परजीवी (प्लाज़्मोडियम फाल्सिपैरम) के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है क्योंकि जिन कोशिकाओं में परजीवी बैठा होता है, उन्हें प्राय: हटा दिया जाता है। अर्थात सिकल कोशिका जीन के संदर्भ में हेटेरोज़ायगस व्यक्तियों को मलेरिया से मृत्यु के खिलाफ काफी सुरक्षा मिल जाती है।
तो, हेटेरोज़ायगस व्यक्ति के शरीर में सिकल कोशिका के जीन को न सिर्फ सुरक्षा मिलती है बल्कि प्राकृतिक वरण द्वारा चुना भी जाता है। जैसी कि अपेक्षा होगी, सिकल कोशिका जीन उन इलाकों में ज़्यादा आम होता है जो मलेरिया ग्रस्त हैं चाहे उस जीन के होमोज़ायगस व्यक्ति सिकल कोशिका रोग से पीड़ित होते रहें। यह एक ऐसी स्थिति है जहां जब तक मलेरिया का प्रकोप बना हुआ है, प्राकृतिक वरण मरम्मत करने में अक्षम रहता है।
शरीर में लेन–देन
जीवों को उनके पर्यावरण के अनुकूल बनाने में प्राकृतिक वरण के मार्ग में अड़चन का एक कारण और भी है। हमारे शरीर को दोषरहित बनाने के मार्ग में प्राय: यह अड़चन आती है कि उस अनुकूलन को अपनाने का असर किसी अन्य गुणधर्म पर पड़ता है। दोनों हाथों में लड्डू मुश्किल है। विलियम्स और नेसे कहते हैं,
“सीधे खड़े होकर चलने की कीमत पीठ-दर्द की समस्याएं हैं। ऊतकों की मरम्मत करने की क्षमता की कीमत कैंसर के रूप में सामने आती है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की कीमत प्रतिरक्षा विकारों के रूप में दिखती है। दुश्चिंता की कीमत पैनिक डिसऑर्डर होती है। प्रत्येक मामले में, प्राकृतिक वरण ने यथासंभव सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है – लाभों को लागतों के साथ संतुलित करके। जहां भी संतुलन बिंदु होगा, बीमारी अवश्यंभावी है।
अनुकूलनवादी वैज्ञानिक शरीर को एक दोषमुक्त पर्फेक्ट रचना के रूप में नहीं बल्कि समझौतों के एक पुंज के रूप में देखते हैं। उन्हें समझकर हम बीमारियों को बेहतर समझ पाएंगे।”
आगामी लेखों में हम ऐसे समझौतों का और अन्वेषण करेंगे और खास तौर से यह देखेंगे कि ये यौवन और बुढ़ापे के बीच तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच किस तरह सामने आते हैं।
सार रूप में, हमारे शरीर कमज़ोर और दोषपूर्ण हैं और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि प्राकृतिक वरण ने कतिपय ऐतिहासिक मार्ग अपनाए होंगे, क्योंकि प्राकृतिक वरण रोगजनक जीवों के पक्ष में भी काम करता है, क्योंकि हमारी जैविकी और हमारी संस्कृति के बीच असामंजस्य है, क्योंकि बुरे जीन्स के कुछ अच्छे असर भी हो सकते हैं और प्राय: लाभ-लागत के बीच ऐसे लेन-देन होते हैं कि कई सारे कार्यों को एक साथ पर्फेक्ट बनाने की प्राकृतिक वरण की क्षमता बाधित होती है।
किसी वैकासिक जीव वैज्ञानिक के लिए यह रोमांचक बुनियादी विज्ञान है जो सौंदर्य और तर्क से लबरेज़ है। साथ ही, वैकासिक चिकित्सा का वायदा है कि यदि हम स्वास्थ्य व बीमारियों को एक वैकासिक नज़रिए से समझने की कोशिश करें, तो इससे चिकित्सा विज्ञान समृद्ध होगा।
अगले लेख में हम वैकासिक चिकित्सा की वर्तमान स्थिति – नेसे व विलियम्स की पुस्तक के प्रकाशन के 30-35 साल बाद – पर विचार करेंगे।(स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://cdn.thewire.in/wp-content/uploads/2022/11/28200347/Image-1-PSM_V57_D097_Hms_beagle_in_the_straits_of_magellan-1536×991.png