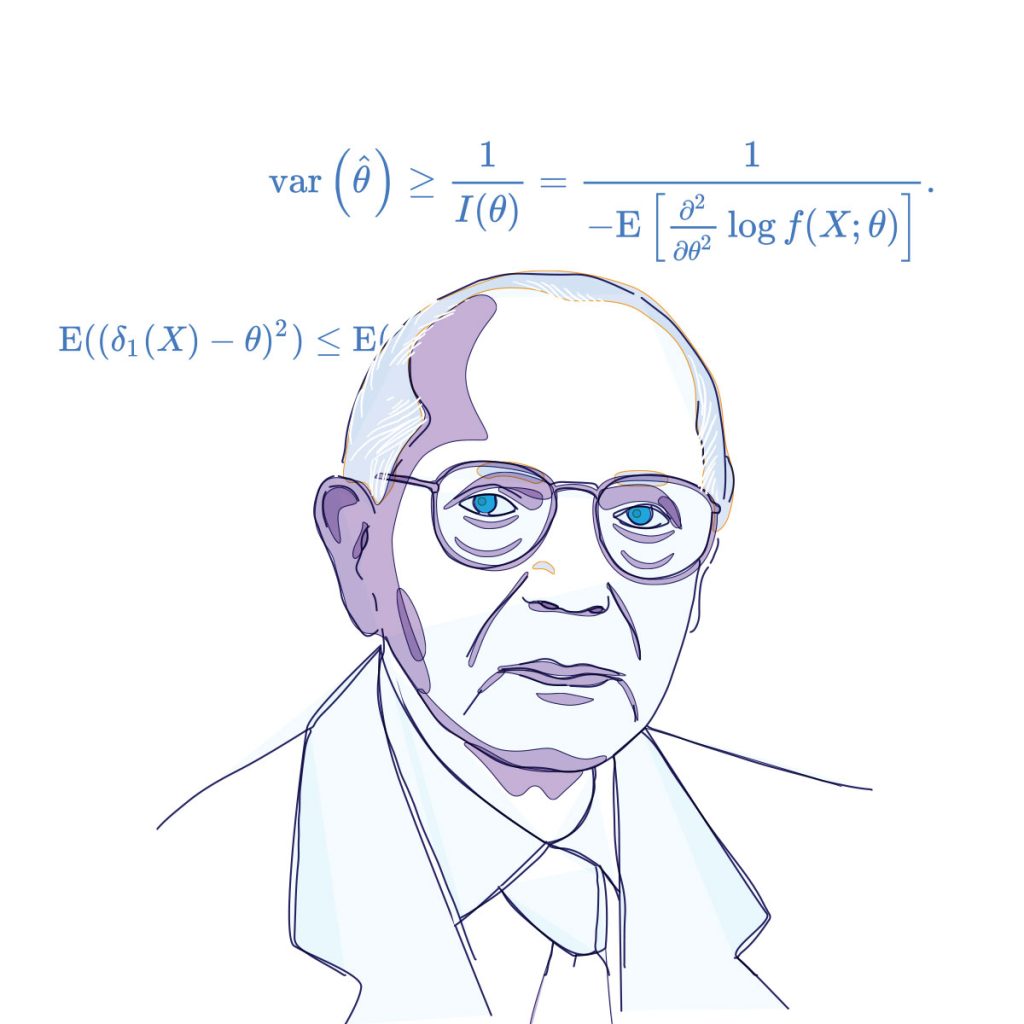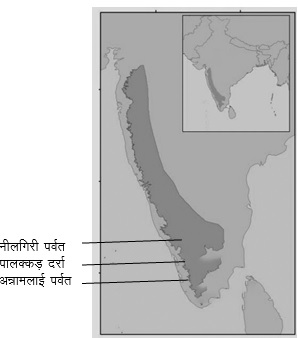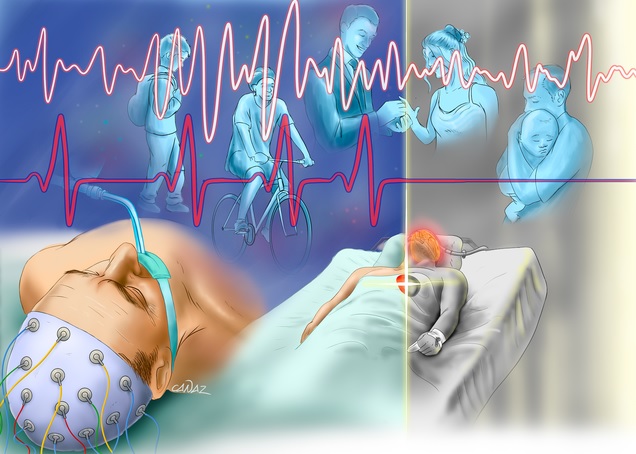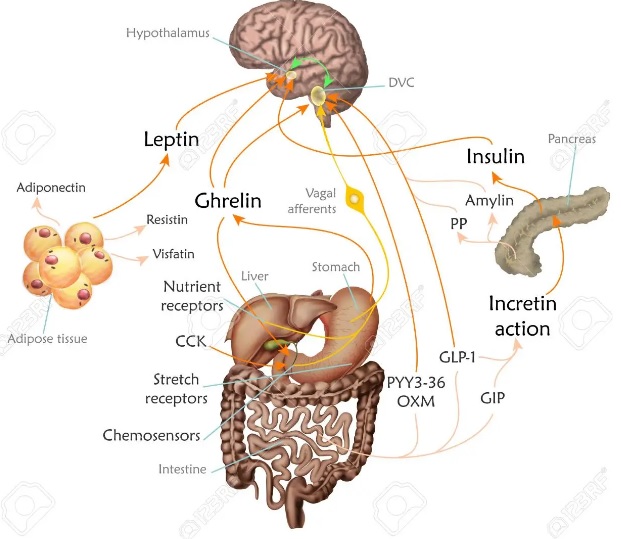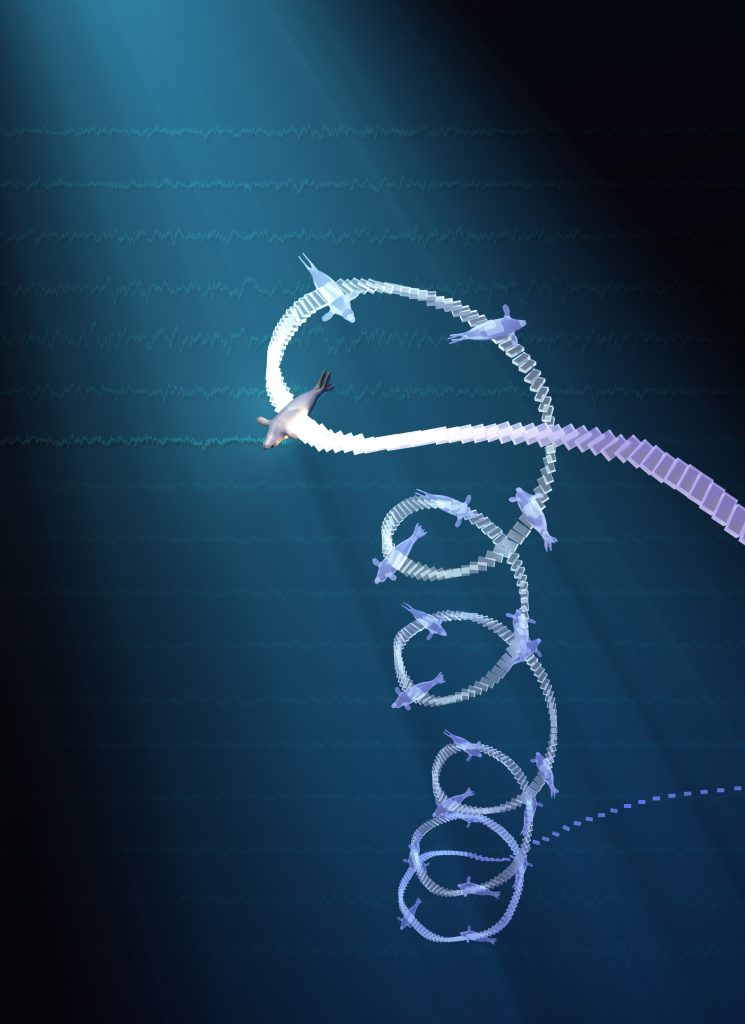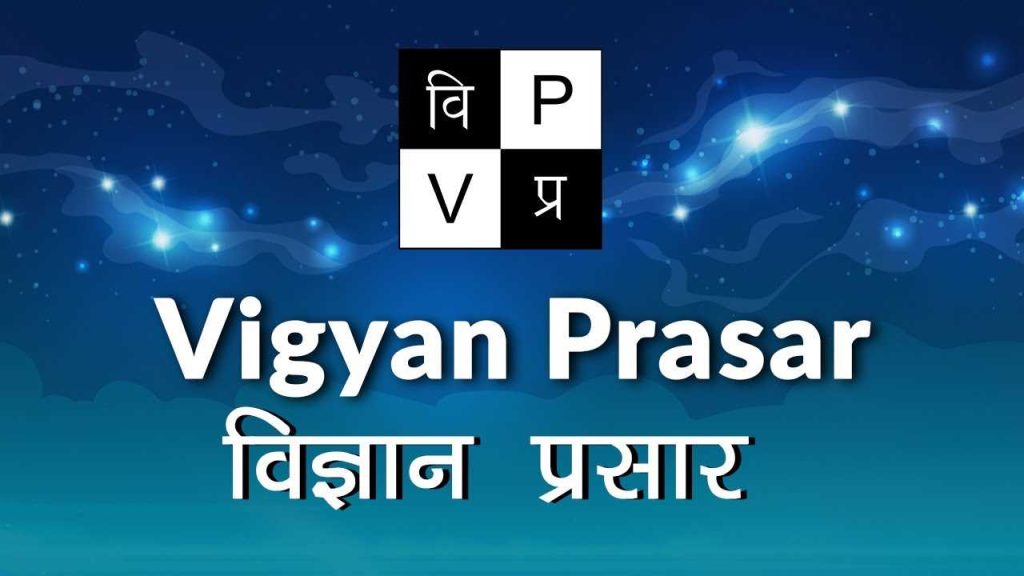
पूरे देश में संचार के प्रमुख माध्यमों और विभिन्न विधाओं के ज़रिए आम आदमी तक विज्ञान की उपलब्धियों को पहुंचाने और वैज्ञानिक जागरूकता के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अक्टूबर 1989 में ‘विज्ञान प्रसार’ नामक एक स्वायत्त संस्था स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना के 33 वर्षों बाद नीति आयोग ने इसे बंद करने की सिफारिश की है।
आज़ादी के 75 सालों बाद जब विज्ञान संचार की गतिविधियों के विस्तार और सशक्तीकरण का अवसर आया है, तब इस तरह के चौंकाने वाले प्रस्ताव ने विचार मंथन और नीति आयोग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है।
इस संस्था ने आम आदमी, संचार माध्यमों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को जोड़ने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। विज्ञान की लोकप्रिय किताबों से लेकर पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो, विज्ञान क्लबों, फिल्मों, हैम रेडियो, एडुसेट उपग्रह तक के माध्यम से विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया है। हाल के वर्षों को छोड़कर ‘विज्ञान प्रसार’ की शानदार उपलब्धियों और गतिविधियों से सराबोर अतीत की सम्यक समीक्षा और विश्लेषण करें तो कहा जा सकता है कि नीति आयोग का निर्णय अनावश्यक और पूर्वाग्रहों से प्रेरित है।
दरअसल, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 1982 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की थी। एनसीएसटीसी की स्थापना के सात वर्षों बाद 1989 में ‘विज्ञान प्रसार’ का जन्म हुआ। डीएसटी ने विज्ञान प्रसार को स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान करते हुए व्यापक स्तर पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का कार्य सौंपा था।
एनसीएसटीसी ने अपनी स्थापना के साथ ही विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू किए। इनमें टीवी सीरियल ‘भारत की छाप’ और ‘क्यों और कैसे’ कार्यक्रम शामिल हैं। रेडियो के ज़रिए विज्ञान को श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ‘मानव का विकास’ नामक धारावाहिक बनाया गया था। यह विश्व का सबसे लंबा विज्ञान रेडियो धारावाहिक है।
एनसीएसटीसी ने ‘भारत जन विज्ञान जत्था’ का आयोजन किया। यह अपने ढंग का अनोखा आयोजन था, जिसमें ग्रामीण लोगों को विज्ञान और वैज्ञानिकों से सीधे संपर्क में आने का मौका मिला था। एनसीएसटीसी न्यूज़लेटर शीर्षक से मासिक प्रकाशन किया गया, जिसमें एनसीएसटीसी की गतिविधियां, भेंटवार्ताएं और पाठकों की प्रतिक्रियाएं होती थीं। किताबों में कहानी माप तौल की, गाएं गाना, खेलें खेल, हॉर्नबिल सीरीज़ आदि हैं।
आरंभ में एनसीएसटीसी और विज्ञान प्रसार ने कंधे से कंधा मिलाकर कुछ गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिनमें 1995 में ‘पूर्ण सूर्यग्रहण’ के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम विज्ञान संचार के इतिहास में अहम और उल्लेखनीय था। इस कार्यक्रम में एनसीएसटीसी ने संकल्पना में और विज्ञान प्रसार ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर के विकास में योगदान किया था।
वास्तव में, एनसीएसटीसी ने अपनी स्थापना के शुरुआती दौर में जहां सरकारी ढांचे की सीमाओं के भीतर योगदान दिया, वहीं विज्ञान प्रसार ने स्वायत्त संस्थान की आज़ादी का लाभ उठाते हुए नवीन कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू कीं और पहली बार देश में आम लोगों के लिए विज्ञान संचार की ज़रूरत और महत्व को उजागर किया। विज्ञान प्रसार के विस्तार के बाद एनसीएसटीसी के कार्यों का दायरा देश भर की विज्ञान संस्थाओं की परियोजनाओं के वित्त पोषण, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के सालाना आयोजन और विज्ञान संचार के राष्ट्रीय पुरस्कार तक सिमट कर रह गया है।
विज्ञान प्रसार के विज्ञान संचार कार्यक्रमों को मोटे तौर पर दस भागों में विभाजित किया जा सकता है – प्रकाशन, टेलीविज़न, रेडियो, विपनेट क्लब, खगोल विज्ञान, लिंग समानता एवं प्रौद्योगिकी संचार, हैम रेडियो, गतिविधि किट, फिल्मों के द्वारा विज्ञान और एडुसैट नेटवर्क।
विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक लगभग 400 किताबें प्रकाशित की गई हैं। ये पुस्तकें विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत हिन्दी और अंग्रेज़ी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला आदि विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं।
ड्रीम 2047 विज्ञान प्रसार की लोकप्रिय मासिक विज्ञान पत्रिका है। इसका प्रकाशन अक्टूबर 1998 में आरंभ हुआ था। इस द्विभाषी पत्रिका का प्रकाशन अनवरत जारी है। विख्यात और वरिष्ठ पत्रकार एवं मुंबई से प्रकाशित फ्री प्रेस जर्नल में लंबे समय तक नियमित स्तम्भकार रहे पद्मभूषण एम. वी. कामथ ने ड्रीम 2047 के सौवें अंक में प्रकाशित आलेख में इस पत्रिका को अनूठी विज्ञान पत्रिका बताया है। ड्रीम 2047 पत्रिका का इलेक्ट्राॅनिक संस्करण विज्ञान प्रसार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
विज्ञान प्रसार विपनेट न्यूज़ प्रकाशित कर रहा है। इस मासिक पत्र में खगोल विज्ञान, जैव विविधता, प्रकृति, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों से सम्बंधित आलेख होते हैं। यह पत्रिका विज्ञान क्लब के सदस्यों के बीच संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है।
विज्ञान प्रसार द्वारा भारतीय भाषाओं में विज्ञान संचार, लोकप्रियकरण एवं विस्तार (स्कोप) परियोजना आरंभ करने से देश में विज्ञान संचार को एक नई दिशा मिली है। इसके तहत विभिन्न भाषाओं में वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशित हो रहे हैं। उर्दू में तजस्सुस शीर्षक से मासिक पत्र प्रकाशित हो रहा है। तजस्सुस का अर्थ है उत्सुकता। इसी प्रकार से बांग्ला में विज्ञान कथा का प्रकाशन जारी है। तमिल में अरिवियल पलागाई मासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है।
विज्ञान प्रसार ने भारत में टेलीविज़न को लोकप्रिय माध्यम के रूप में देखते हुए इसका उपयोग वैज्ञानिक जागरूकता और प्रसार के लिए करने का निर्णय लिया। इसरो की डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन युनिट (डेकू) के साथ मिलकर विज्ञान सम्बंधी कार्यक्रम बनाए, जिनका विभिन्न भारतीय भाषाओं में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल और क्षेत्रीय केंद्रों से प्रसारण किया गया। साइंस ऑन टेलीविज़न के माध्यम से टेलीविज़न पर विज्ञान कार्यक्रम लोकसभा और राज्यसभा टीवी, क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और ज्ञान दर्शन के माध्यम से प्रसारित होते रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित लगभग 2000 कार्यक्रमों को देश के लाखों दर्शकों ने पसंद किया। इस संस्था का इंटरनेट आधारित ओवर-दी-टॉप (ओटीटी) साइंस चैनल है। यह प्लेटफॉर्म 24X7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान के लिए समर्पित है।
विज्ञान प्रसार ने विभिन्न विषयों और मुद्दों पर मेगा विज्ञान रेडियो धारावाहिकों का निर्माण किया है। इनमें पृथ्वी ग्रह, खगोल विज्ञान, गणित, जैव विविधता, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि सम्मिलित हैं। 19 भाषाओं में निर्मित इन कार्यक्रमों को विभिन्न एफएम केंद्रों के साथ 117 मीडियम वेव केंद्रों से प्रसारित किया गया है।
रेडियो के ज़रिए जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदायों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत जनजातीय भाषाओं में भी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
हैम रेडियो का लोकप्रियकरण विज्ञान प्रसार की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है। हैम रेडियो संचार किसी भी आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण बैकअप के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विज्ञान प्रसार हैम रेडियो स्टेशनों की स्थापना, ऑपरेटरों के प्रशिक्षण और रचनात्मक गतिविधियों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही विश्व भर के शौकिया ऑपरेटरों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी मदद प्रदान करता है। विज्ञान प्रसार स्कूली विद्यार्थियों और प्रौद्योगिकी संस्थानों में हैम रेडियो को बढ़ावा दे रहा है।
विज्ञान प्रसार का एक प्रमुख कार्यक्रम ‘नेशनल साइंस फिल्म फेस्टीवल’ भी है। इस फिल्म फेस्टीवल का उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से विज्ञान की पहुंच का विस्तार और विज्ञान फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देना रहा है। इसमें पूरे देश से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वैज्ञानिक मुद्दों और विषयों पर फिल्में आमंत्रित की जाती हैं। चयनित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है और पुरस्कार दिए जाते हैं।
विज्ञान प्रसार ने देश के दूरदराज़ इलाकों तक पहुंचने के लिए शैक्षणिक उपग्रह ‘एडुसैट’ का उपयोग करके इंटरएक्टिव टर्मिनलों का नेटवर्क बनाया है और देश के विभिन्न हिस्सों में 50 टर्मिनल स्थापित किए हैं। इस तकनीक का उपयोग विज्ञान प्रसार विभिन्न विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रमों के प्रसारण में कर रहा है।
विज्ञान प्रसार ने बीते वर्षों में देश भर में आम लोगों के बीच कई राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाए हैं। इनमें पूर्ण सूर्य ग्रहण 1999, शुक्र पारगमन 2004, विज्ञान रेल: पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी 2003-04, पूर्ण सूर्यग्रहण 2009 आदि सम्मिलित हैं।
विज्ञान प्रसार द्वारा देश में विज्ञान क्लब कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1998 में विज्ञान क्लब के देशव्यापी नेटवर्क ‘विपनेट’ की स्थापना की गई। वर्तमान में विज्ञान प्रसार का लगभग 3000 विज्ञान क्लबों का नेटवर्क है, जिसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियां की जाती रही हैं। वास्तव में विपनेट विज्ञान प्रसार के उद्देश्यों की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाता है। विज्ञान क्लब रोचक और ज्ञानवर्धन गतिविधियों का मंच है, जिसमें मित्रों को भी शामिल किया जा सकता है।
विपनेट देश के हर कोने में अच्छी तरह से जाना जाता है। अपनी स्थापना के दो वर्षों बाद मध्यप्रदेश का रतलाम ज़िला देश का सबसे अधिक सदस्यता (107) वाला ज़िला और उत्तरप्रदेश सबसे अधिक 350 विज्ञान क्लबों वाला राज्य बन गया था।
विज्ञान प्रसार के नेतृत्व में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के 75 स्थानों पर विज्ञान महोत्सवों का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय ‘विज्ञान सर्वत्र पूज्यते’ था। विज्ञान उत्सव के माध्यम से स्थानीय लोगों को वैज्ञानिक विरासत और प्रगति से परिचित कराया गया था। इस दौरान विज्ञान पुस्तक मेला, विज्ञान कवि सम्मेलन, विज्ञान प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
साल 2020 में विज्ञान प्रसार ने कोरोना वायरस से फैली कोविड-19 महामारी के दौरान देश के वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के कार्यों से सबको परिचित कराने के लिए अनूठी कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला पर वृत्तचित्र का निर्माण किया।
विज्ञान प्रसार अनेक वर्षों से खगोल विज्ञान के लोकप्रियकरण में जुटा हुआ है और विद्यार्थियों, अध्यापकों और शौकिया खगोल वैज्ञानिकों के लिए दूरबीन निर्माण सम्बंधी कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है।
विज्ञान को आम लोगों तक ले जाने की मुहिम की एक प्रमुख कड़ी है – ‘इंडिया साइंस वायर प्रोजेक्ट’। विज्ञान प्रसार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के समाचार पत्रों और वेब पोर्टल्स को विज्ञान समाचार और फीचर नियमित रूप से उपलब्ध करा रहा है।
विज्ञान प्रसार ने देश के 17 स्थानों पर ‘गांधी एट 150 प्रोजेक्ट’ शीर्षक से डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया था।
इसने ‘शोध अभिव्यक्ति के लिए लेखन कौशल को प्रोत्साहन’ परियोजना शुरू की, जिसके तहत विज्ञान विषयों में पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टरेट करने वाले व्यक्तियों को फैलोशिप के दौरान अपनी रिसर्च से सम्बंधित मुद्दे पर लोकप्रिय विज्ञान लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय अनुसंधान कार्यों को जन साधारण के बीच रोचक अंदाज़ में प्रस्तुत करना है।
विज्ञान प्रसार ने वर्ष 2018-19 में विद्यार्थी विज्ञान मंथन (वीवीएम) परीक्षा के आयोजन में योगदान किया। डिजिटल उपकरणों की सहायता से आयोजित इस परीक्षा में कक्षा 6-11 के विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी विरासत से परिचित कराना है।
क्रियाकलाप और खिलौना विकास एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। विज्ञान प्रसार ने पिछले एक दशक में लगभग 10 विषयों में विषयगत किट विकसित किए हैं। इनमें जैव विविधता, खगोल विज्ञान, भूकंप, मौसम आदि सम्मिलित हैं।
बीते दशकों के दौरान विज्ञान प्रसार ने महत्वपूर्ण दिवसों के अवसर पर उत्सव समारोह आयोजित किए हैं। इनमें मेघनाद साहा की 125वीं जयंती समारोह, राष्ट्रीय गणित दिवस समारोह, रामानुजन यात्रा आदि शामिल हैं।
कुल मिलाकर नीति आयोग द्वारा विज्ञान प्रसार को बंद करने के निर्णय से भारत में विज्ञान संचार के मैदान में पूरे उत्साह, लगन और समर्पण भाव से जुटे विज्ञान संचारकों को गहरा आघात पहुंचा है। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://secure.brighterkashmir.com//images/news/d25b8647-0937-4490-a056-5ddf19ea794c.jpg