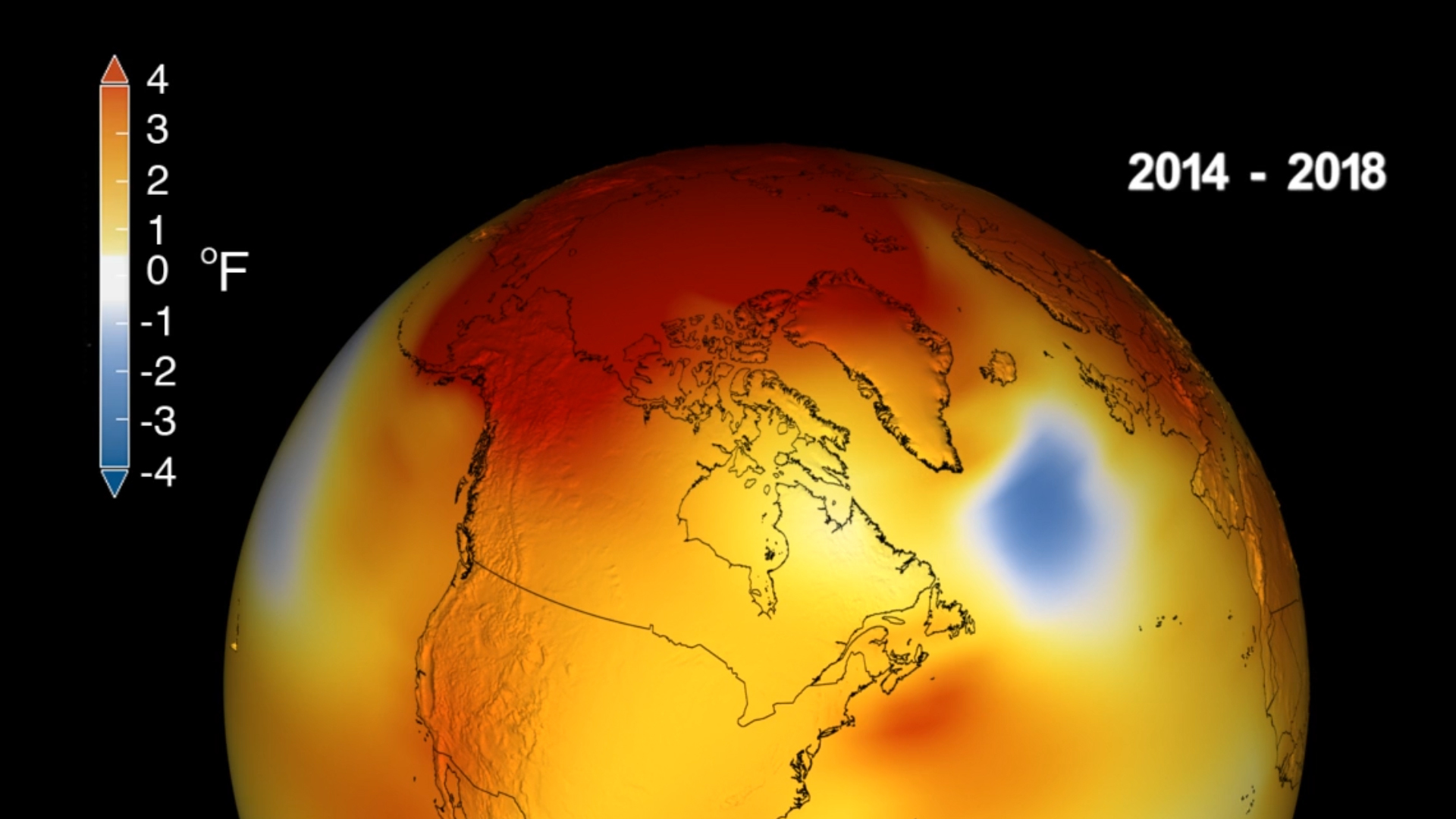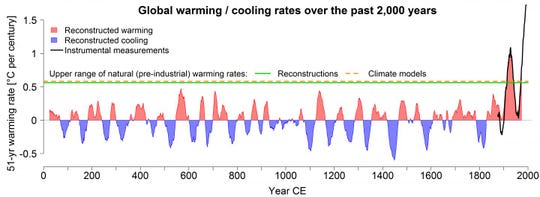लगभग दस हज़ार साल पूर्व, जब से मनुष्यों ने समुदायों में रहना शुरू किया, तब से टीबी (क्षयरोग) हमारे साथ रहा है। पश्चिमी एशिया की तरह भारत में भी लोग प्राचीन काल से ही टीबी के बारे में जानते थे। लगभग 1500 ईसा पूर्व के संस्कृत ग्रंथों में इसके बारे में उल्लेख मिलता है जिनमें इसे शोष कहा गया है। 600 ईसा पूर्व की सुश्रुत संहिता में क्षय रोग के उपचार के लिए मां का दूध, अल्कोहल और आराम की सलाह दी गई है। 900 ईस्वीं के मधुकोश नामक ग्रंथ में इस बीमारी का उल्लेख यक्ष्मा (या क्षय होना) के नाम से है। टीबी के बारे में यह भी जानकारी थी कि मनुष्य से मनुष्य में यह रोग खखार और बलगम के माध्यम से फैलता है (यहां तक कि पशुओं के बलगम से भी यह रोग फैल सकता है)। इसके इलाज के लिए कई औषधि-उपचार आज़माए जाते थे, मगर सफलता बहुत अधिक नहीं मिलती थी।
वर्ष 1882 में जाकर जर्मन सूक्ष्मजीव विज्ञानी रॉबर्ट कॉच ने पता लगाया था कि टीबी रोग मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (एमटीबी) नामक रोगाणु के कारण होता है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कॉच ने टीबी के उपचार के लिए दवा खोजने के भी प्रयास किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूबरक्यूलिन नामक दवा बनी, हालांकि यह टीबी के उपचार में ज़्यादा सफल नहीं रही। उस समय से अब तक टीबी के उपचार के लिए कई दवाएं बाज़ार में आ चुकी हैं, जैसे रिफेम्पिसिन, आइसोनिएज़िड, पायराज़िनेमाइड, और हाल ही में प्रेटोमेनिड और बैडाक्विलिन। भारत सरकार हर साल टीबी के लाखों मरीज़ों के उपचार के लिए इनमें से कई या सभी दवाओं का उपयोग करती है।
अलबत्ता, इलाज से बेहतर है बचाव। प्रतिरक्षा विज्ञान इसी कहावत पर अमल करते हुए हमलावर रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने और बीमारी फैलाने से रोकने का प्रयास करता है। इसी दिशा में वर्ष 1908-1921 के दौरान दो फ्रांसिसी जीवाणु विज्ञानियों अल्बर्ट कामेट और कैमिली ग्यूरिन को एक ऐसा उत्पाद बनाने में सफलता मिली थी जो टीबी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकता था। इसे बैसिलस-कामेट-ग्यूरिन (बीसीजी) नाम दिया गया था। जब बीसीजी को टीके के रूप में शरीर में इंजेक्ट किया गया तो इसने एमटीबी के हमले के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता दी। इस तरह टीबी का पहला टीका बना। आज भी यह टीका दुनिया भर में नवजात शिशुओं और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। हालिया अध्ययन बताते हैं कि टीके से यह सुरक्षा 20 वर्षों तक मिलती रहती है। भारत दशकों से सफलतापूर्वक बीसीजी टीके का उपयोग कर रहा है।
सांस के ज़रिए टीका
अलबत्ता, अब यह पता चला है कि बीसीजी का टीका बच्चों के लिए जितना असरदार है उतना वयस्कों पर प्रभावी नहीं रहता क्योंकि वयस्कों में फेफड़ों की टीबी ज़्यादा होती है जबकि बच्चों में आंत, हड्डियों या मूत्र-मार्ग में ज़्यादा देखी गई है और बीसीजी फेफड़ों की टीबी में कम प्रभावी है। किसी अन्य बीमारी (जैसे एड्स) के होने पर भी टीका प्रभावी नहीं रहता क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। कभी-कभी बीसीजी का टीका देने पर कुछ लोगों को बुखार आ जाता है या इंजेक्शन की जगह पर खुजली होने लगती है; यह भी टीके के उपयोग को असहज बनाता है। इसलिए अब एक वैकल्पिक टीके की ज़रूरत है जो खुद तो टीबी के टीके की तरह काम करे ही, साथ में बीसीजी टीके के लिए बूस्टर (वर्धक) का काम भी करे। और यदि यह टीका इंजेक्शन की बजाय अन्य आसान तरीकों से दिया जा सके तो सोने में सुहागा।
लगभग 50 साल पहले टीकाकरण का एक ऐसा तरीका खोजा गया था जिसमें फेफड़ों में सांस के ज़रिए टीका दिया जाता है। इसे ·ासन मार्ग टीका कहते हैं। फुहार के रूप में टीके का पहला परीक्षण 1951 में इंग्लैंड में मुर्गियों के झुंड पर वायरस के खिलाफ किया गया था। इसके बाद 1968 में बीसीजी का इसी तरह का परीक्षण गिनी पिग और कुछ इंसानों पर किया गया। इसकी मदद से मेक्सिको में 1988-1990 के दौरान स्कूली बच्चों में खसरा के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने में सफलता मिली थी और इसके बाद टीबी के खिलाफ प्रतिरोध हासिल करने में। (अधिक जानकारी के लिए मायकोबैक्टीरियल डिसीज़ में प्रकाशित कॉन्ट्रेरास, अवस्थी, हनीफ और हिक्की द्वारा की गई समीक्षा इन्हेल्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी पढ़ सकते हैं)। अच्छी बात यह है कि इस तरीके से टीकाकरण में सुई की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रशिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती, कचरा कम निकलता है और लागत भी कम होती है।
जब रोगजनक जीव शरीर पर हमला करते हैं तो वे शरीर को भेदते हैं और अपनी संख्या वृद्धि करने के लिए अंदर की सामग्री का उपयोग करते हैं, और तबाही मचाते हैं। मेज़बान शरीर अपने प्रतिरक्षा तंत्र की मदद से इन रोगजनक जीवों के खिलाफ लड़ता है। इसमें तथाकथित बी-कोशिकाएं एंटीबॉडी नामक प्रोटीन संश्लेषित करती हैं जो हमलावर के साथ बंधकर उसे निष्क्रिय कर देता है। और सुरक्षा के इस तरीके को याद भी रखा जाता है ताकि भविष्य में जब यही हमलावर हमला करे तो उससे निपटा जा सके। टीके के कार्य करने का आधार यही है, जो सालों तक काम करता रहता है।
वास्तव में एंटीबॉडी बनाने के लिए पूरे हमलावर जीव की ज़रूरत नहीं होती। बी-कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडी बनाने के लिए हमलावर जीव के अणु का एक हिस्सा (‘कामकाजी अंश’ या एपिटोप, एंटीजन का वह हिस्सा जिससे एंटीबॉडी जुड़ती है) ही पर्याप्त होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की एक और श्रेणी होती है टी-कोशिकाएं, जो बी-कोशिकाओं के साथ मिलकर काम करती हैं। टी-कोशकाओं में मौजूद अणु हमलावर को मारने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में भी पूरे अणु की ज़रूरत नहीं होती बल्कि मात्र उस हिस्से की ज़रूरत होती है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए सहायक के रूप में काम करता है।
ऑस्ट्रेलिया की युनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोधकर्ताओं के दल ने इन तीनों सिद्धांतों की मदद से सांस के द्वारा दिया जा सकने वाला टीबी का टीका तैयार किया है। उनका यह शोधकार्य जर्नल ऑफ केमिस्ट्री के 16 अगस्त 2019 अंक में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने टी-कोशिकाओं के अणु के एक हिस्से को सहायक के रूप में प्रयोगशाला में संश्लेषित किया और फिर इसे प्रयोगशाला में ही संश्लेषित किए गए एमटीबी के एपिटोप वाले हिस्से से जोड़ दिया। इस तरह संश्लेषित किए गए टीके (जिसे कंपाउंड I कहा गया) को चूहों में नाक से दिया गया। और इसके बाद चूहों को एमटीबी से संक्रमित किया गया और कुछ हफ्तों बाद चूहों के फेफड़े और तिल्ली को जांचा गया। जांच में बैक्टीरिया काफी कम संख्या में पाए गए जो यह दर्शाता है कि सांस के ज़रिए दिए जाने पर I एक टीके की तरह सुरक्षा दे सकता है। और तो और, इंजेक्शन की बजाय सांस के ज़रिए टीका देना बेहतर पाया गया है। इस तरह के टीके से बच्चे और टीके से घबराने वाले वयस्क खुश हो जाएंगे। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://dlg7f0e93aole.cloudfront.net/wp-content/uploads/shutterstock_186335381-1-750×500.jpg