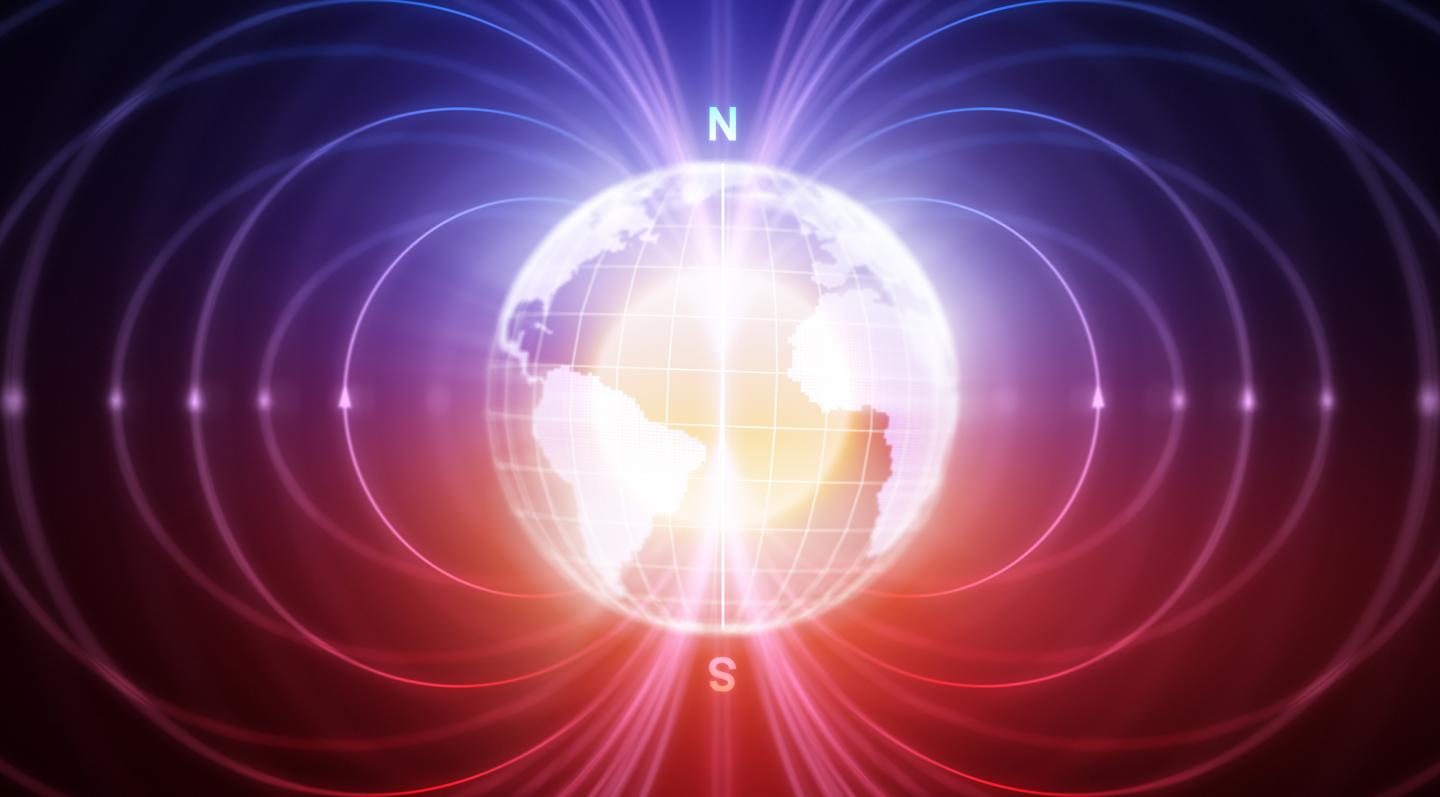जीव-जन्तु विभिन्न प्रकार के प्राकृतवासों में रहते हैं। इन्हीं में से एक है वेटलैंड यानी नमभूमि। सामान्य भाषा में वेटलैंड ताल, झील, पोखर, जलाशय, दलदल आदि के नाम से जाने जाते हैं। सामान्यतया वर्षा ऋतु में ये पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाते हैं। वेटलैंड्स का जलस्तर परिवर्तित होता रहता है। कई वेटलैंड वर्ष भर जल प्लावित रहते हैं जबकि कई ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं।
वेटलैंड एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है तथा जैव विविधता का महत्वपूर्ण अंग है। ज़मीन व जल क्षेत्र का मिलन स्थल होने के कारण वेटलैंड समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र होता है। वेटलैंड न केवल जल भंडारण का कार्य करते हैं, अपितु बाढ़ की विभीषिका कम करते हैं और पर्यावरण संतुलन में सहायक हैं।
वेटलैंड्स को जैविक सुपर मार्केट कहा जाता है। इनमें विस्तृत खाद्य जाल पाया जाता है। इन्हें धरती के गुर्दे भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल को शुद्ध करते हैं। ये मछली, खाद्य वनस्पति, लकड़ी, छप्पर बनाने व ईंधन के रूप में उपयोगी वनस्पति एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वेटलैंड्स असंख्य लोगों को भोजन (मछली व चावल) प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेटलैंड्स कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ये पक्षियों और जानवरों, देशज पौधों और कीटों को आवास उपलब्ध कराते हैं।
भारत के अधिकांश वेटलैंड्स गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती जैसी प्रमुख नदी तंत्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे हुए हैं। एशियन वेटलैंड्स कोश के अनुसार वेटलैंड्स का देश के क्षेत्रफल (नदियों को छोड़कर) में 18.4 प्रतिशत हिस्सा है, जिसके 70 प्रतिशत भाग में धान की खेती होती है। भारत में वेटलैंड्स का अनुमानित क्षेत्रफल 41 लाख हैक्टर है, जिसमें 15 लाख हैक्टर प्राकृतिक और 26 लाख हैक्टर मानव निर्मित है। तटीय वेटलैंड्स का क्षेत्रफल 6750 वर्ग किलोमीटर है और यहां मुख्यत: मैंग्रोव पाए जाते हैं।
वर्तमान में प्रदूषण और औद्योगीकरण के कारण वेटलैंड्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आजकल वेटलैंड्स के किनारे कूड़ा डम्प किया जा रहा है जिसके कारण ये प्रदूषित हो रहे हैं। कई जगहों पर वेटलैंड्स को पाटकर उन पर कांक्रीट के जंगल उगाए जा रहे हैं। वेटलैंड्स के संकटग्रस्त होने के कारण वहां रहने वाले पशु, पक्षी एवं वनस्पतियों का अस्तित्व भी संकट में है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला दलदली हिरण कम हो रहा है। इसी प्रकार तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली फिशिंग कैट पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जंगली गधा भी खतरे में है। असम के काजीरंगा का एक सींग वाला भारतीय गैंडा भी संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणी में शामिल है। इसी प्रकार ओटर, गंगा डॉल्फिन, डूगोंग, एशियाई जलीय भैंस जैसे वेटलैंड से जुड़े अनेक जीव खतरे में हैं।
वेटलैंड संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास में ‘रामसर संधि’ प्रमुख है। यह एक अन्तर-सरकारी संधि है, जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 1971 में देशों ने ईरान के रामसर में विश्व के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस दिन ‘विश्व वेटलैंड्स दिवस’ का आयोजन किया जाता है।
वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में 2200 से अधिक वेटलैंड्स हैं, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है । रामसर कन्वेंशन में शामिल होने वाले देश वेटलैंड्स को पहुंची हानि और उनके स्तर में आई गिरावट को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
वेटलैंड्स संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। 1986 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अन्तर्गत संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई थी।
वर्ष 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड्स के संरक्षण से सम्बंधित नए नियम अधिसूचित किए गए थे। नए नियमों में वेटलैंड्स प्रबंधन के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि क्षेत्रीय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राज्य अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकें।
उल्लेखनीय है कि देश में मौजूद 26 वेटलैंड्स को ही संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसे हज़ारों वेटलैंड्स हैं जो जैविक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
वेटलैंड परितंत्र के अदृश्य अर्थतंत्र का आकलन करने वाली संस्था ‘दी इकॉनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी सर्विसेज़’ के अनुसार समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए वेटलैंड जीवनरेखा है। वेटलैंड्स की सेवाओं को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
(क) जीवन-यापन के रुाोत उपलब्ध कराना ताकि इन क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब लोगों को कमाई का अवसर मिल सके। वेटलैंड से शुद्ध पेयजल, भोजन, रेशे, र्इंधन, जेनेटिक संसाधन, जैव रसायन, प्राकृतिक औषधियां आदि प्राप्त होते हैं।
(ख) स्थानीय जलवायु विनियमन, ग्रीनहाउस गैसों के नियंत्रण हेतु एक वृहद कार्बन सिंक, जलीय चक्र को रेगुलेट करना और भूमिगत जल के स्तर को नियंत्रित करना भी वेटलैंड के लाभ के अन्तर्गत आता है। आपदा जोखिम को कम करना, खासकर बाढ़ और आंधी से बचाव। मृदा सृजन और मृदा अपरदन का नियंत्रण, सतही और भूमिगत जल में उपस्थित जैव रसायन और आर्सेनिक, लेड, आयरन, फ्लोरीन आदि का उपचार। वेटलैंड्स जल का शुद्धिकरण करते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाने में भूमिका निभाते हैं।
(ग) वेटलैंड्स सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था का केंद्र माने जाते हैं। ग्रामीण अंचल में लोग इनकी पूजा करते हैं। आजकल वेटलैंड्स को इकोटूरिज़्म के विशेष केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। इकोटूरिज़्म के साथ-साथ शिक्षा और वैज्ञानिक-शोध के केंद्र के तौर पर भी इन्हें विकसित किया जा रहा है।
(घ) वेटलैंड्स को जैव विविधता का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये शीतकालीन पक्षियों और विभिन्न जीव-जन्तुओं का आश्रय स्थल होते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियों और जन्तुओं के प्रजनन के लिए भी ये उपयुक्त होते हैं।
वेटलैंड्स से हमारा जीवन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वेटलैंड्स बचाए बगैर न तो वैश्विक तापमान में वृद्धि रोकी जा सकती है और न ही जलवायु परिवर्तन की मार से बचा जा सकता है। अत: अपने स्वार्थ के लिए सही, अब ज़रूरी हो गया है कि वेटलैंड्स को बचाएं। (स्रोत फीचर्स)
भारत के प्रमुख वेटलैंड्स
भितरकनिका (उड़ीसा), चिलिका (उड़ीसा), भोज ताल (मध्य प्रदेश), चंद्रताल (हिमाचल प्रदेश), पोंग बांध झील (हिमाचल प्रदेश), रेणुका नमभूमि (हिमाचल प्रदेश), डिपोल बिल (असम), पूर्वी कोलकाता नमभूमि (पश्चिम बंगाल), हरिका झील (पंजाब), कंजली (पंजाब), रोपर (पंजाब), सांभर झील (राजस्थान), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), कौलुरू झील (आंध्र प्रदेश), लोकटक झील (मणिपुर), नलसरोवर पक्षी अभयारण्य (गुजरात), पाइंट कैलियर पक्षी विहार (तमिलनाडु), रूद्रसागर झील (त्रिपुरा), ऊपरी गंगा नदी (उत्तर प्रदेश), अष्टमुडी (केरल), वायनाड-कोल नमभूमि (केरल), साथामुकोटा झील (केरल), सौमित्री (जम्मू एवं कश्मीर), सुरिनसर-मान्सर झील (जम्मू एवं कश्मीर), होकेरा (जम्मू एवं कश्मीर) तथा वूलर झील (जम्मू एवं कश्मीर)।
प्रमुख जीव-जन्तु और वनस्पतियां
गैंडा, हिस्पिड हेअर (खरगोश), हिरण, ऊदबिलाव, गंगा डॉल्फिन, बारहसिंघा, बंगाल फ्लोरिकन, सारस, ककेर, घड़ियाल, मगर, फ्रेशवाटर टर्टल्स, पनकौआ, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, संगमरमरी टील आदि। वनस्पतियों में सरपत, मूंज, नरकुल, सेवार, तिन्नाधान, कसेरू, कमलगट्टा, मखाना, सिंघाड़ा आदि प्रमुख हैं।
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : http://www.ontarioparks.com/parksblog/wp-content/uploads/2018/03/Wetland-cell-3-summer-2017-1-825×510.jpg