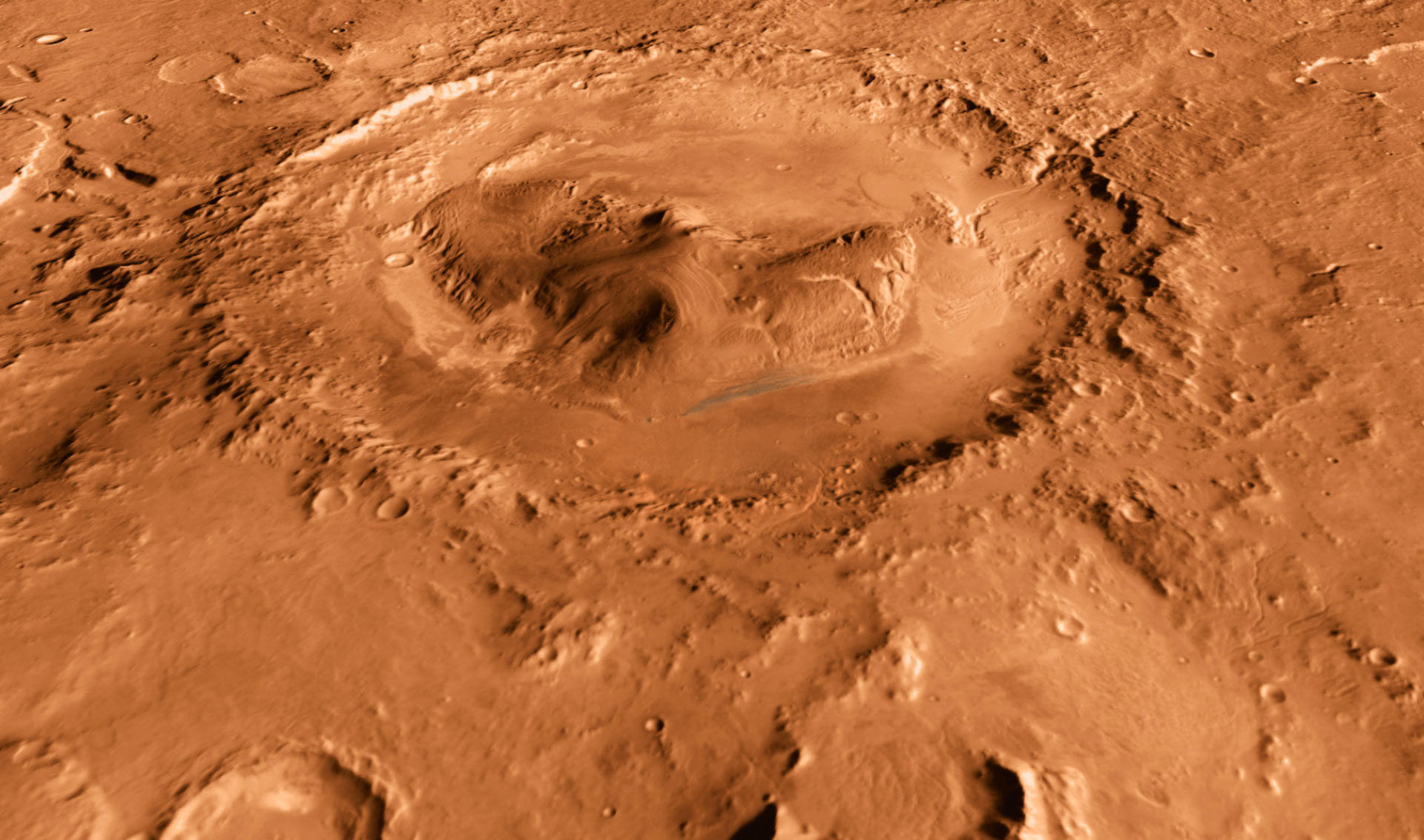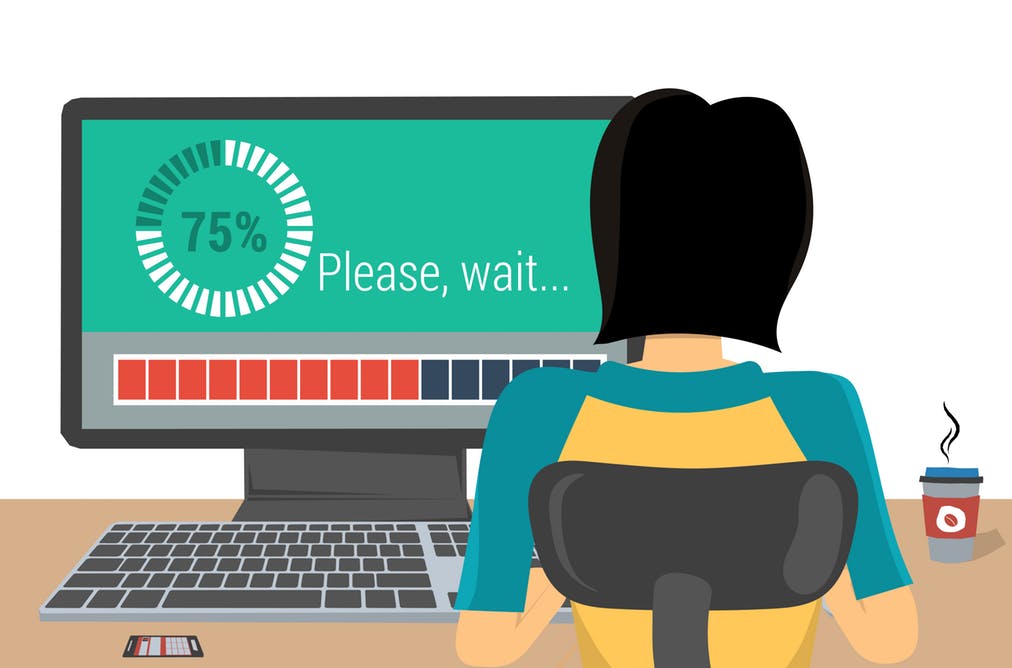हालांकि भूमिगत जल में व्यापक आर्सेनिक प्रदूषण भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बंगाल डेल्टा बेसिन के इलाकों तक सीमित है किंतु भारत के कई हिस्सों और राज्यों के भूमिगत जल में भी आर्सेनिक पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की सुरक्षित मात्रा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। किंतु वर्तमान में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों के भूमिगत जल में 50 से 3700 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया गया है। भूमिगत जल में आर्सेनिक पाए जाने के कुछ भूगर्भीय कारण माने जाते हैं। अब तक आर्सेनिक प्रदूषित इलाकों में सबसे अधिक ध्यान पेयजल पर दिया जा रहा था जबकि इन इलाकों में भूमिगत जल का उपयोग पेयजल से ज़्यादा सिंचार्इं में किया जाता है। आर्सेनिक युक्त भूमिगत जल वाले इलाकों में सिंचाई के कारण मिट्टी–पौधे–मनुष्य शृंखला पर होने वाले असर पर अध्ययन बहुत कम हुए हैं। वास्तव में बंगाल डेल्टा बेसिन समेत आर्सेनिक प्रभावित अन्य क्षेत्रों में इस तरह के शोध की आवश्यकता है। आर्सेनिक प्रदूषण के मुख्य कारण को पहचानना महत्वपूर्ण है। जहां पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण का स्रोत एक बिंदु पर सिमटा होता है, वहीं खेती में आर्सेनिक प्रदूषित भूजल से सिंचाई के माध्यम से मानव–खाद्य शृंखलामेंफैलताहैऔरखाद्य शृंखलामेंआगेबढ़ते हुए इसकी गंभीरता बढ़ती है। इस लेख में आर्सेनिक प्रदूषण के महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों के साथ–साथ इसके समाधान की सूची बनाने का प्रयास किया है। इसमें लोगों की भागीदारी अहम होगी। साथ ही उचित नीतियों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।
भूमिका
आर्सेनिक फारसी शब्द ज़ार्निक से आया है जो यूनानी में आर्सेनिकॉन हुआ। हिंदी में इसे संखिया कहते हैं। पर्शिया और अन्य जगहों के लोग आर्सेनिक का उपयोग प्राचीन काल से करते रहे हैं। आर्सेनिक ‘शाही ज़हर’और ‘ज़हर का राजा’नाम से भी मशहूर है।
कांस्य युग में आर्सेनिक कांसे में अशुद्धि के रूप में मौजूद होता था जिससे धातु कठोर हो जाती थी। माना जाता है कि अल्बर्टस मैग्नस ने 1250 ईस्वीं में इस तत्व को सबसे पहले पृथक किया था। आर्सेनिक का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। कीटनाशकों के छिड़काव से मानव खाद्य और पर्यावरण में आर्सेनिक प्रदूषण हुआ है जिसका लोगों और उनकी अगली पीढ़ी के स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूमिगत आर्सेनिक दुनिया की कई जगहों के पेयजल स्रोतों को प्रभावित करता है। लगातार सालों तक प्रदूषित पानी पीने की वजह से लाखों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
मिट्टी, पानी, वनस्पति, पशु और मानव में विषैले आर्सेनिक की मौजूदगी पर्यावरणीय चिंता का विषय है। जैव–मंडल में इसके अति विषैलेपन और बढ़ी हुई मात्रा ने सार्वजनिक और राजनीतिक चिंता को जन्म दिया है। अर्जेंटाइना, चिली, फिनलैंड, हंगरी, मेक्सिको, नेपाल, ताइवान, बांग्लादेश और भारत समेत दुनिया के 20 देशों में भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण और इसके कारण मानव स्वास्थ सम्बंधी समस्या दर्ज हुई है। सबसे अधिक प्रदूषण और स्वास्थ्य सम्बंधी समस्या बांग्लादेश में है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। बंगाल डेल्टा बेसिन के लाखों लोग खतरे में हैं। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे बसे 5 ज़िलों और इसकी सीमा से लगे बांग्लादेश के ज़िलों में मुख्य रूप से भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण है। बंगाल डेल्टा बेसिन के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी अधिक निकली है। इसके अलावा चट्टानों, अन्य पदार्थों और पानी के विभिन्न स्रोतों में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है।
अधिकतम की सीमा
डब्ल्यूएचओ ने अस्थायी तौर पर पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर निर्धारित की है क्योंकि इससे कम स्तर के प्रदूषण का मापन बड़े पैमाने पर संभव नहीं है। भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों में डब्ल्यूएचओ की इससे पूर्व 1971 में निर्धारित स्वीकार्य सीमा 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर थी। हाल ही में भारत ने भी पेयजल में आर्सेनिक की स्वीकार्य सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर निर्धारित की है।
मनुष्यों में अकार्बनिक आर्सेनिक यौगिकों के कारण कैंसर होने के पर्याप्त प्रमाण और जानवरों में सीमित प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर अकार्बनिक आर्सेनिक यौगिकों के समूह को कैंसर–जनक समूह में रखा गया है। इसलिए पेयजल में आर्सेनिक की उपस्थिति की स्वीकार्य सीमा को घटाकर 5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर करना विचाराधीन है। किंतु कार्बनिक आर्सेनिक की कैंसरकारिता के पर्याप्त प्रमाण नहीं है। 1983 में एफएओ/डब्ल्यूएचओ की एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा मनुष्यों द्वारा अकार्बनिक आर्सेनिक के दैनिक सेवन की अधिकतम सीमा शरीर के प्रति किलोग्राम वज़न पर 2.1 माइक्रोग्राम तय की गई है। इसके बाद 1988 में साप्ताहिक स्वीकार्य सेवन की सीमा शरीर के प्रति किलोग्राम वजन पर 15 माइक्रोग्राम निर्धारित की गई। किंतु इस तरह के मानक मिट्टी, पौधे और पशुओं के लिए निर्धारित नहीं हैं।
पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक सांद्रता (50-3700 माइक्रोग्राम प्रति लीटर) भारत और डब्ल्यूएचओ की निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक है। इसके अलावा, पंजाब के भूमिगत जल में आर्सेनिक सांद्रता 4 से 688 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक है। 1978 में पहली बार पश्चिम बंगाल में भूजल में आर्सेनिक की निर्धारित सीमा से अधिक उपस्थिति का पता चला था और मनुष्यों में आर्सेनिक के विषैले असर का पहला मामला 1983 में कलकत्ता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में सामने आया था। पेयजल में अकार्बनिक आर्सेनिक और वयस्कों में इसके स्वास्थ्य सम्बंधी प्रभावों को चिकित्सक भलीभांति स्थापित कर चुके हैं।
अब तक भूमिगत जल में आर्सेनिक की उपस्थिति को पेयजल की समस्या के तौर पर ही देखा जा रहा था जबकि पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो मिट्टी और कृषि उपज में आर्सेनिक अधिक मात्रा में होने की संभावना है। दरअसल आर्सेनिक युक्त मिट्टी में खेती और आर्सेनिक युक्त जल से सिंचाई के कारण कृषि उपज में आर्सेनिक पहुंचने की बात कई शोधकर्ता बता चुके हैं। इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। जहां पेयजल में आर्सेनिक की समस्या किसी ट्यूब वेल जैसे स्पष्ट स्रोत से जोड़ी जा सकती है वहीं कृषि उपज में आर्सेनिक की उपस्थिति एक विस्तृत और अनिश्चित–सा स्रोत है। इस बात का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब यह देखा जाता है कि ऐसे लोगों के मूत्र के नमूनों में भी उच्च मात्रा में आर्सेनिक निकला है जिन्होंने कभी आर्सेनिक युक्त पानी नहीं पीया। दिलचस्प बात यह है कि आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में सतही जल स्रोत आर्सेनिक मुक्त हैं। इससे लगता है कि मिट्टी आर्सेनिक युक्त पानी लेती है और इसे अपने में ही रोक कर रखती है और आस पास के जल–स्रोतों में इसे फैलने नहीं देती।
स्वास्थ्य पर प्रभाव
प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आर्सेनिक विषैला तत्व है। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड की अत्यंत कम मात्रा (0.1 ग्राम) भी इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आर्सेनिक विषाक्तता के शुरुआती लक्षण त्वचा सम्बंधी विकार, कमज़ोरी, थकान, एनोरेक्सिया (भूख न लगना), मितली, उल्टी और दस्त या कब्ज़ हैं। जैसे–जैसे विषाक्तता बढ़ती है, लक्षण और अधिक विशिष्ट होने लगते हैं, जिनमें गंभीर दस्त, पानीदार सूजन (विशेष रूप से पलकों और एड़ियों पर), त्वचा का रंग बदलना, आर्सेनिकल काला कैंसर और चमड़ी का मोटा व सख्त होना, लीवर बढ़ना, श्वसन रोग और त्वचा कैंसर शामिल हैं। कुछ गंभीर मामलों में पैर में गेंग्रीन और ऊतकों में असामान्य वृद्धि भी देखी गई है। आर्सेनिक विषाक्तता के कारण अर्जेंटाइना में ‘बेल विले रोग’, ताइवान में ‘ब्लैक फुट रोग’ और थाईलैंड में ‘काई डेम’ रोग व्याप्त हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के बाल, नाखून, त्वचा और पेशाब के कई नमूनों में निर्धारित सीमा से अधिक आर्सेनिक था।
मनुष्यों पर प्रभाव
आर्सेनिक के रूप और विषाक्तता
भूमिगत जल और मिट्टी में आर्सेनिक कार्बनिक रूपों के अलावा आर्सेनाइट्स (तीन–संयोजी आर्सेनिक) या आर्सेनेट (पांच–संयोजी आर्सेनिक) के रूप में मौजूद रहता है। मिट्टी और फसल में आर्सेनिक की घुलनशीलता, गतिशीलता, जैव उपलब्धता और विषाक्तता मुख्य रूप से आर्सेनिक की ऑक्सीकरण अवस्था (वैलेंसी) पर निर्भर करती है। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह अकार्बनिक रूप में है या कार्बनिक रूप में। भूमिगत जल/मिट्टी में विभिन्न आर्सेनिक यौगिकों के विषैलेपन का क्रम:
आर्सीन > ऑर्गेनो–आर्सेनिक यौगिक > आर्सेनाइट्स और ऑक्साइड > आर्सेनेट्स > एक–संयोजी आर्सेनिक > मुक्त आर्सेनिक धातु।
जल और मिट्टी में आर्सेनेट की तुलना में आर्सेनाइट अधिक घुलनशील, गतिशील और ज़हरीला होता है। आर्सेनिक के कार्बनिक रूप मुख्य रुप से डाईमिथाइल आर्सेनिक एसिड या केकोडाइलिक एसिड भी मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। ये मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थितियों में वाष्पशील डाईमिथाइल आर्सीन और ट्राईमिथाइल आर्सीन बनाते हैं। भूमिगत जल और मिट्टी में मोनो मिथाइल आर्सेनिक एसिड (एमएमए) भी मौजूद रहता है। आर्सेनिक के कार्बनिक रूप या तो ज़हरीले नहीं होते या बहुत कम ज़हरीले होते हैं। जब फसलों को हवादार मिट्टी में उगाया जाता है तो मिट्टी में मुख्य रूप से पांच–संयोजी आर्सेनिक पाया जाता है। यह कम ज़हरीला होता है। जबकि चावल के पानी भरे खेतों में अधिक घुलनशील और ज़हरीले तीन–संयोजी रूप अधिक रहते हैं।
मिट्टी–फसल में आर्सेनिक की उपस्थिति और खाद्य शृंखला पर प्रभाव
यह पाया गया कि शरद ऋतु में उगाई जाने वाली धान से प्राप्त चावल में आर्सेनिक के अधिक विषैले तीन–संयोजी रूप पाए जाते हैं। दूसरी ओर, चावल के भूसे में आर्सेनिक के पांच–संयोजी रूप मौजूद होते हैं। इसके अलावा धान की, पारंपरिक और उच्च पैदावार, दोनों ही किस्मों के साथ पारबॉइलिंग और मिलिंग जैसी प्रक्रियाओं में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है। जैविक खाद के माध्यम से मृदा संशोधन करने पर आर्सेनिक की मात्रा में कमी आती है। आर्सेनिक प्रदूषित इलाकों में उगाए जाने वाले चावल में आर्सेनिक विषाक्तता और इसके सेवन से सम्बंधित खतरों का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण बंगाल में चावल के माध्यम से अकार्बनिक आर्सेनिक का सेवन, दूषित पेयजल की तुलना में मानव स्वास्थ के लिए ज़्यादा बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। जैविक संशोधन और संवर्धित फॉस्फेट तथा चुनिंदा सूक्ष्म पोषक तत्वों (जैसे जस्ता, लौह) से उर्वरीकरण चावल में आर्सेनिक को कम करता है। साथ ही इसके सेवन से होने वाला खतरा भी कम होता है।
भूजल दूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में पानी और आहार दोनों के माध्यम से आर्सेनिक सेवन और पेशाब में आर्सेनिक के उत्सर्जन को लेकर किए गए कई अध्ययन बताते हैं कि आर्सेनिक प्रदूषित इलाकों में सिर्फ पेयजल में आर्सेनिक की समस्या को दूर करने से आर्सेनिक सम्बंधी खतरे कम नहीं होंगे। चावल का नियमित सेवन शरीर में आर्सेनिक पहुंचने का एक प्रमुख ज़रिया है जिसका समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। आर्सेनिक विषाक्तता के उपचार के लिए समग्र व समेकित तरीके की आवश्यकता है जिसमें खाद्य शृंखला में आर्सेनिक की उपस्थिति और पेयजल में आर्सेनिक सुरक्षित मात्रा की सीमा में रखने के मिले–जुले प्रयास करने होंगे।
सुधार के उपाय
चावल समेत कई उपज में आर्सेनिक की उपस्थिति को कम करने में कुछ उपाय काफी प्रभावी पाए गए हैं।
1. कम वर्षा वाली अवधि में आर्सेनिक युक्त पानी से सिंचाई कम करने के लिए सतही जल स्रोतों और भूमिगत जल का मिला–जुला इस्तेमाल हो। साथ ही वर्षा के आर्सेनिक–मुक्त पानी को ज़मीन में पहुंचाने की व्यवस्था हो।
2. आर्सेनिक युक्त इलाकों में कम पानी में ज़्यादा फसल देने वाली और आर्सेनिक का कम संग्रह करने वाली किस्मों की पहचान/विकास हो। इन इलाकों में खास तौर से जनवरी से मई के कम वर्षा वाले दिनों में अनुकूल फसल चक्र अपनाया जाए। जैसे जूट–चावल–चावल या हरी खाद–चावल–चावल की जगह जमीकंद–सरसों–तिल, मूंग–धान–सरसों जैसे फसल चक्र।
3. भूजल को तालाब में भरकर उस संग्रहित पानी से सिंचाई करना। इस तरह अवसादन और वर्षा का पानी मिलने से संग्रहित पानी में आर्सेनिक की मात्रा कम की जा सकती है।
4. धान की सिचांई के लिए भूमिगत जल की दक्षता को बढ़ाना, खास तौर पर गर्मियों की धान में। उदाहरण के लिए फसल की वृद्धि के दौरान कुछ–कुछ समय खेतों में पानी भरा जाए और पकने के दौरान लगातार पानी भरकर रखा जाए। ऐसा करने से फसल की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भूजल का उपयोग कम होने से आर्सेनिक की मात्रा में कमी आएगी।
5. कंपोस्ट और अन्य जैविक व हरी खाद का उपयोग बढ़ाएं। साथ ही अकार्बनिक लवणों का उपयुक्त उपयोग किया जाए।
6. ऐसी फसलों की पहचान और विकास हो जो फसल के खाद्य हिस्सों में कम से कम आर्सेनिक जमा करती हों और जिनमें आर्सेनिक के अकार्बनिक रूपों का अनुपात कम हो।
7. सस्ते वनस्पति और जैविक उपचार विकल्प विकसित करना चाहिए।
8. बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार।
9. लोगों की भगीदारी से खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के उपायों को अपनाया और लोकप्रिय बनाया जाए।
नीतिगत हस्तक्षेप
देश के कुछ हिस्सों के भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण का मुद्दा और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, सामुदायिक शोधकर्ताओं, कानून बनाने वालों और आम जनता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आर्सेनिक प्रदूषण के संदर्भ में मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति की समस्या को दूर करने पर ज़ोर दिया गया है। पेयजल की समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन इलाकों में पेयजल के अधिकतर विकल्प या तो सतही जल स्रोत या 150-200 मीटर से अधिक गहराई के जल–स्रोत के उपयोग पर आधारित हैं। इस गहराई में पानी में विषैले पदार्थ नहीं होते। इन पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की समय–समय पर जांच भी काफी अच्छे से होती है।
खाद्य शृंखला का मुद्दा अनछुआ रह जाता है। आर्सेनिक–प्रदूषित भूजल से सिंचाई के माध्यम से आर्सेनिक खाद्य पदार्थों में पहुंचता है। वैसे इस बारे में काफी समझ बनी है कि खाद्य शृंखला द्वारा ग्रामीण इलाकों में आर्सेनिक लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। इसलिए बड़े स्तर पर आर्सेनिक विषाक्तता को दूर करने के लिए पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा को कम करने के साथ–साथ खाद्य शृंखला से आर्सेनिक को दूर करने के लिए समेकित तरीके अपनाने की ज़रूरत है। जब तक यह प्रयास सफल नहीं होता तब तक सुरक्षित खाद्य की चिंता बनी रहेगी। वैज्ञानिकों के बीच इस मुद्दे की गंभीरता के एहसास के बावजूद अभी तक ठोस योजना बनाने की दरकार है। शुरू में छोटे स्तर पर प्रायोगिक कार्यक्रम लागू करके फिर इसे प्रभावित क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है।
इस तरह के एकीकृत तरीकों की सफलता विभिन्न हितधारकों की प्रकृति, शोधकर्ताओं, तकनीशियनों और योजनाकारों को जोड़कर ही संभव है जिसमें वास्तविक लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। लाभार्थी इस कार्यक्रम को समझ सकें और उसमें अपना योगदान दे सकें इसके लिए उन्हें जागरूक और प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। खालिस तकनीकी तरीकों की जगह समेकित तरीके अपनाने के लिए तकनीकी व्यावहारिकता, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से मज़बूत कार्य योजना की ज़रूरत है।
निष्कर्ष
लोगो को पेयजल की गुणवत्ता जांचने के मामले में जागरूक करना और परीक्षण करने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। गंभीर त्वचा–घाव से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य खतरे और परेशानी को ध्यान में रखते हुए आर्सेनिक मुक्त पेयजल की आपूर्ति के साथ राज्य अस्पतालों में इन रोगियों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था बीमारी को कम करने में मदद कर सकती है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आर्सेनिक से प्रभावित लोग बहुत गरीब हैं व दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।
जैसा कि पहले बताया गया है, बंगाल और अन्यत्र सिंचाई और पीने के लिए आर्सेनिक प्रदूषित भूजल ही समस्या की जड़ है। आर्सेनिक प्रदूषित भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी और खाद्य शृंखला में काफी आर्सेनिक प्रदूषण हुआ है। आर्सेनिक प्रदूषित जल का उपयोग कम करने और इसके उपायों के बारे में किसानों को जागरूक बनाने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा समेकित तरीके की सफलता के लिए सिर्फ कृषि वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि चिकित्सकों, सामाजिक वैज्ञानिकों और योजनाकारों को भी साथ लाना होगा।
फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर आर्सेनिक की मात्रा पता करने के लिए खेतों और प्रयोगशाला प्रोटोकॉल में सुधार की ज़रूरत है ताकि भूमिगत जल में विभिन्न आर्सेनिक रूपों का मापन किया जा सके। खाद्य शृंखला में कुल आर्सेनिक के कारण कितनी विषाक्तता है इसे पहचानने की ज़रूरत है। इसके अलावा विविध संस्थाओं और विविध विषयों को जोड़कर कार्यक्रमों को मज़बूत करना होगा, तभी आर्सेनिक–दूषित संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए दीर्घकालिक तकनीकी विकल्प विकसित हो सकेंगे। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : Yourstory