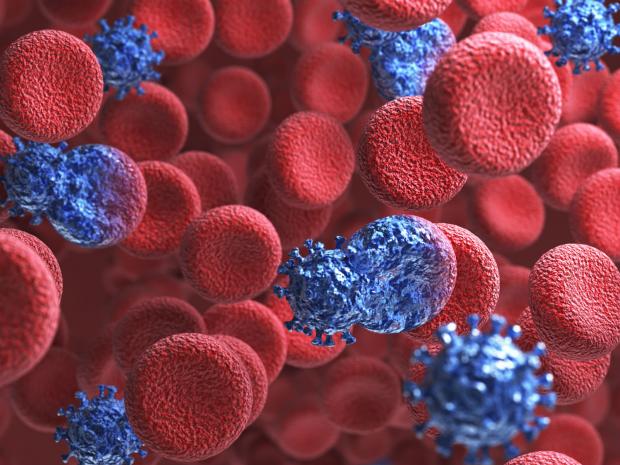भारत में वर्ष 2014 से एलईडी बल्ब की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उजाला कार्यक्रम के तहत सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की बदौलत हुई है। हालांकि, फिलामेंट बल्ब की मांग अभी भी काफी है, हालांकि धीरे–धीरे घट रही है। 2017 में, भारत में लगभग 77 करोड़ फिलामेंट बल्ब बेचे गए थे, जो उस वर्ष बल्ब और ट्यूब–लाइट की कुल बिक्री के 50 प्रतिशत से भी अधिक था।
इस आलेख में, हम भारत में फिलामेंट बल्ब के निरंतर उपयोग की जांच के लिए भारतीय घरों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकाश विकल्पों की मांग और आपूर्ति के कुछ पहलुओं की जांच करेंगे। इस विश्लेषण के आधार पर, हम भारत में फिलामेंट बल्ब के उपयोग को कम करने और अंतत: समाप्त करने करने के लिए कुछ कार्यक्रम और नीतिगत हस्तक्षेपों के सुझाव भी देंगे।
हमने अपने द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया कि लोग, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में, एलईडी बल्ब और उसके लाभों से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं हैं। संभावित उपभोक्ता की प्रमुख चिंता एलईडी बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की गुणवत्ता और देश में खराब बिजली आपूर्ति के मद्देनज़र उनके टिकाऊपन को लेकर है। एलईडी बल्ब की एकमुश्त ऊंची कीमत अभी भी एक चुनौती है क्योंकि अधिकांश सर्वेक्षित घरों ने वित्त पोषित योजना को पसंद किया है। सर्वेक्षण में स्थानीय बाज़ारों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्बों की सीमित उपलब्धता का भी पता चला है।
जहां तक फिलामेंट बल्ब की आपूर्ति का सवाल है, मुट्ठी भर कंपनियां भारत में अधिकांश फिलामेंट बल्ब का उत्पादन करती हैं। फिलामेंट बल्ब का उत्पादन करने वाले कारखाने पुराने, घिसे–पिटे और स्वचालित हैं। फिलामेंट बल्ब के उत्पादन में शोध, गारंटी और विपणन की लागत बहुत कम होती है। इस कारण से कंपनियां फिलामेंट बल्ब बहुत कम कीमत पर बेच पाती हैं। इसके अलावा, फिलामेंट बल्ब उद्योग में कोई नया प्रवेशकर्ता भी नहीं है।
दूसरी तरफ, एलईडी लाइटिंग उद्योग हाल ही के वर्षों में उजाला कार्यक्रम द्वारा उत्पन्न मांग पर चल रहा है। चूंकि शुरुआती पूंजी निवेश कम लगता है और बल्ब के पुर्ज़ों को हाथ से जोड़ा जा सकता है, इसलिए मांग को पूरा करने के लिए लघु उद्योग भी मौजूद है। भारतीय मानक ब्यूरो और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास एलईडी बल्बों के प्रदर्शन और सुरक्षा सम्बंधी अनिवार्य मानक हैं। हालांकि, बाज़ार में उपलब्ध उत्पादों में इन मानकों के अनुपालन को लेकर स्थिति चिंताजनक है। मात्र कीमत में कमी पर ध्यान केन्द्रित किए जाने के कारण शायद एलईडी बल्ब की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ होगा। खास तौर से उन पहलुओं की उपेक्षा हुई होगी जो उनके जीवनकाल और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। मौजूदा मानकों में शायद इन्हें सटीक रूप से पकड़ा नहीं जा सका है।
फिलामेंट बल्ब को बाज़ार से दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अब तक अपनाए गए मूल्य–केंद्रित हस्तक्षेप एलईडी बल्ब की कीमत को कम करके उनकी मांग में वृद्धि करने में सफल रहे हैं। किंतु फिलामेंट बल्ब से पूरी तरह से निजात पाने के लिए मूल्य–केंद्रित हस्तक्षेप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लोगों को एलईडी बल्ब के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित कर सकता है। ऐसे अभियान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के स्टार रेटिंग कार्यक्रम द्वारा प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब खरीदने के बारे में जागरूकता भी बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और भारतीय मानक ब्यूरो समय–समय पर मानकों के अनुपालन की जांच कर सकते हैं और अनुपालन न करने वालों की जानकारी प्रकाशित भी कर सकते हैं। उजाला की कार्यान्वयन एजेंसी, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल), खरीदे गए एलईडी बल्बों की गुणवत्ता की जांच कर सकती है और अनुपालन न करने वाले निर्माताओं को ब्लैक–लिस्ट कर सकती है। ईईएसएल सुनिश्चित कर सकता है कि गारंटीशुदा बल्बों को बदलने की प्रक्रिया आसान हो। इससे लोगों में एलईडी बल्ब की गुणवत्ता को लेकर विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। एलईडी बल्ब के ऊंचे मूल्य के मुद्दे को हल करने के लिए, ईईएसएल बिल भुगतान के समय वित्त पोषण प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दे सकता है। यह उजाला कार्यक्रम का हिस्सा तो रहा है, लेकिन इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ईईएसएल ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए डाकघर, पेट्रोल पंप और ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से वितरण की अपनी वर्तमान पहल को जारी रख सकता है। सरकार का विद्युतीकरण कार्यक्रम – सौभाग्य – नव विद्युतीकृत घरों में एलईडी बल्ब के उपयोग को बढ़ावा देने का एक और तरीका हो सकता है।
एलईडी बल्ब के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने, उनकी कीमत को कम करने और उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने और आसान बनाने जैसे हस्तक्षेपों से भारत में फिलामेंट बल्ब के उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। लेकिन आज की स्थिति में तो अन्य समस्याओं को संबोधित किए बिना फिलामेंट बल्ब को एकाएक विदा करने की सिफारिश नहीं की जा सकती है। ऐसा करने से इसका बोझ मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग और नव विद्युतीकृत घरों पर पड़ेगा। (स्रोत फीचर्स)
पुणे स्थित प्रयास (ऊर्जा समूह) ने हाल ही में एलईडी बल्बों के उपयोग सम्बंधी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी – ‘ऑब्स्टिनेट बल्ब – मूविंग बियॉण्ड प्राइस फोकस्ड इंटरवेंशन्स टु टेकल इंडियाज़ पर्सिस्टेंट इनकेंडेसेंट बल्ब प्रॉबलम’। यह रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.prayaspune.org/peg/publications/item/380यहां उस रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत है।
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo credit: IndiaMart