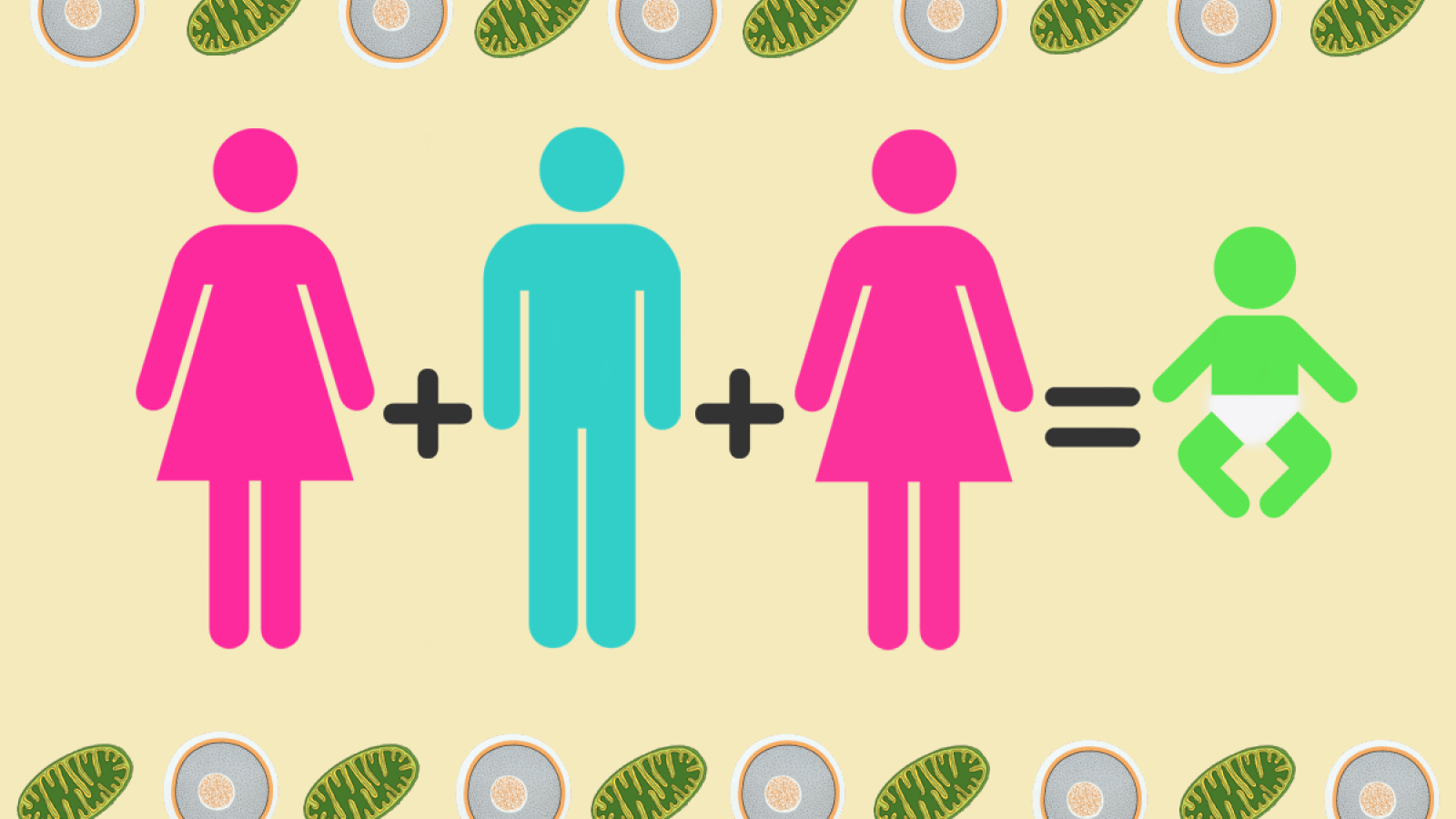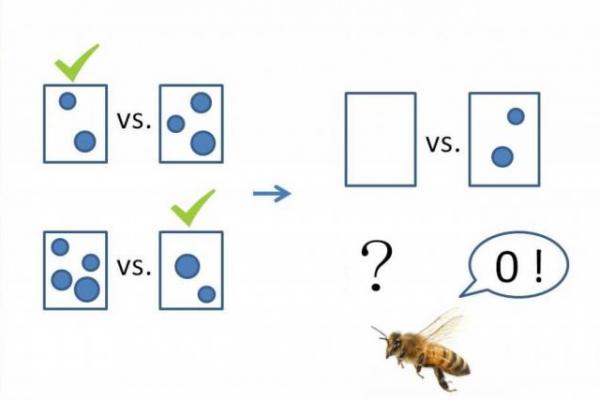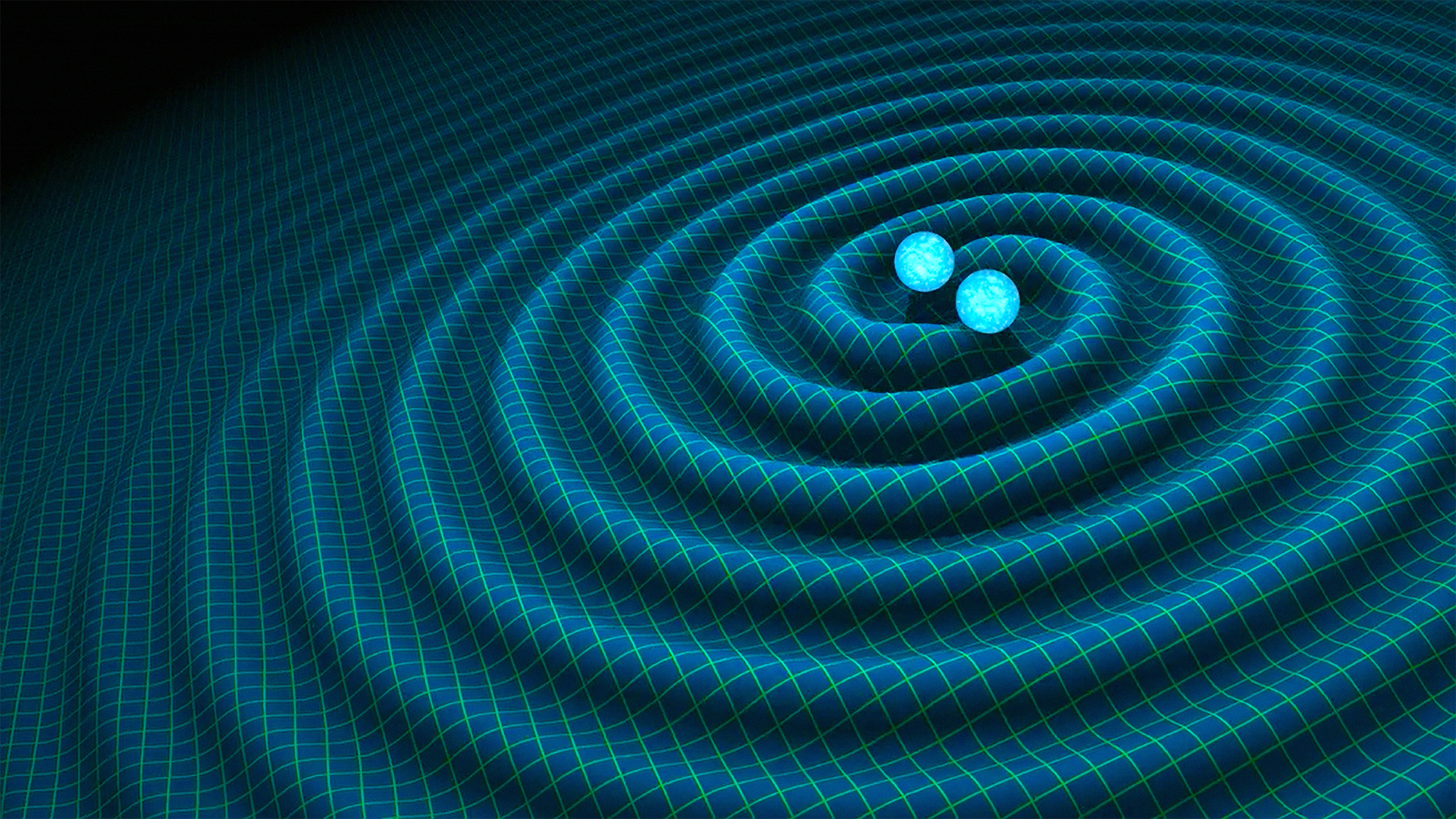भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल यानी एसोचैम के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद के ताज़ा अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करने वाला देश है। यहां हर वर्ष 13 लाख टन ई–कचरा उत्पन्न होता है, जिसका सिर्फ1.5 प्रतिशत भाग विभिन्न संगठित अथवा असंगठित इकाइयों में दोबारा इस्तेमाल योग्यबनाया जाता है।
असल में आज का युग उपभोक्तावाद का युग है और इस युग को तेज़ गति प्रदान की है सूचना तथा संचार क्रांति ने। अर्थव्यवस्था, उद्योगों तथा संस्थाओं सहित हमारे दैनिक जीवन में सूचना तथा संचार क्रांति तेज़ी से बदलाव ला रही है। एक ओर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर यही उत्पाद, संसाधनों के अनियंत्रित उपभोग तथा भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
प्रौद्योगिकी का तेज़ विकास, तकनीकी आविष्कारों का आधुनिकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तेज़ी से बदलाव के कारण विश्व में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई–कचरा इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत उपकरणों से उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी प्रकार के कचरे को कहते हैं, जिनकी अब मूल रूप में उपयोगिता नहीं रही है और जिन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाने या पूरी तरह समाप्त कर देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पुराने रेफ्रिजरेटर, खराब हो चुकी वॉशिंग मशीन, बेकार कंप्यूटर तथा प्रिंटर, टेलीविज़न, मोबाइल, आईपॉड, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि।
देश में उत्पन्न ई–कचरे का 90% से अधिक भाग असंगठित बाज़ार में दोबारा इस्तेमाल के लिए अथवा नष्ट करने के लिए पहुंचता है। ये असंगठित क्षेत्रआम तौर पर महानगरों तथा बड़े शहरों की झुग्गीबस्तियों में होते हैं, जहां अकुशल कामगार लागत कम करने के उद्देश्य से बिलकुल अनगढ़ तरीकों से ई–कचरे को दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। ये कामगार खतरनाक परिस्थितियों जैसे, दस्तानों तथा मुखौटों का प्रयोग किए बिना कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में कचरे से निकलने वाली गैसें, अम्ल, विषैला धुआं तथा विषैली राख कामगारों तथा स्थानीय पर्यावरण के लिए खतरनाक होती है ।
ई–कचरे में कई प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले तथा विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे, सर्किट बोर्ड में कैडमियम तथा लेड, स्विच तथा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में पारा, पुराने कैपेसिटर्स तथा ट्रांसफार्मर्स में पोलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल तथा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जलाने पर निकलने वाली ब्रोमीन–युक्त आग। इन हानिकारक पदार्थों तथा विषैले धुएं के लगातार सम्पर्क में रहने से इस काम में लगे कामगारों में बीमारियां पनपती हैं।
देश के 70 प्रतिशत ई–कचरे का उत्पादन देश के 10 राज्यों में होता है, जिसमें 19.8 प्रतिशत योगदान के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु में 13.1 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 12.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 10.1 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 9.8 प्रतिशत, दिल्ली में 9.5 प्रतिशत, कर्नाटक में 8.9 प्रतिशत, गुजरात में 8.8 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश में 7.6 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन होता है।
देश में बढ़ते ई–कचरे के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई–कचरा प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया है। 2018 में इसनियम में सुधार किया गया, ताकिदेश में ई–कचरे के निस्तारण को दिशा दी जा सके तथा निर्धारित तरीके से कचरे को नष्टअथवा पुनर्चक्रित किया जा सके। कोशिश यह है किई–कचरे को ठिकाने लगाने के क्षेत्रको मान्यता प्राप्त हो, कामगारों के स्वास्थ्यपर बुरा प्रभाव ना पड़े तथा वातावरण प्रदूषित न हो।
नए नियमों में इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के उत्पादकों के लिए उनके निस्तारण, प्रबंधन तथा परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2018 के संशोधन के बाद अब यह इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं की ज़िम्मेदारी है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ई–कचरे को एकत्र करके निस्तारण करें। इससे उत्पादक भी कम विषैले तथा पर्यावरण के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरित होंगे, और उपभोक्ता स्वस्थ वातावरण में प्रौद्योगिकी के विकास का सार्थक एवं स्वस्थ उपयोग कर सकें । (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
फोटो क्रेडिट : Wired