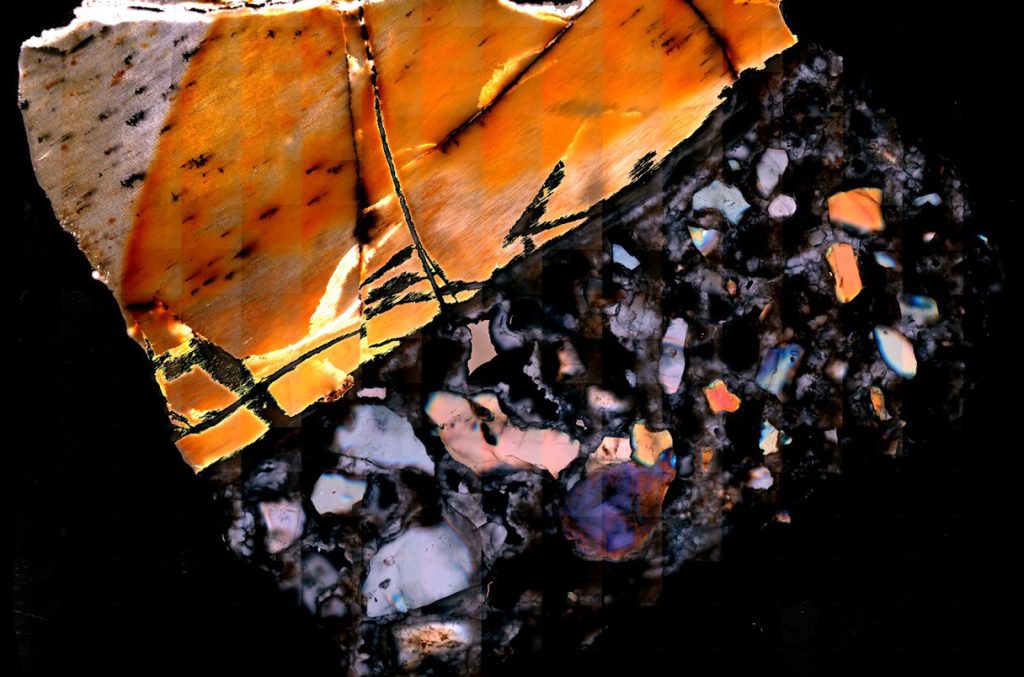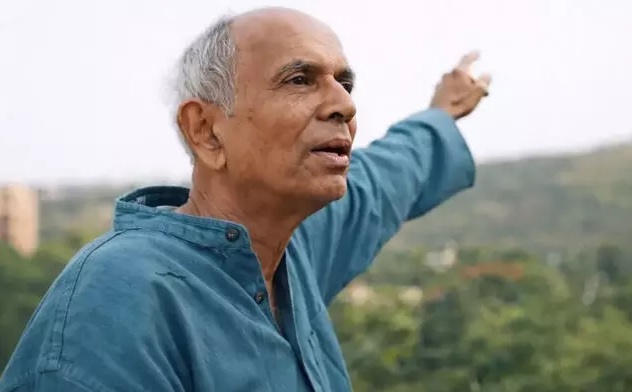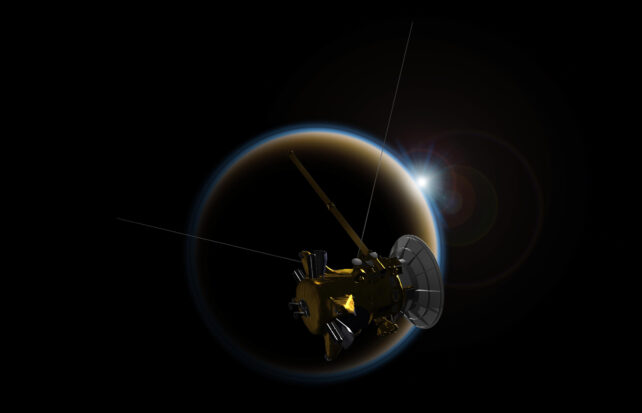भारत डोगरा

जलवायु बदलाव (climate change) की समस्या के समाधान के रूप में विश्व स्तर पर दो तरह के प्रयास चर्चित हैं। पहला तो यह है कि इसके लिए ज़िम्मेदार ग्रीनहाऊस गैसों (greenhouse gases) के उत्सर्जन को कम किया जाए। दूसरा, कि इस समस्या का सामना करने के लिए लोगों व समुदायों की तैयारी बेहतर हो। इन दो पक्षों को प्रायः मिटिगेशन व एडाप्टेशन कहा जाता है व ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आगे चुनौती ऐसा कार्यक्रम बनाने की है जिनसे लोगों की आजीविका भी बेहतर हो तथा साथ में जलवायु बदलाव संकट के इन दोनों पक्षों पर भी कार्य आगे बढ़ सके।
भारत जैसे विकासशील देशों (developing countries) के संदर्भ में तो यह चुनौती और भी अहम है क्योंकि जहां जलवायु बदलाव के संदर्भ में हमें अपनी ज़िम्मेदारी अवश्य निभानी है पर साथ में आजीविका व आर्थिक पक्ष (economic development) को भी आगे बढ़ाना है। ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जिनमें उचित समन्वय बन सके। फिर भारत जैसे देश में यह समन्वय ग्रामीण क्षेत्रों में बनाना तो और भी ज़रूरी हो गया है।
यदि हम पहले पक्ष ‘मिटिगेशन’ या ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात करें तो प्राकृतिक खेती (natural farming) व बागवानी (sustainable agriculture) को बढ़ाना इसमें अहम कदम है। प्राकृतिक खेती व बागवानी को बढ़ाकर कृषि पर ग्रीनहाऊस गैस का अत्यधिक उत्सर्जन करने वाले जीवाश्म ईंधन का जो बड़ा बोझ है, उसे कम किया जा सकता है। यदि किसी गांव में प्राकृतिक खेती के त्वरित प्रसार से रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा आदि का उपयोग कम होता है तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग व ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे औज़ारों के उपयोग को प्रोत्साहित कर बड़ी मशीनों व ट्रैक्टरों आदि में डीज़ल की अधिक खपत की संभावना भी कम होती है।
प्राकृतिक खाद (organic manure) के उपयोग से व प्राकृतिक खेती से खेतों की मिट्टी में जैविक तत्व बढ़ता है, उसकी मिट्टी में कार्बन संजोने की क्षमता (carbon sequestration) बढ़ती है व वायुमंडल में कार्बन डाईक्साइड का उत्सर्जन कम होता है।
किसान छोटे बगीचों में फलदार पेड़ लगा सकते हैं, गावों के आसपास मिश्रित स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष (native species) इस तरह साथ-साथ लगाए जा सकते हैं कि वे एक साथ एक-दूसरे से सहयोग करते हुए पनप सकें।
दूसरी ओर, जलवायु बदलाव व उससे जुड़े प्रतिकूल मौसम और आपदाओं का सामना बेहतर ढंग से करने की क्षमता यानी एडाप्टेशन (climate resilience) के लिए जल व मिट्टी संरक्षण (water and soil conservation) सबसे महत्त्वपूर्ण है। जल व मिट्टी संरक्षण से सूखे व बाढ़ (drought and flood) दोनों तरह की आपदाओं को कम करने में मदद मिलती है व साथ में ग्रामीण आजीविकाओं का मज़बूत आधार तैयार होता है। सामान्य वर्ष में भी कुछ महीनों के लिए अनेक गांवों के जल-स्रोत सूख जाते हैं। यह स्थिति गांववासियों के लिए ही नहीं, पशु-पक्षियों के लिए भी बड़ा संकट बन जाती है।
वन्य जीव-जंतुओं (wildlife) व आवारा घूम रहे पशुओं के लिए भी प्यास का संकट बढ़ जाता है। जल-संरक्षण से यह संभावना बढ़ती है कि इन जल-स्रोतों में वर्ष भर पानी की उपस्थिति बनी रहेगी। जल संरक्षण से भूजल स्तर (groundwater level) ठीक बना रहता है जिससे कुंओं व हैंडपंप आदि से पानी मिलता रहता है। अधिक वर्षा के समय बहुत-सा पानी विभिन्न गांवों में व उनके जल-स्रोतों व खेतों में संरक्षित रह जाए तो विभिन्न स्थानों पर बाढ़ की संभावना अपने आप कम हो जाएगी।
प्रतिकूल मौसम (extreme weather) के समय में मिश्रित खेती (mixed cropping) की पद्धति से फसल के कुछ हिस्से को बचाने की संभावना बढ़ जाती है। मिश्रित खेती को कई स्तरों पर बढ़ावा देकर व छोटे किसानों को खेतों में अनाज, दलहन, तिलहन के साथ कई तरह की सब्ज़ियां व फल लगाने को प्रोत्साहित कर उन्हें प्रतिकूल मौसम में भी सशक्त रहने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है।
प्राकृतिक खेती की इन तकनीकों से किसानों का खर्च बहुत कम (low-cost farming) हो सकता है। यदि खर्च कम होगा तो कर्ज़ की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। इस तरह, छोटे किसान जलवायु बदलाव के अधिक कठिन दौर का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरी ओर, किसानों की बीज सम्बंधी आत्म-निर्भरता (seed self-reliance) को बढ़ाने पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। आत्म-निर्भरता बढ़ने से जलवायु बदलाव का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है।
जिन समुदायों में आपसी सहयोग व एकता (community cooperation) बढ़ती है, उनकी जलवायु बदलाव के दौर का आपसी सहयोग से बेहतर ढंग से सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है। ज़रूरत है कि ग्रामीण समुदाय आपसी सहयोग को बढ़ाएं, उनके स्व-सहायता समूह (self-help groups) गठित किए जाएं, अधिक व्यापक स्तर पर भी संगठन बनाए जाएं, सबके सहयोग से सामाजिक उद्यम (social enterprises) स्थापित किए जाएं।
उपरोक्त सभी प्रयास सृजन संस्था ने निरंतर अपने कार्यक्रमों के ज़रिए किए हैं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य ग्रामीण आजीविकाओं (जैसे कृषि, बागवानी, बकरी-पालन) को टिकाऊ तौर पर बेहतर और समृद्ध करना है व इसमें विशेष तौर पर कमज़ोर वर्ग व उसमें भी महिलाओं (women empowerment) पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सृजन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे बगीचों में फलदार पेड़ लगाने के अतिरिक्त तपोवन नामक मानव-निर्मित वन (community forests) अनेक गांवों में लगाए गए हैं जिनमें मिश्रित स्थानीय प्रजातियों के हज़ारों वृक्ष साथ-साथ लगाए गए हैं। कार्यक्रम जलवायु बदलाव के संकट के दोनों पहलुओं के लिहाज़ से बहुत मददगार सिद्ध हो रहा है।
इस तरह अनेक स्तरों पर जो कार्य ग्रामीण आजीविका आधार को मजबूत करते हैं, वे जलवायु बदलाव (climate action) की गंभीर समस्या के संदर्भ में भी मददगार होते हैं। एक ओर वे जलवायु बदलाव के संकट को कम करने में सहयोग करते हैं तो दूसरी ओर, प्रतिकूल मौसम और आपदाओं का सामना करने की ग्रामीण समुदायों की क्षमता को बढ़ाते भी हैं। इन कार्यक्रमों के इस व्यापक महत्व व समन्वय क्षमता को देखते हुए इन्हें सरकारी व सी.एस.आर. स्तर (CSR initiatives) पर अधिक सहयोग व समर्थन प्राप्त होना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)
नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
Photo Credit : https://www.asiapathways-adbi.org/wp-content/uploads/2024/06/Climate-Smart-Agriculture-for-a-Sustainable-Future-1024×631.png